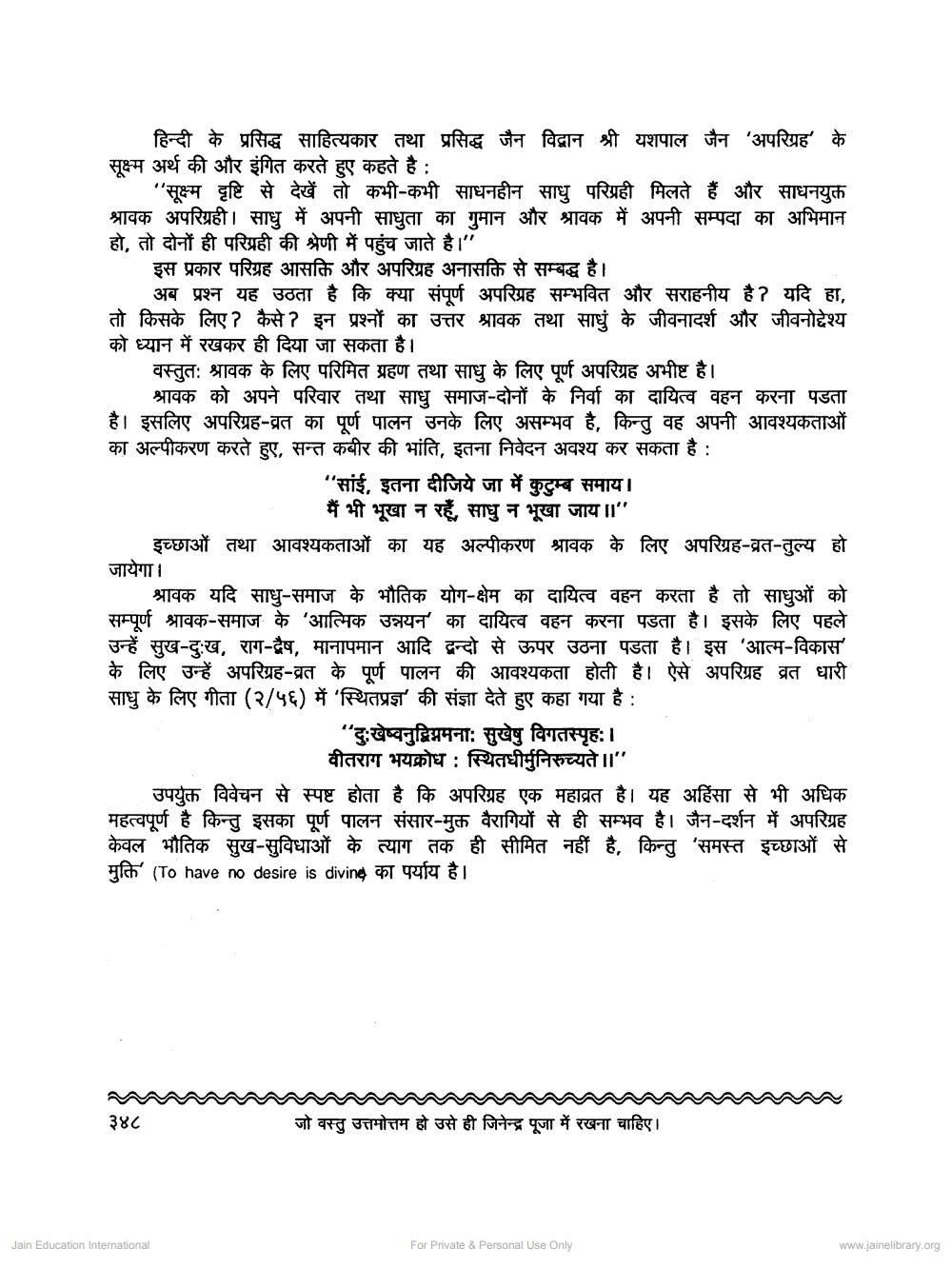________________
हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा प्रसिद्ध जैन विद्वान श्री यशपाल जैन 'अपरिग्रह के सूक्ष्म अर्थ की और इंगित करते हुए कहते है :
"सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो कभी-कभी साधनहीन साधु परिग्रही मिलते हैं और साधनयुक्त श्रावक अपरिग्रही। साधु में अपनी साधुता का गुमान और श्रावक में अपनी सम्पदा का अभिमान हो, तो दोनों ही परिग्रही की श्रेणी में पहुंच जाते है।"
इस प्रकार परिग्रह आसक्ति और अपरिग्रह अनासक्ति से सम्बद्ध है।
अब प्रश्न यह उठता है कि क्या संपूर्ण अपरिग्रह सम्भवित और सराहनीय है? यदि हा, तो किसके लिए? कैसे? इन प्रश्नों का उत्तर श्रावक तथा साधु के जीवनादर्श और जीवनोद्देश्य को ध्यान में रखकर ही दिया जा सकता है।
वस्तुत: श्रावक के लिए परिमित ग्रहण तथा साधु के लिए पूर्ण अपरिग्रह अभीष्ट है।
श्रावक को अपने परिवार तथा साधु समाज-दोनों के निर्वा का दायित्व वहन करना पड़ता है। इसलिए अपरिग्रह-व्रत का पूर्ण पालन उनके लिए असम्भव है, किन्तु वह अपनी आवश्यकताओं का अल्पीकरण करते हुए, सन्त कबीर की भांति, इतना निवेदन अवश्य कर सकता है :
"सांई, इतना दीजिये जा में कुटुम्ब समाय।
मैं भी भूखा न रहूँ, साधु न भूखा जाय ।।" इच्छाओं तथा आवश्यकताओं का यह अल्पीकरण श्रावक के लिए अपरिग्रह-व्रत-तुल्य हो जायेगा।
श्रावक यदि साधु-समाज के भौतिक योग-क्षेम का दायित्व वहन करता है तो साधुओं को सम्पूर्ण श्रावक-समाज के 'आत्मिक उन्नयन' का दायित्व वहन करना पड़ता है। इसके लिए पहले उन्हें सुख-दु:ख, राग-द्वेष, मानापमान आदि द्वन्दो से ऊपर उठना पड़ता है। इस 'आत्म-विकास' के लिए उन्हें अपरिग्रह-व्रत के पूर्ण पालन की आवश्यकता होती है। ऐसे अपरिग्रह व्रत धारी साधु के लिए गीता (२/५६) में 'स्थितप्रज्ञ' की संज्ञा देते हुए कहा गया है :
"दुःखेष्वनुद्विग्नमना: सुखेषु विगतस्पृहः।
वीतराग भयक्रोध : स्थितधीर्मुनिरुच्यते।।" उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि अपरिग्रह एक महाव्रत है। यह अहिंसा से भी अधिक महत्वपूर्ण है किन्तु इसका पूर्ण पालन संसार-मुक्त वैरागियों से ही सम्भव है। जैन-दर्शन में अपरिग्रह केवल भौतिक सुख-सुविधाओं के त्याग तक ही सीमित नहीं है, किन्तु 'समस्त इच्छाओं से मुक्ति' (To have no desire is divine का पर्याय है।
३४८
जो वस्तु उत्तमोत्तम हो उसे ही जिनेन्द्र पूजा में रखना चाहिए।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org