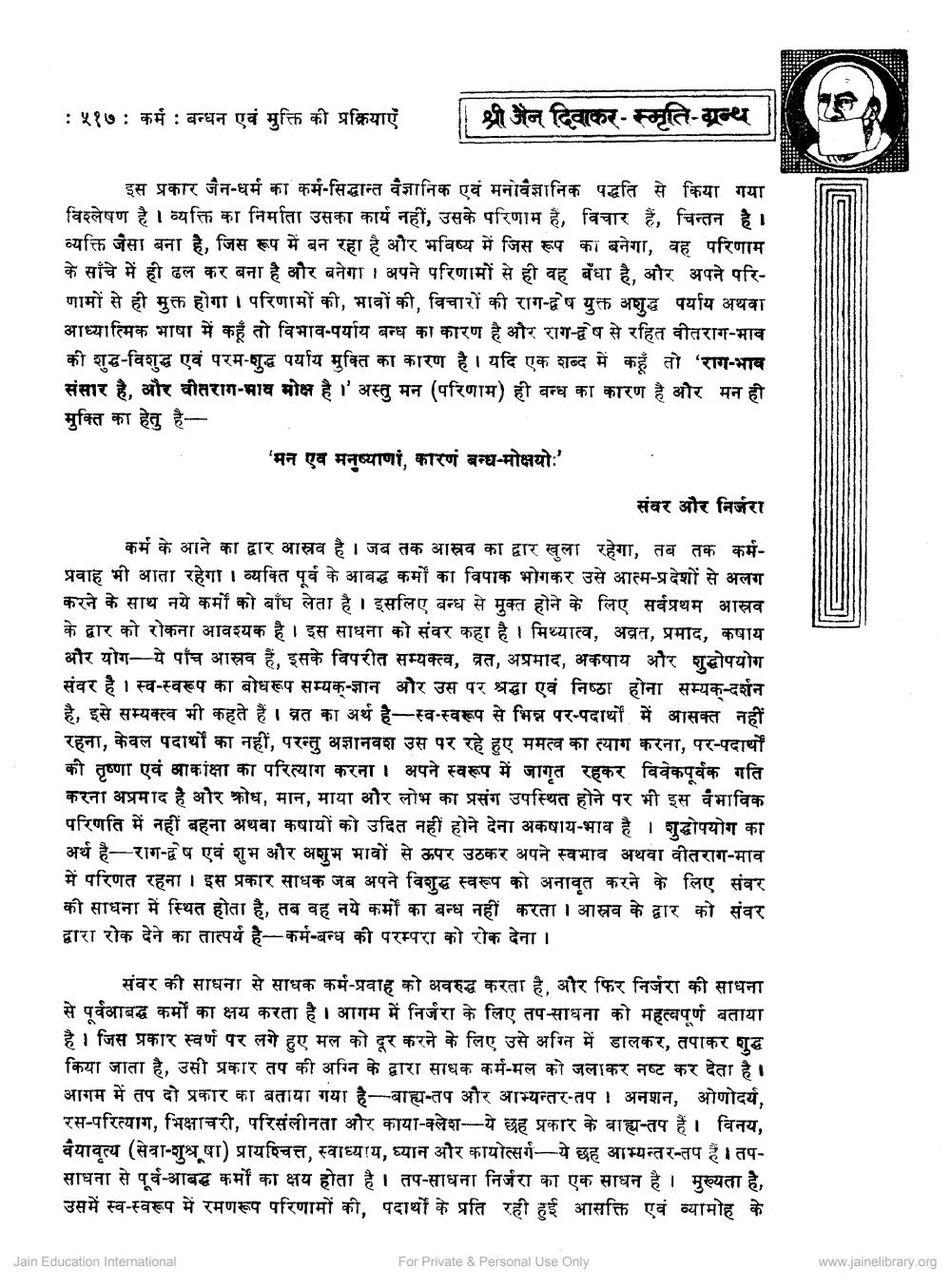________________
: ५१७ : कर्म : बन्धन एवं मुक्ति की प्रक्रियाएँ
श्री जैन दिवाकर स्मृति-ग्रन्थ
इस प्रकार जैन-धर्म का कर्म-सिद्धान्त वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक पद्धति से किया गया विश्लेषण है । व्यक्ति का निर्माता उसका कार्य नहीं, उसके परिणाम हैं, विचार हैं, चिन्तन है। व्यक्ति जैसा बना है, जिस रूप में बन रहा है और भविष्य में जिस रूप का बनेगा, वह परिणाम के साँचे में ही ढल कर बना है और बनेगा । अपने परिणामों से ही वह बँधा है, और अपने परिणामों से ही मुक्त होगा। परिणामों की, भावों की, विचारों की राग-द्वेष युक्त अशुद्ध पर्याय अथवा आध्यात्मिक भाषा में कहूँ तो विभाव-पर्याय बन्ध का कारण है और राग-द्वेष से रहित वीतराग-भाव की शुद्ध-विशुद्ध एवं परम-शुद्ध पर्याय मुक्ति का कारण है। यदि एक शब्द में कहूँ तो 'राग-भाव संसार है, और वीतराग-भाव मोक्ष है ।' अस्तु मन (परिणाम) ही बन्ध का कारण है और मन ही मुक्ति का हेतु है
'मन एव मनुष्याणां, कारणं बन्ध-मोक्षयोः'
संवर और निर्जरा
कर्म के आने का द्वार आस्रव है । जब तक आस्रव का द्वार खुला रहेगा, तब तक कर्मप्रवाह भी आता रहेगा। व्यक्ति पूर्व के आबद्ध कर्मों का विपाक भोगकर उसे आत्म-प्रदेशों से अलग करने के साथ नये कर्मों को बाँध लेता है। इसलिए बन्ध से मुक्त होने के लिए सर्वप्रथम आस्रव के द्वार को रोकना आवश्यक है। इस साधना को संवर कहा है । मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग-ये पाँच आस्रव हैं, इसके विपरीत सम्यक्त्व, व्रत, अप्रमाद, अकषाय और शुद्धोपयोग संवर है। स्व-स्वरूप का बोधरूप सम्यक-ज्ञान और उस पर श्रद्धा एवं निष्ठा होना सम्यक-दर्शन है, इसे सम्यक्त्व भी कहते हैं । व्रत का अर्थ है-स्व-स्वरूप से भिन्न पर-पदार्थों में आसक्त नहीं रहना, केवल पदार्थों का नहीं, परन्तु अज्ञानवश उस पर रहे हुए ममत्व का त्याग करना, पर-पदार्थों की तृष्णा एवं आकांक्षा का परित्याग करना। अपने स्वरूप में जागृत रहकर विवेकपूर्वक गति करना अप्रमाद है और क्रोध, मान, माया और लोभ का प्रसंग उपस्थित होने पर भी इस वभाविक परिणति में नहीं बहना अथवा कषायों को उदित नहीं होने देना अकषाय-भाव है । शुद्धोपयोग का अर्थ है-राग-द्वेष एवं शुभ और अशुभ भावों से ऊपर उठकर अपने स्वभाव अथवा वीतराग-माव में परिणत रहना । इस प्रकार साधक जब अपने विशुद्ध स्वरूप को अनावृत करने के लिए संवर की साधना में स्थित होता है, तब वह नये कर्मों का बन्ध नहीं करता । आस्रव के द्वार को संवर द्वारा रोक देने का तात्पर्य है-कर्म-बन्ध की परम्परा को रोक देना ।
___ संवर की साधना से साधक कर्म-प्रवाह को अवरुद्ध करता है. और फिर निर्जरा की साधना से पर्वआबद्ध कर्मों का क्षय करता है। आगम में निर्जरा के लिए तप-साधना को महत्वपूर्ण बताया है। जिस प्रकार स्वर्ण पर लगे हए मल को दूर करने के लिए उसे अग्नि में डालकर, तपाकर शर किया जाता है, उसी प्रकार तप की अग्नि के द्वारा साधक कर्म-मल को जलाकर नष्ट कर देता है। आगम में तप दो प्रकार का बताया गया है-बाह्य-तप और आभ्यन्तर-तप । अनशन, ओणोदर्य, रस-परित्याग, भिक्षाचरी, परिसंलीनता और काया-क्लेश-ये छह प्रकार के बाह्य-तप हैं। विनय, वैयावृत्य (सेवा-शुश्र षा) प्रायश्चित्त, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग-ये छह आभ्यन्तर-तप हैं । तपसाधना से पूर्व-आबद्ध कर्मों का क्षय होता है। तप-साधना निर्जरा का एक साधन है। मुख्यता है, उसमें स्व-स्वरूप में रमणरूप परिणामों की, पदार्थों के प्रति रही हई आसक्ति एवं व्यामोह के
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org