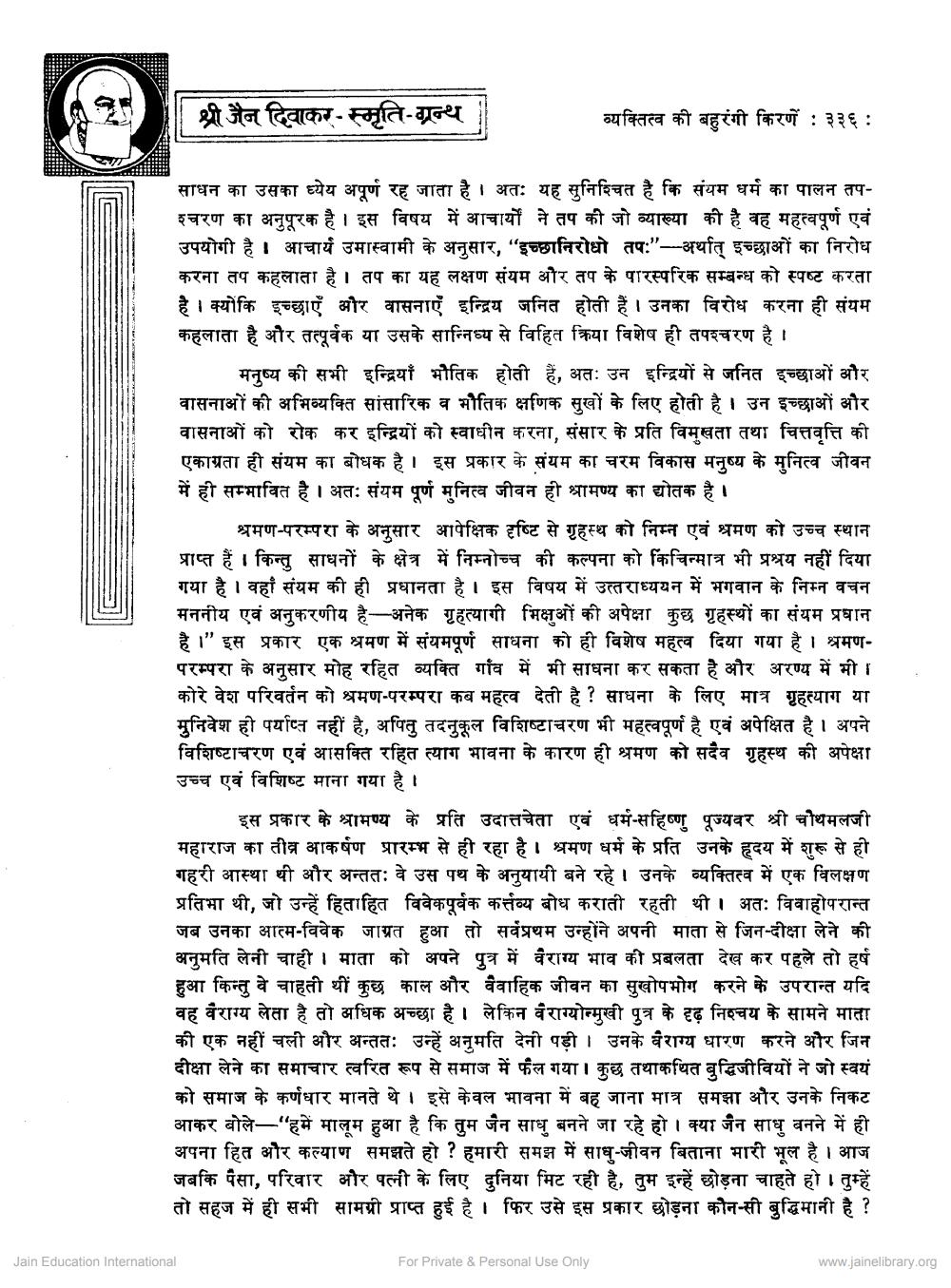________________
| श्री जैन दिवाकर स्मृति-वान्थ ।
व्यक्तित्व की बहुरंगी किरणें : ३३६ :
साधन का उसका ध्येय अपूर्ण रह जाता है । अतः यह सुनिश्चित है कि संयम धर्म का पालन तपश्चरण का अनुपूरक है । इस विषय में आचार्यों ने तप की जो व्याख्या की है वह महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। आचार्य उमास्वामी के अनुसार, "इच्छानिरोधो तप:"---अर्थात् इच्छाओं का निरोध करना तप कहलाता है। तप का यह लक्षण संयम और तप के पारस्परिक सम्बन्ध को स्पष्ट करता है। क्योंकि इच्छाएँ और वासनाएँ इन्द्रिय जनित होती हैं । उनका विरोध करना ही संयम कहलाता है और तत्पूर्वक या उसके सान्निध्य से विहित क्रिया विशेष ही तपश्चरण है। मनुष्य की सभी इन्द्रियाँ भौतिक होती हैं, अतः उन इन्द्रियों से जनित इच्छाओं और
तिक क्षणिक सुखों के लिए होती है। उन इच्छाओं और वासनाओं को रोक कर इन्द्रियों को स्वाधीन करना, संसार के प्रति विमुखता तथा चित्तवृत्ति की एकाग्रता ही संयम का बोधक है। इस प्रकार के संयम का चरम विकास मनुष्य के मुनित्व जीवन में ही सम्भावित है । अतः संयम पूर्ण मुनित्व जीवन ही श्रामण्य का द्योतक है ।
श्रमण-परम्परा के अनुसार आपेक्षिक दृष्टि से गृहस्थ को निम्न एवं श्रमण को उच्च स्थान प्राप्त हैं । किन्तु साधनों के क्षेत्र में निम्नोच्च की कल्पना को किचिन्मात्र भी प्रश्रय नहीं दिया गया है। वहाँ संयम की ही प्रधानता है। इस विषय में उत्तराध्ययन में भगवान के निम्न वचन मननीय एवं अनुकरणीय है-अनेक गृहत्यागी भिक्षुओं की अपेक्षा कुछ गृहस्थों का संयम प्रधान है।" इस प्रकार एक श्रमण में संयमपूर्ण साधना को ही विशेष महत्व दिया गया है। श्रमणपरम्परा के अनुसार मोह रहित व्यक्ति गांव में भी साधना कर सकता है और अरण्य में भी। कोरे वेश परिवर्तन को श्रमण-परम्परा कब महत्व देती है ? साधना के लिए मात्र गृहत्याग या मुनिवेश ही पर्याप्त नहीं है, अपितु तदनुकूल विशिष्टाचरण भी महत्वपूर्ण है एवं अपेक्षित है। अपने विशिष्टाचरण एवं आसक्ति रहित त्याग भावना के कारण ही श्रमण को सदैव गृहस्थ की अपेक्षा उच्च एवं विशिष्ट माना गया है।
।
इस प्रकार के श्रामण्य के प्रति उदात्तचेता एवं धर्म-सहिष्णु पूज्यवर श्री चौथमलजी महाराज का तीव्र आकर्षण प्रारम्भ से ही रहा है। श्रमण धर्म के प्रति उनके हृदय में शुरू से ही गहरी आस्था थी और अन्ततः वे उस पथ के अनुयायी बने रहे। उनके व्यक्तित्व में एक विलक्षण प्रतिभा थी, जो उन्हें हिताहित विवेकपूर्वक कर्तव्य बोध कराती रहती थी। अतः विवाहोपरान्त जब उनका आत्म-विवेक जाग्रत हुआ तो सर्वप्रथम उन्होंने अपनी माता से जिन-दीक्षा लेने की अनुमति लेनी चाही। माता को अपने पुत्र में वैराग्य भाव की प्रबलता देख कर पहले तो हर्ष हुआ किन्तु वे चाहती थीं कुछ काल और वैवाहिक जीवन का सुखोपभोग करने के उपरान्त यदि वह वैराग्य लेता है तो अधिक अच्छा है। लेकिन वैराग्योन्मुखी पुत्र के दृढ़ निश्चय के सामने माता की एक नहीं चली और अन्ततः उन्हें अनुमति देनी पड़ी। उनके वैराग्य धारण करने और जिन दीक्षा लेने का समाचार त्वरित रूप से समाज में फैल गया। कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों ने जो स्वयं को समाज के कर्णधार मानते थे। इसे केवल भावना में बह जाना मात्र समझा और उनके निकट आकर बोले- "हमें मालूम हुआ है कि तुम जैन साधु बनने जा रहे हो । क्या जैन साधु बनने में ही अपना हित और कल्याण समझते हो? हमारी समझ में साधु-जीवन बिताना भारी भूल है। आज जबकि पैसा, परिवार और पत्नी के लिए दुनिया मिट रही है, तुम इन्हें छोड़ना चाहते हो। तुम्हें तो सहज में ही सभी सामग्री प्राप्त हुई है। फिर उसे इस प्रकार छोड़ना कौन-सी बुद्धिमानी है ?
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org