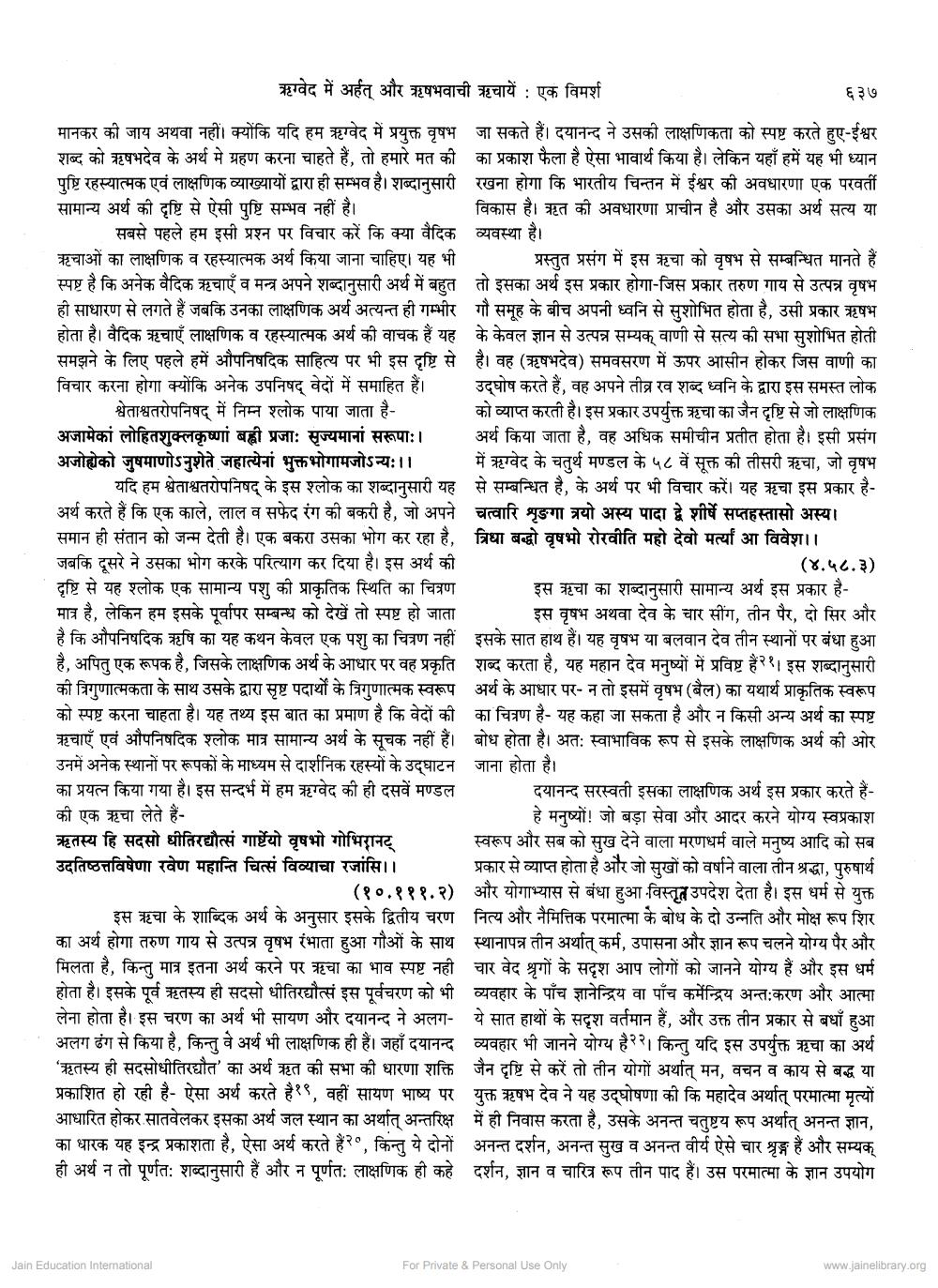________________
ऋग्वेद में अर्हत और ऋषभवाची ऋचायें : एक विमर्श
६३७
मानकर की जाय अथवा नहीं। क्योंकि यदि हम ऋग्वेद में प्रयुक्त वृषभ जा सकते हैं। दयानन्द ने उसकी लाक्षणिकता को स्पष्ट करते हुए-ईश्वर शब्द को ऋषभदेव के अर्थ मे ग्रहण करना चाहते हैं, तो हमारे मत की का प्रकाश फैला है ऐसा भावार्थ किया है। लेकिन यहाँ हमें यह भी ध्यान पुष्टि रहस्यात्मक एवं लाक्षणिक व्याख्यायों द्वारा ही सम्भव है। शब्दानुसारी रखना होगा कि भारतीय चिन्तन में ईश्वर की अवधारणा एक परवर्ती सामान्य अर्थ की दृष्टि से ऐसी पुष्टि सम्भव नहीं है।
विकास है। ऋत की अवधारणा प्राचीन है और उसका अर्थ सत्य या सबसे पहले हम इसी प्रश्न पर विचार करें कि क्या वैदिक व्यवस्था है। ऋचाओं का लाक्षणिक व रहस्यात्मक अर्थ किया जाना चाहिए। यह भी प्रस्तुत प्रसंग में इस ऋचा को वृषभ से सम्बन्धित मानते हैं स्पष्ट है कि अनेक वैदिक ऋचाएँ व मन्त्र अपने शब्दानुसारी अर्थ में बहुत तो इसका अर्थ इस प्रकार होगा-जिस प्रकार तरुण गाय से उत्पन्न वृषभ ही साधारण से लगते हैं जबकि उनका लाक्षणिक अर्थ अत्यन्त ही गम्भीर गौ समूह के बीच अपनी ध्वनि से सुशोभित होता है, उसी प्रकार ऋषभ होता है। वैदिक ऋचाएँ लाक्षणिक व रहस्यात्मक अर्थ की वाचक हैं यह के केवल ज्ञान से उत्पन्न सम्यक् वाणी से सत्य की सभा सुशोभित होती समझने के लिए पहले हमें औपनिषदिक साहित्य पर भी इस दृष्टि से है। वह (ऋषभदेव) समवसरण में ऊपर आसीन होकर जिस वाणी का विचार करना होगा क्योंकि अनेक उपनिषद् वेदों में समाहित हैं। उद्घोष करते हैं, वह अपने तीव्र रव शब्द ध्वनि के द्वारा इस समस्त लोक श्वेताश्वतरोपनिषद् में निम्न श्लोक पाया जाता है
को व्याप्त करती है। इस प्रकार उपर्युक्त ऋचा का जैन दृष्टि से जो लाक्षणिक अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वी प्रजाः सृज्यमानां सरूपाः। अर्थ किया जाता है, वह अधिक समीचीन प्रतीत होता है। इसी प्रसंग अजोह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः।। में ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल के ५८ वें सूक्त की तीसरी ऋचा, जो वृषभ
यदि हम श्वेताश्वतरोपनिषद् के इस श्लोक का शब्दानुसारी यह से सम्बन्धित है, के अर्थ पर भी विचार करें। यह ऋचा इस प्रकार हैअर्थ करते हैं कि एक काले, लाल व सफेद रंग की बकरी है, जो अपने चत्वारि शृङगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य। समान ही संतान को जन्म देती है। एक बकरा उसका भोग कर रहा है, त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मां आ विवेश।। जबकि दूसरे ने उसका भोग करके परित्याग कर दिया है। इस अर्थ की
(४.५८.३) दृष्टि से यह श्लोक एक सामान्य पशु की प्राकृतिक स्थिति का चित्रण इस ऋचा का शब्दानुसारी सामान्य अर्थ इस प्रकार हैमात्र है, लेकिन हम इसके पूर्वापर सम्बन्ध को देखें तो स्पष्ट हो जाता इस वृषभ अथवा देव के चार सींग, तीन पैर, दो सिर और है कि औपनिषदिक ऋषि का यह कथन केवल एक पशु का चित्रण नहीं इसके सात हाथ हैं। यह वृषभ या बलवान देव तीन स्थानों पर बंधा हुआ है, अपित एक रूपक है, जिसके लाक्षणिक अर्थ के आधार पर वह प्रकृति शब्द करता है, यह महान देव मनुष्यों में प्रविष्ट हैं २१। इस शब्दानुसारी की त्रिगुणात्मकता के साथ उसके द्वारा सृष्ट पदार्थों के त्रिगुणात्मक स्वरूप अर्थ के आधार पर- न तो इसमें वृषभ (बैल) का यथार्थ प्राकृतिक स्वरूप को स्पष्ट करना चाहता है। यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि वेदों की का चित्रण है- यह कहा जा सकता है और न किसी अन्य अर्थ का स्पष्ट ऋचाएँ एवं औपनिषदिक श्लोक मात्र सामान्य अर्थ के सूचक नहीं हैं। बोध होता है। अत: स्वाभाविक रूप से इसके लाक्षणिक अर्थ की ओर उनमें अनेक स्थानों पर रूपकों के माध्यम से दार्शनिक रहस्यों के उद्घाटन जाना होता है। का प्रयत्न किया गया है। इस सन्दर्भ में हम ऋग्वेद की ही दसवें मण्डल दयानन्द सरस्वती इसका लाक्षणिक अर्थ इस प्रकार करते हैंकी एक ऋचा लेते हैं
हे मनुष्यों! जो बड़ा सेवा और आदर करने योग्य स्वप्रकाश ऋतस्य हि सदसो धीतिरद्यौत्सं गार्टेयो वृषभो गोभिरानट स्वरूप और सब को सुख देने वाला मरणधर्म वाले मनुष्य आदि को सब उदतिष्ठत्तविषेणा रवेण महान्ति चित्सं विव्याचा रजांसि।। प्रकार से व्याप्त होता है और जो सुखों को वर्षाने वाला तीन श्रद्धा, पुरुषार्थ
(१०.१११.२) और योगाभ्यास से बंधा हुआ विस्तृत उपदेश देता है। इस धर्म से युक्त इस ऋचा के शाब्दिक अर्थ के अनुसार इसके द्वितीय चरण नित्य और नैमित्तिक परमात्मा के बोध के दो उन्नति और मोक्ष रूप शिर का अर्थ होगा तरुण गाय से उत्पन्न वृषभ रंभाता हुआ गौओं के साथ स्थानापन्न तीन अर्थात् कर्म, उपासना और ज्ञान रूप चलने योग्य पैर और मिलता है, किन्तु मात्र इतना अर्थ करने पर ऋचा का भाव स्पष्ट नही चार वेद श्रृगों के सदृश आप लोगों को जानने योग्य हैं और इस धर्म होता है। इसके पूर्व ऋतस्य ही सदसो धीतिरद्यौत्सं इस पूर्वचरण को भी व्यवहार के पाँच ज्ञानेन्द्रिय वा पाँच कर्मेन्द्रिय अन्त:करण और आत्मा लेना होता है। इस चरण का अर्थ भी सायण और दयानन्द ने अलग- ये सात हाथों के सदृश वर्तमान हैं, और उक्त तीन प्रकार से बधाँ हुआ अलग ढंग से किया है, किन्तु वे अर्थ भी लाक्षणिक ही हैं। जहाँ दयानन्द व्यवहार भी जानने योग्य है २२। किन्तु यदि इस उपर्युक्त ऋचा का अर्थ 'ऋतस्य ही सदसोधीतिरद्यौत' का अर्थ ऋत की सभा की धारणा शक्ति जैन दृष्टि से करें तो तीन योगों अर्थात् मन, वचन व काय से बद्ध या प्रकाशित हो रही है- ऐसा अर्थ करते है१९, वहीं सायण भाष्य पर युक्त ऋषभ देव ने यह उद्घोषणा की कि महादेव अर्थात् परमात्मा मृत्यों आधारित होकर सातवेलकर इसका अर्थ जल स्थान का अर्थात् अन्तरिक्ष में ही निवास करता है, उसके अनन्त चतुष्टय रूप अर्थात् अनन्त ज्ञान, का धारक यह इन्द्र प्रकाशता है, ऐसा अर्थ करते हैं२०, किन्तु ये दोनों अनन्त दर्शन, अनन्त सुख व अनन्त वीर्य ऐसे चार श्रङ्ग हैं और सम्यक ही अर्थ न तो पूर्णत: शब्दानुसारी हैं और न पूर्णत: लाक्षणिक ही कहे दर्शन, ज्ञान व चारित्र रूप तीन पाद हैं। उस परमात्मा के ज्ञान उपयोग
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org