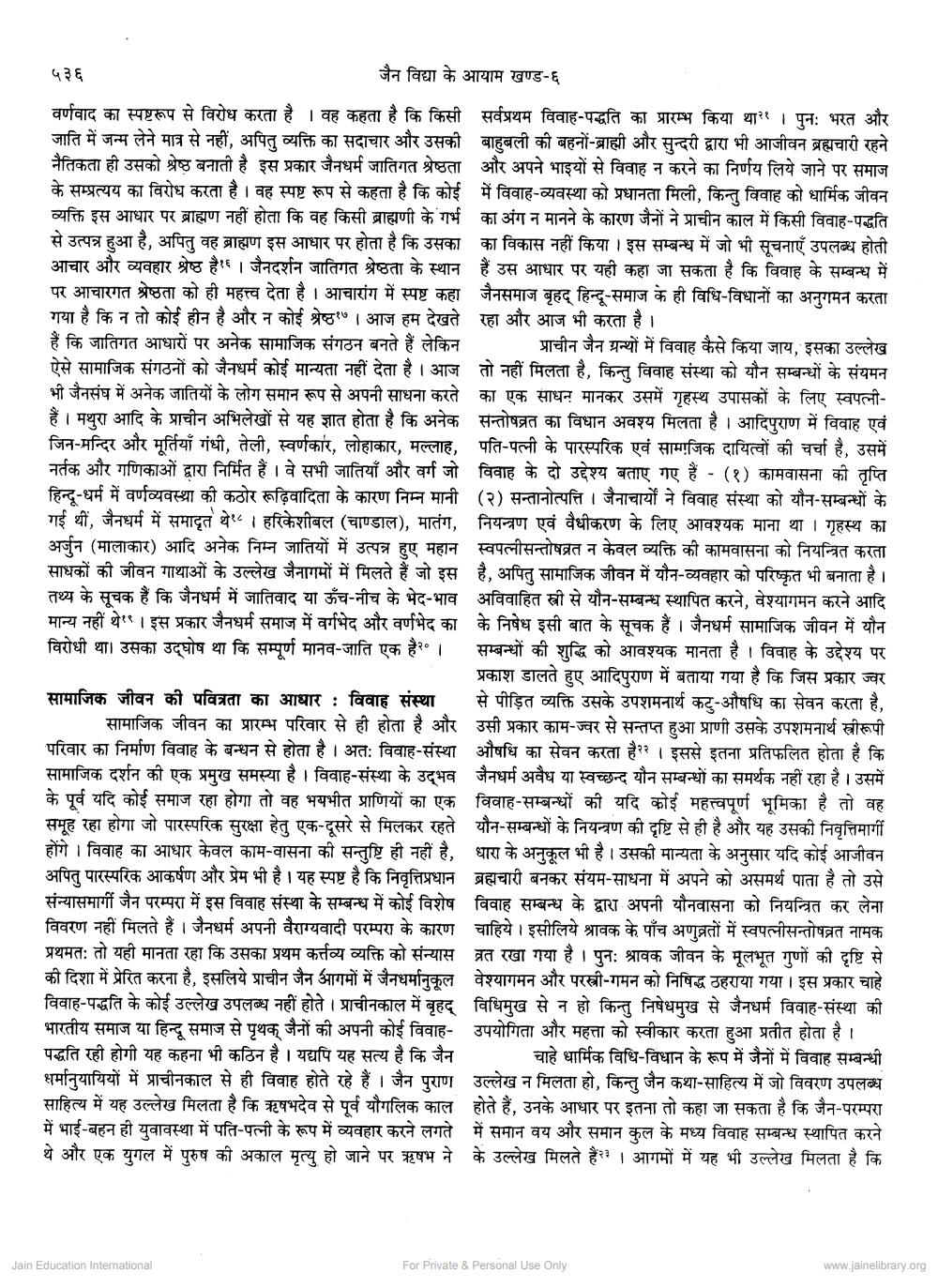________________
५३६
जैन विद्या के आयाम खण्ड-६
वर्णवाद का स्पष्टरूप से विरोध करता है । वह कहता है कि किसी सर्वप्रथम विवाह-पद्धति का प्रारम्भ किया थारे । पुनः भरत और जाति में जन्म लेने मात्र से नहीं, अपितु व्यक्ति का सदाचार और उसकी बाहुबली की बहनों-ब्राह्मी और सुन्दरी द्वारा भी आजीवन ब्रह्मचारी रहने नैतिकता ही उसको श्रेष्ठ बनाती है इस प्रकार जैनधर्म जातिगत श्रेष्ठता और अपने भाइयों से विवाह न करने का निर्णय लिये जाने पर समाज के सम्प्रत्यय का विरोध करता है । वह स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई में विवाह-व्यवस्था को प्रधानता मिली, किन्तु विवाह को धार्मिक जीवन व्यक्ति इस आधार पर ब्राह्मण नहीं होता कि वह किसी ब्राह्मणी के गर्भ का अंग न मानने के कारण जैनों ने प्राचीन काल में किसी विवाह-पद्धति से उत्पन्न हुआ है, अपितु वह ब्राह्मण इस आधार पर होता है कि उसका का विकास नहीं किया । इस सम्बन्ध में जो भी सूचनाएँ उपलब्ध होती आचार और व्यवहार श्रेष्ठ है१६ । जैनदर्शन जातिगत श्रेष्ठता के स्थान हैं उस आधार पर यही कहा जा सकता है कि विवाह के सम्बन्ध में पर आचारगत श्रेष्ठता को ही महत्त्व देता है । आचारांग में स्पष्ट कहा जैनसमाज बृहद् हिन्दू-समाज के ही विधि-विधानों का अनुगमन करता गया है कि न तो कोई हीन है और न कोई श्रेष्ठ । आज हम देखते रहा और आज भी करता है। हैं कि जातिगत आधारों पर अनेक सामाजिक संगठन बनते हैं लेकिन प्राचीन जैन ग्रन्थों में विवाह कैसे किया जाय, इसका उल्लेख ऐसे सामाजिक संगठनों को जैनधर्म कोई मान्यता नहीं देता है । आज तो नहीं मिलता है, किन्तु विवाह संस्था को यौन सम्बन्धों के संयमन भी जैनसंघ में अनेक जातियों के लोग समान रूप से अपनी साधना करते का एक साधन मानकर उसमें गृहस्थ उपासकों के लिए स्वपत्नीहैं। मथुरा आदि के प्राचीन अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि अनेक सन्तोषव्रत का विधान अवश्य मिलता है । आदिपुराण में विवाह एवं जिन-मन्दिर और मूर्तियाँ गंधी, तेली, स्वर्णकार, लोहाकार, मल्लाह, पति-पत्नी के पारस्परिक एवं सामाजिक दायित्वों की चर्चा है, उसमें नर्तक और गणिकाओं द्वारा निर्मित हैं । वे सभी जातियाँ और वर्ग जो विवाह के दो उद्देश्य बताए गए हैं - (१) कामवासना की तृप्ति हिन्दू-धर्म में वर्णव्यवस्था की कठोर रूढ़िवादिता के कारण निम्न मानी (२) सन्तानोत्पत्ति । जैनाचार्यों ने विवाह संस्था को यौन सम्बन्धों के गई थीं, जैनधर्म में समादृत थे।८ । हरिकेशीबल (चाण्डाल), मातंग, नियन्त्रण एवं वैधीकरण के लिए आवश्यक माना था । गृहस्थ का अर्जुन (मालाकार) आदि अनेक निम्न जातियों में उत्पन्न हुए महान स्वपत्नीसन्तोषव्रत न केवल व्यक्ति की कामवासना को नियन्त्रित करता साधकों की जीवन गाथाओं के उल्लेख जैनागमों में मिलते हैं जो इस है, अपितु सामाजिक जीवन में यौन-व्यवहार को परिष्कृत भी बनाता है। तथ्य के सूचक हैं कि जैनधर्म में जातिवाद या ऊँच-नीच के भेद-भाव अविवाहित स्त्री से यौन सम्बन्ध स्थापित करने, वेश्यागमन करने आदि मान्य नहीं थे१९ । इस प्रकार जैनधर्म समाज में वर्गभेद और वर्णभेद का के निषेध इसी बात के सूचक हैं । जैनधर्म सामाजिक जीवन में यौन विरोधी था। उसका उद्घोष था कि सम्पूर्ण मानव-जाति एक है। सम्बन्धों की शुद्धि को आवश्यक मानता है । विवाह के उद्देश्य पर
प्रकाश डालते हुए आदिपुराण में बताया गया है कि जिस प्रकार ज्वर सामाजिक जीवन की पवित्रता का आधार : विवाह संस्था से पीड़ित व्यक्ति उसके उपशमनार्थ कटु-औषधि का सेवन करता है,
सामाजिक जीवन का प्रारम्भ परिवार से ही होता है और उसी प्रकार काम-ज्वर से सन्तप्त हुआ प्राणी उसके उपशमनार्थ स्त्रीरूपी परिवार का निर्माण विवाह के बन्धन से होता है । अत: विवाह-संस्था औषधि का सेवन करता है२२ । इससे इतना प्रतिफलित होता है कि सामाजिक दर्शन की एक प्रमुख समस्या है । विवाह-संस्था के उद्भव जैनधर्म अवैध या स्वच्छन्द यौन सम्बन्धों का समर्थक नहीं रहा है । उसमें के पूर्व यदि कोई समाज रहा होगा तो वह भयभीत प्राणियों का एक विवाह-सम्बन्धों की यदि कोई महत्त्वपूर्ण भूमिका है तो वह समूह रहा होगा जो पारस्परिक सुरक्षा हेतु एक-दूसरे से मिलकर रहते यौन सम्बन्धों के नियन्त्रण की दृष्टि से ही है और यह उसकी निवृत्तिमार्गी होंगे । विवाह का आधार केवल काम-वासना की सन्तुष्टि ही नहीं है, धारा के अनुकूल भी है। उसकी मान्यता के अनुसार यदि कोई आजीवन अपितु पारस्परिक आकर्षण और प्रेम भी है । यह स्पष्ट है कि निवृत्तिप्रधान ब्रह्मचारी बनकर संयम-साधना में अपने को असमर्थ पाता है तो उसे संन्यासमार्गी जैन परम्परा में इस विवाह संस्था के सम्बन्ध में कोई विशेष विवाह सम्बन्ध के द्वारा अपनी यौनवासना को नियन्त्रित कर लेना विवरण नहीं मिलते हैं । जैनधर्म अपनी वैराग्यवादी परम्परा के कारण चाहिये । इसीलिये श्रावक के पाँच अणुव्रतों में स्वपत्नीसन्तोषव्रत नामक प्रथमत: तो यही मानता रहा कि उसका प्रथम कर्तव्य व्यक्ति को संन्यास व्रत रखा गया है । पुनः श्रावक जीवन के मूलभूत गुणों की दृष्टि से की दिशा में प्रेरित करना है, इसलिये प्राचीन जैन आगमों में जैनधर्मानुकूल वेश्यागमन और परस्त्री-गमन को निषिद्ध ठहराया गया। इस प्रकार चाहे विवाह-पद्धति के कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं होते। प्राचीनकाल में बृहद् विधिमुख से न हो किन्तु निषेधमुख से जैनधर्म विवाह-संस्था की भारतीय समाज या हिन्दू समाज से पृथक् जैनों की अपनी कोई विवाह- उपयोगिता और महत्ता को स्वीकार करता हुआ प्रतीत होता है। पद्धति रही होगी यह कहना भी कठिन है । यद्यपि यह सत्य है कि जैन चाहे धार्मिक विधि-विधान के रूप में जैनों में विवाह सम्बन्धी धर्मानुयायियों में प्राचीनकाल से ही विवाह होते रहे हैं । जैन पुराण उल्लेख न मिलता हो, किन्तु जैन कथा-साहित्य में जो विवरण उपलब्ध साहित्य में यह उल्लेख मिलता है कि ऋषभदेव से पूर्व यौगलिक काल होते हैं, उनके आधार पर इतना तो कहा जा सकता है कि जैन-परम्परा में भाई-बहन ही युवावस्था में पति-पत्नी के रूप में व्यवहार करने लगते में समान वय और समान कुल के मध्य विवाह सम्बन्ध स्थापित करने थे और एक युगल में पुरुष की अकाल मृत्यु हो जाने पर ऋषभ ने के उल्लेख मिलते हैं२३ । आगमों में यह भी उल्लेख मिलता है कि
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org