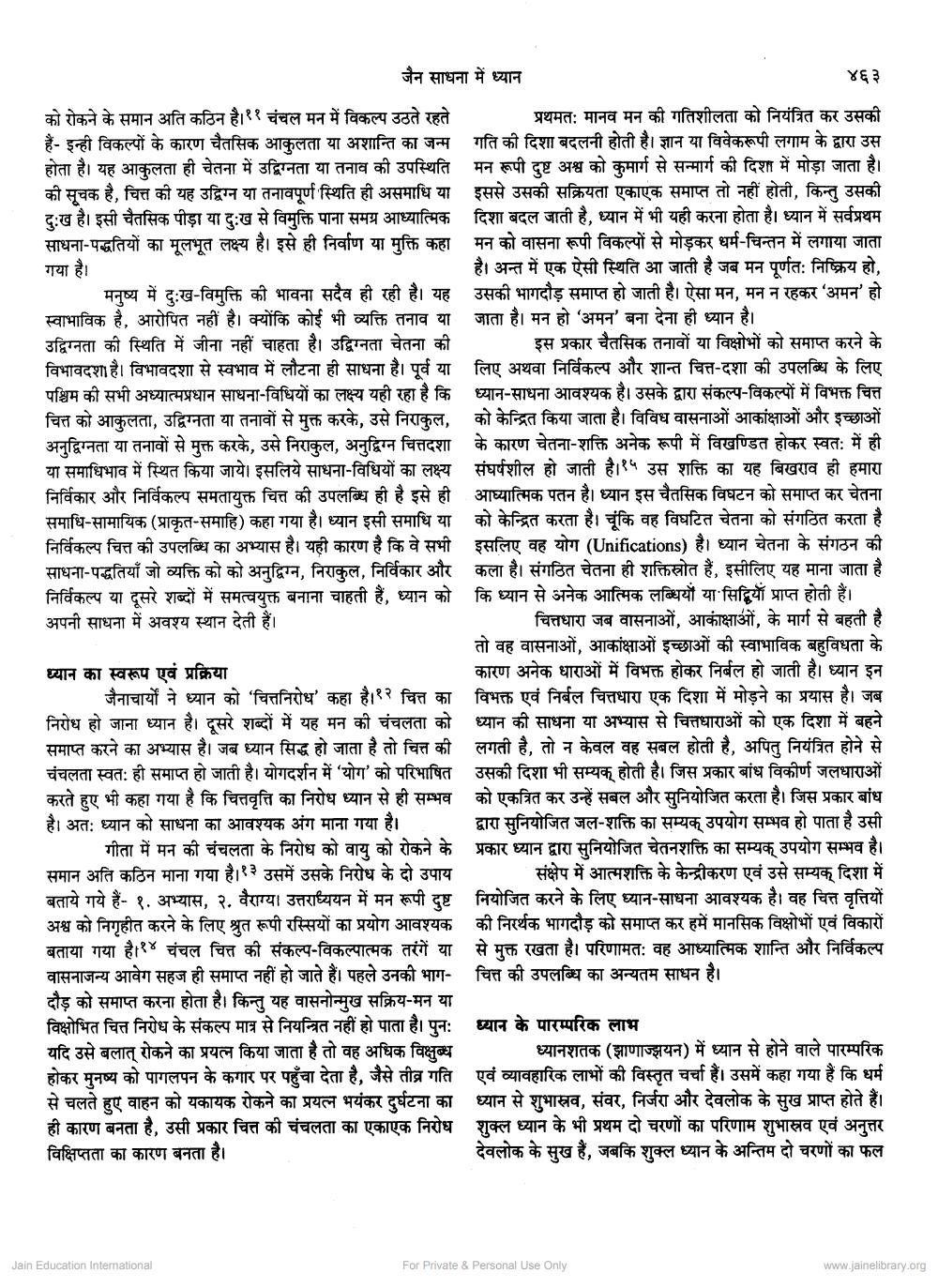________________
को कानयोग (UDHशक्तिमा
जैन साधना में ध्यान
४६३ को रोकने के समान अति कठिन है।११ चंचल मन में विकल्प उठते रहते प्रथमत: मानव मन की गतिशीलता को नियंत्रित कर उसकी हैं- इन्ही विकल्पों के कारण चैतसिक आकुलता या अशान्ति का जन्म गति की दिशा बदलनी होती है। ज्ञान या विवेकरूपी लगाम के द्वारा उस होता है। यह आकुलता ही चेतना में उद्विग्नता या तनाव की उपस्थिति मन रूपी दुष्ट अश्व को कुमार्ग से सन्मार्ग की दिशा में मोड़ा जाता है। की सूचक है, चित्त की यह उद्विग्न या तनावपूर्ण स्थिति ही असमाधि या इससे उसकी सक्रियता एकाएक समाप्त तो नहीं होती, किन्तु उसकी दुःख है। इसी चैतसिक पीड़ा या दुःख से विमुक्ति पाना समग्र आध्यात्मिक दिशा बदल जाती है, ध्यान में भी यही करना होता है। ध्यान में सर्वप्रथम साधना-पद्धतियों का मूलभूत लक्ष्य है। इसे ही निर्वाण या मुक्ति कहा मन को वासना रूपी विकल्पों से मोड़कर धर्म-चिन्तन में लगाया जाता गया है।
है। अन्त में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब मन पूर्णतः निष्क्रिय हो, मनुष्य में दुःख-विमुक्ति की भावना सदैव ही रही है। यह उसकी भागदौड़ समाप्त हो जाती है। ऐसा मन, मन न रहकर 'अमन' हो स्वाभाविक है, आरोपित नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति तनाव या जाता है। मन हो 'अमन' बना देना ही ध्यान है। उद्विग्नता की स्थिति में जीना नहीं चाहता है। उद्विग्नता चेतना की इस प्रकार चैतसिक तनावों या विक्षोभों को समाप्त करने के विभावदशा है। विभावदशा से स्वभाव में लौटना ही साधना है। पूर्व या लिए अथवा निर्विकल्प और शान्त चित्त-दशा की उपलब्धि के लिए पश्चिम की सभी अध्यात्मप्रधान साधना-विधियों का लक्ष्य यही रहा है कि ध्यान-साधना आवश्यक है। उसके द्वारा संकल्प-विकल्पों में विभक्त चित्त चित्त को आकुलता, उद्विग्नता या तनावों से मुक्त करके, उसे निराकुल, को केन्द्रित किया जाता है। विविध वासनाओं आकांक्षाओं और इच्छाओं अनुद्विग्नता या तनावों से मुक्त करके, उसे निराकुल, अनुद्विग्न चित्तदशा के कारण चेतना-शक्ति अनेक रूपी में विखण्डित होकर स्वत: में ही या समाधिभाव में स्थित किया जाये। इसलिये साधना-विधियों का लक्ष्य संघर्षशील हो जाती है।१५ उस शक्ति का यह बिखराव ही हमारा निर्विकार और निर्विकल्प समतायुक्त चित्त की उपलब्धि ही है इसे ही आध्यात्मिक पतन है। ध्यान इस चैतसिक विघटन को समाप्त कर चेतना समाधि-सामायिक (प्राकृत-समाहि) कहा गया है। ध्यान इसी समाधि या को केन्द्रित करता है। चूंकि वह विघटित चेतना को संगठित करता है निर्विकल्प चित्त की उपलब्धि का अभ्यास है। यही कारण है कि वे सभी इसलिए वह योग (Unifications) है। ध्यान चेतना के संगठन की साधना-पद्धतियाँ जो व्यक्ति को को अनुद्विग्न, निराकुल, निर्विकार और कला है। संगठित चेतना ही शक्तिस्रोत हैं, इसीलिए यह माना जाता है निर्विकल्प या दूसरे शब्दों में समत्वयुक्त बनाना चाहती हैं, ध्यान को कि ध्यान से अनेक आत्मिक लब्धियों या सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अपनी साधना में अवश्य स्थान देती हैं।
चित्तधारा जब वासनाओं, आकाक्षाओं, के मार्ग से बहती है
तो वह वासनाओं, आकांक्षाओं इच्छाओं की स्वाभाविक बहुविधता के ध्यान का स्वरूप एवं प्रक्रिया
कारण अनेक धाराओं में विभक्त होकर निर्बल हो जाती है। ध्यान इन जैनाचार्यों ने ध्यान को 'चित्तनिरोध' कहा है।१२ चित्त का विभक्त एवं निर्बल चित्तधारा एक दिशा में मोड़ने का प्रयास है। जब निरोध हो जाना ध्यान है। दूसरे शब्दों में यह मन की चंचलता को ध्यान की साधना या अभ्यास से चित्तधाराओं को एक दिशा में बहने समाप्त करने का अभ्यास है। जब ध्यान सिद्ध हो जाता है तो चित्त की लगती है, तो न केवल वह सबल होती है, अपितु नियंत्रित होने से चंचलता स्वत: ही समाप्त हो जाती है। योगदर्शन में 'योग' को परिभाषित उसकी दिशा भी सम्यक् होती है। जिस प्रकार बांध विकीर्ण जलधाराओं करते हुए भी कहा गया है कि चित्तवृत्ति का निरोध ध्यान से ही सम्भव को एकत्रित कर उन्हें सबल और सुनियोजित करता है। जिस प्रकार बांध है। अत: ध्यान को साधना का आवश्यक अंग माना गया है। द्वारा सुनियोजित जल-शक्ति का सम्यक् उपयोग सम्भव हो पाता है उसी
गीता में मन की चंचलता के निरोध को वायु को रोकने के प्रकार ध्यान द्वारा सुनियोजित चेतनशक्ति का सम्यक् उपयोग सम्भव है। समान अति कठिन माना गया है।१३ उसमें उसके निरोध के दो उपाय संक्षेप में आत्मशक्ति के केन्द्रीकरण एवं उसे सम्यक् दिशा में बताये गये हैं- १. अभ्यास, २. वैराग्य। उत्तराध्ययन में मन रूपी दुष्ट नियोजित करने के लिए ध्यान-साधना आवश्यक है। वह चित्त वृत्तियों अश्व को निगृहीत करने के लिए श्रुत रूपी रस्सियों का प्रयोग आवश्यक की निरर्थक भागदौड़ को समाप्त कर हमें मानसिक विक्षोभों एवं विकारों बताया गया है।१४ चंचल चित्त की संकल्प-विकल्पात्मक तरंगें या से मुक्त रखता है। परिणामत: वह आध्यात्मिक शान्ति और निर्विकल्प वासनाजन्य आवेग सहज ही समाप्त नहीं हो जाते हैं। पहले उनकी भाग- चित्त की उपलब्धि का अन्यतम साधन है। दौड़ को समाप्त करना होता है। किन्तु यह वासनोन्मुख सक्रिय-मन या विक्षोभित चित्त निरोध के संकल्प मात्र से नियन्त्रित नहीं हो पाता है। पुन: ध्यान के पारम्परिक लाभ यदि उसे बलात् रोकने का प्रयत्न किया जाता है तो वह अधिक विक्षुब्ध ध्यानशतक (झाणाज्झयन) में ध्यान से होने वाले पारम्परिक होकर मुनष्य को पागलपन के कगार पर पहुँचा देता है, जैसे तीव्र गति एवं व्यावहारिक लाभों की विस्तृत चर्चा हैं। उसमें कहा गया हैं कि धर्म से चलते हुए वाहन को यकायक रोकने का प्रयत्न भयंकर दुर्घटना का ध्यान से शुभास्रव, संवर, निर्जरा और देवलोक के सुख प्राप्त होते हैं। ही कारण बनता है, उसी प्रकार चित्त की चंचलता का एकाएक निरोध शुक्ल ध्यान के भी प्रथम दो चरणों का परिणाम शुभास्रव एवं अनुत्तर विक्षिप्तता का कारण बनता है।
देवलोक के सुख हैं, जबकि शुक्ल ध्यान के अन्तिम दो चरणों का फल
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org