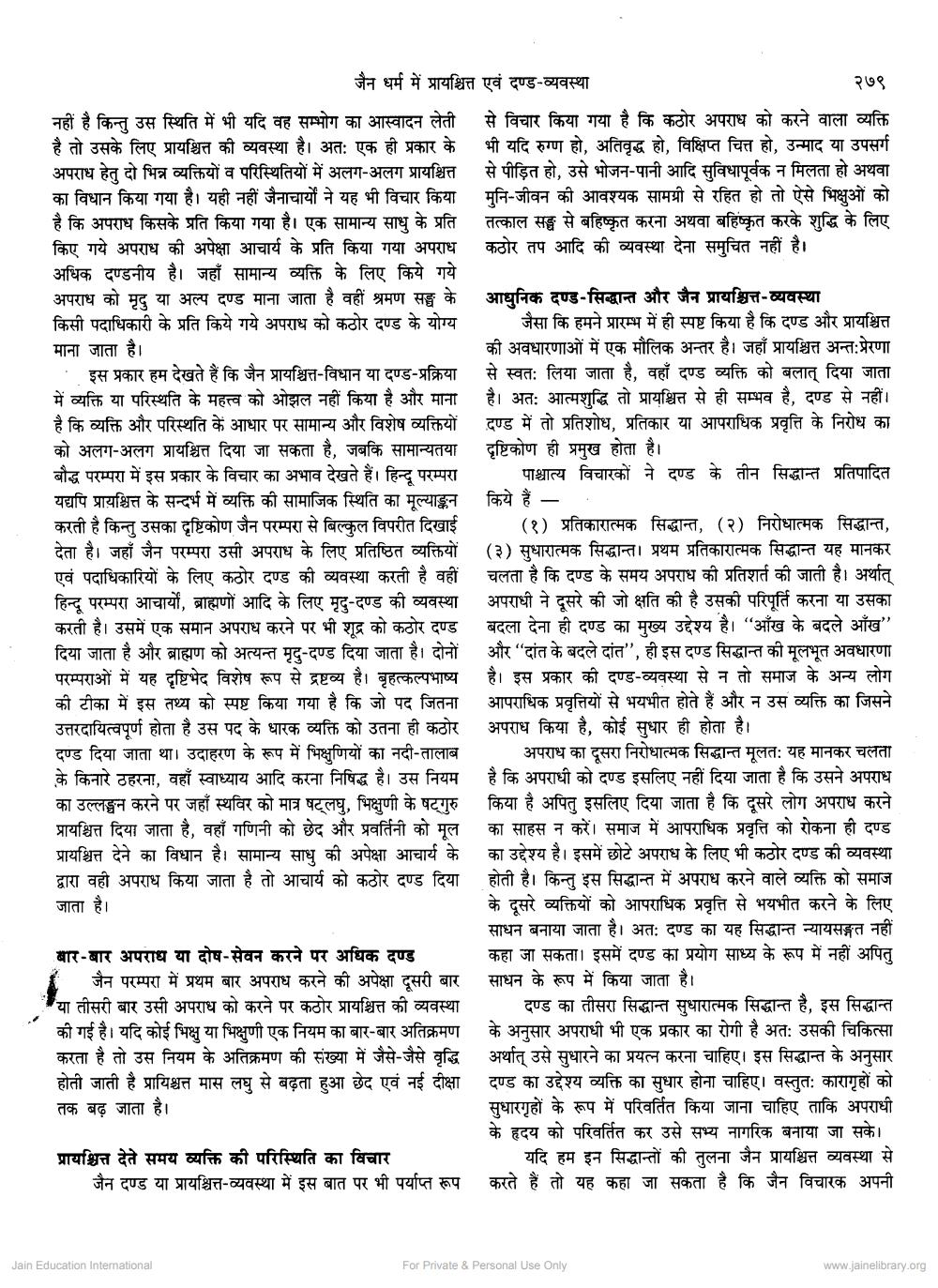________________
जैन धर्म में प्रायश्चित्त एवं दण्ड-व्यवस्था
नहीं है किन्तु उस स्थिति में भी यदि वह सम्भोग का आस्वादन लेती है तो उसके लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था है। अतः एक ही प्रकार के अपराध हेतु दो भिन्न व्यक्तियों व परिस्थितियों में अलग-अलग प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। यही नहीं जैनाचार्यों ने यह भी विचार किया है कि अपराध किसके प्रति किया गया है। एक सामान्य साधु के प्रति किए गये अपराध की अपेक्षा आचार्य के प्रति किया गया अपराध अधिक दण्डनीय है जहाँ सामान्य व्यक्ति के लिए किये गये अपराध को मृदु या अल्प दण्ड माना जाता है वहीं श्रमण सङ्घ के किसी पदाधिकारी के प्रति किये गये अपराध को कठोर दण्ड के योग्य माना जाता है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन प्रायश्चित विधान या दण्ड प्रक्रिया में व्यक्ति या परिस्थति के महत्त्व को ओझल नहीं किया है और माना है कि व्यक्ति और परिस्थति के आधार पर सामान्य और विशेष व्यक्तियों को अलग-अलग प्रायश्चित्त दिया जा सकता है, जबकि सामान्यतया बौद्ध परम्परा में इस प्रकार के विचार का अभाव देखते हैं। हिन्दू परम्परा यद्यपि प्रायश्चित्त के सन्दर्भ में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का मूल्याइन करती है किन्तु उसका दृष्टिकोण जैन परम्परा से बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है। जहाँ जैन परम्परा उसी अपराध के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं पदाधिकारियों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था करती है वहीं हिन्दू परम्परा आचार्यों, ब्राह्मणों आदि के लिए मृदु-दण्ड की व्यवस्था करती है। उसमें एक समान अपराध करने पर भी शूद्र को कठोर दण्ड दिया जाता है और ब्राह्मण को अत्यन्त मृदु-दण्ड दिया जाता है। दोनों परम्पराओं में यह दृष्टिभेद विशेष रूप से द्रष्टव्य है। बृहत्कल्पभाष्य की टीका में इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है कि जो पद जितना उत्तरदायित्वपूर्ण होता है उस पद के धारक व्यक्ति को उतना ही कठोर दण्ड दिया जाता था। उदाहरण के रूप में भिक्षुणियों का नदी तालाब के किनारे ठहरना, वहाँ स्वाध्याय आदि करना निषिद्ध है। उस नियम का उल्लङ्घन करने पर जहाँ स्थविर को मात्र पलघु, भिक्षुणी के षटगुरु प्रायश्चित दिया जाता है, वहाँ गणिनी को छेद और प्रवर्तिनी को मूल प्रायश्चित्त देने का विधान है सामान्य साधु की अपेक्षा आचार्य के द्वारा वही अपराध किया जाता है तो आचार्य को कठोर दण्ड दिया जाता है।
बार-बार अपराध या दोष सेवन करने पर अधिक दण्ड
जैन परम्परा में प्रथम बार अपराध करने की अपेक्षा दूसरी बार या तीसरी बार उसी अपराध को करने पर कठोर प्रायश्चित्त की व्यवस्था की गई है। यदि कोई भिक्षु या भिक्षुणी एक नियम का बार-बार अतिक्रमण करता है तो उस नियम के अतिक्रमण की संख्या में जैसे-जैसे वृद्धि होती जाती है प्रायिश्चत्त मास लघु से बढ़ता हुआ छेद एवं नई दीक्षा तक बढ़ जाता है।
प्रायश्चित्त देते समय व्यक्ति की परिस्थिति का विचार
जैन दण्ड या प्रायश्चित्त-व्यवस्था में इस बात पर भी पर्याप्त रूप
Jain Education International
२७९
से विचार किया गया है कि कठोर अपराध को करने वाला व्यक्ति भी यदि रुग्ण हो, अतिवृद्ध हो, विक्षिप्त चित्त हो, उन्माद या उपसर्ग से पीड़ित हो, उसे भोजन-पानी आदि सुविधापूर्वक न मिलता हो अथवा मुनि-जीवन की आवश्यक सामग्री से रहित हो तो ऐसे भिक्षुओं को तत्काल सङ्घ से बहिष्कृत करना अथवा बहिष्कृत करके शुद्धि के लिए कठोर तप आदि की व्यवस्था देना समुचित नहीं है।
आधुनिक दण्ड- सिद्धान्त और जैन प्रायश्चित्त-व्यवस्था
जैसा कि हमने प्रारम्भ में ही स्पष्ट किया है कि दण्ड और प्रायश्चित्त की अवधारणाओं में एक मौलिक अन्तर है जहाँ प्रायश्चित्त अन्त: प्रेरणा से स्वतः लिया जाता है, वहाँ दण्ड व्यक्ति को बलात् दिया जाता है। अतः आत्मशुद्धि तो प्रायश्चित्त से ही सम्भव है, दण्ड से नहीं । दण्ड में तो प्रतिशोध प्रतिकार या आपराधिक प्रवृत्ति के निरोध का दृष्टिकोण ही प्रमुख होता है।
पाश्चात्य विचारकों ने दण्ड के तीन सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं
(१) प्रतिकारात्मक सिद्धान्त (२) निरोधात्मक सिद्धान्त, (३) सुधारात्मक सिद्धान्त । प्रथम प्रतिकारात्मक सिद्धान्त यह मानकर चलता है कि दण्ड के समय अपराध की प्रतिशर्त की जाती है। अर्थात् अपराधी ने दूसरे की जो क्षति की है उसकी परिपूर्ति करना या उसका बदला देना ही दण्ड का मुख्य उद्देश्य है। "आँख के बदले आँख" और “दांत के बदले दांत", ही इस दण्ड सिद्धान्त की मूलभूत अवधारणा है । इस प्रकार की दण्ड-व्यवस्था से न तो समाज के अन्य लोग आपराधिक प्रवृत्तियों से भयभीत होते हैं और न उस व्यक्ति का जिसने अपराध किया है, कोई सुधार ही होता है।
अपराध का दूसरा निरोधात्मक सिद्धान्त मूलतः यह मानकर चलता है कि अपराधी को दण्ड इसलिए नहीं दिया जाता है कि उसने अपराध किया है अपितु इसलिए दिया जाता है कि दूसरे लोग अपराध करने का साहस न करें। समाज में आपराधिक प्रवृत्ति को रोकना ही दण्ड का उद्देश्य है। इसमें छोटे अपराध के लिए भी कठोर दण्ड की व्यवस्था होती है। किन्तु इस सिद्धान्त में अपराध करने वाले व्यक्ति को समाज के दूसरे व्यक्तियों को आपराधिक प्रवृत्ति से भयभीत करने के लिए साधन बनाया जाता है। अतः दण्ड का यह सिद्धान्त न्यायसङ्गत नहीं कहा जा सकता। इसमें दण्ड का प्रयोग साध्य के रूप में नहीं अपितु साधन के रूप में किया जाता है।
-
दण्ड का तीसरा सिद्धान्त सुधारात्मक सिद्धान्त है, इस सिद्धान्त के अनुसार अपराधी भी एक प्रकार का रोगी है अतः उसकी चिकित्सा अर्थात् उसे सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। इस सिद्धान्त के अनुसार दण्ड का उद्देश्य व्यक्ति का सुधार होना चाहिए। वस्तुतः कारागृहों को सुधारगृहों के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए ताकि अपराधी के हृदय को परिवर्तित कर उसे सभ्य नागरिक बनाया जा सके।
यदि हम इन सिद्धान्तों की तुलना जैन प्रायश्चित्त व्यवस्था से करते हैं तो यह कहा जा सकता है कि जैन विचारक अपनी
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org.