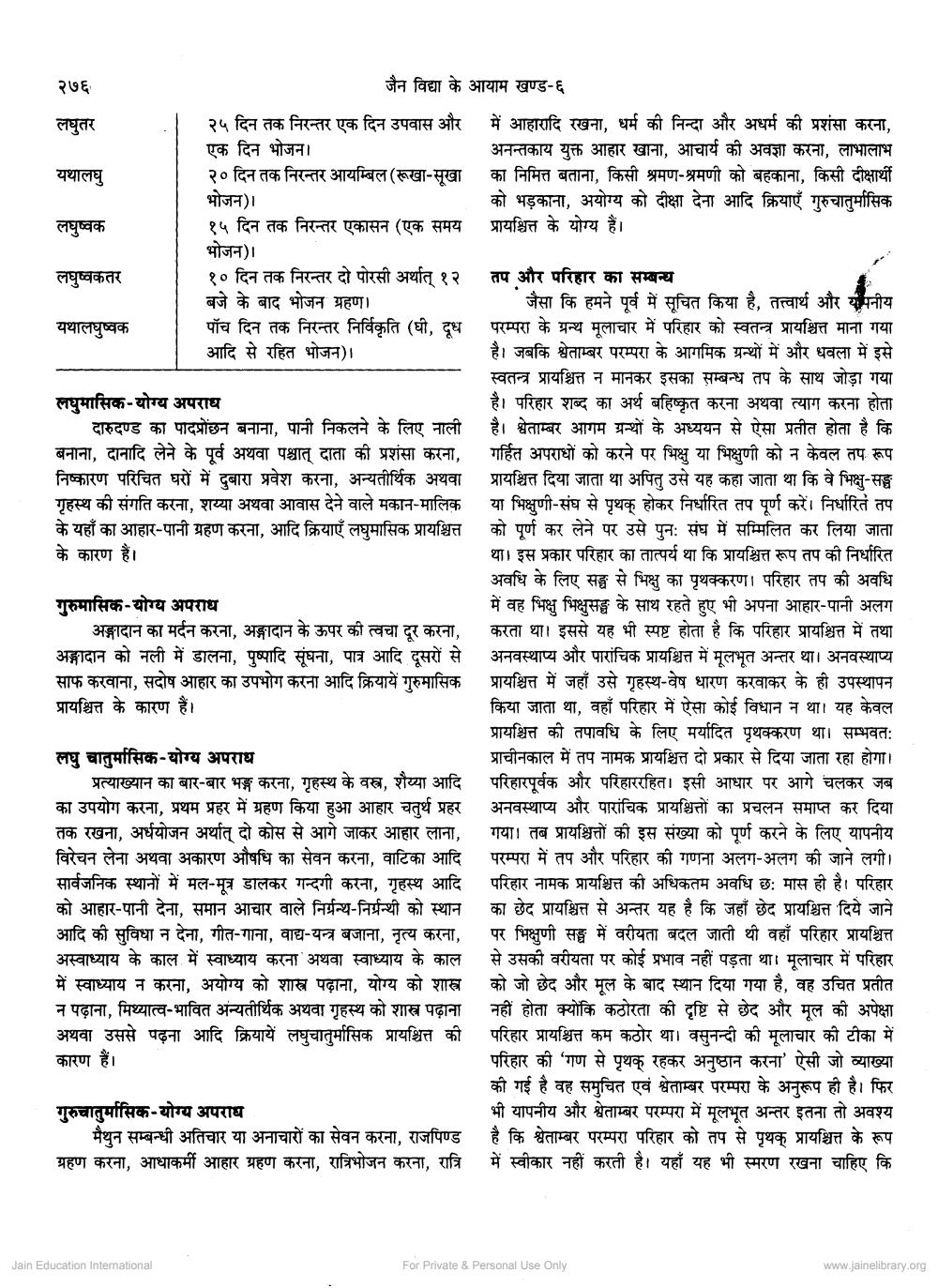________________
२७६
जैन विद्या के आयाम खण्ड-६ लघुतर
२५ दिन तक निरन्तर एक दिन उपवास और में आहारादि रखना, धर्म की निन्दा और अधर्म की प्रशंसा करना, एक दिन भोजन।
अनन्तकाय युक्त आहार खाना, आचार्य की अवज्ञा करना, लाभालाभ यथालघु
२० दिन तक निरन्तर आयम्बिल (रूखा-सूखा का निमित्त बताना, किसी श्रमण-श्रमणी को बहकाना, किसी दीक्षार्थी भोजन)।
को भड़काना, अयोग्य को दीक्षा देना आदि क्रियाएँ गुरुचातुर्मासिक लघुष्वक
१५ दिन तक निरन्तर एकासन (एक समय प्रायश्चित्त के योग्य हैं।
भोजन)। लघुष्वकतर १० दिन तक निरन्तर दो पोरसी अर्थात् १२ तप और परिहार का सम्बन्ध बजे के बाद भोजन ग्रहण।
जैसा कि हमने पूर्व में सूचित किया है, तत्त्वार्थ और यमनीय यथालघुष्वक पाँच दिन तक निरन्तर निर्विकृति (घी, दूध परम्परा के ग्रन्थ मूलाचार में परिहार को स्वतन्त्र प्रायश्चित्त माना गया आदि से रहित भोजन)।
है। जबकि श्वेताम्बर परम्परा के आगमिक ग्रन्थों में और धवला में इसे
स्वतन्त्र प्रायश्चित्त न मानकर इसका सम्बन्ध तप के साथ जोड़ा गया लघुमासिक-योग्य अपराध
है। परिहार शब्द का अर्थ बहिष्कृत करना अथवा त्याग करना होता दारुदण्ड का पादपोंछन बनाना, पानी निकलने के लिए नाली है। श्वेताम्बर आगम ग्रन्थों के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि बनाना, दानादि लेने के पूर्व अथवा पश्चात् दाता की प्रशंसा करना, गर्हित अपराधों को करने पर भिक्षु या भिक्षुणी को न केवल तप. रूप निष्कारण परिचित घरों में दुबारा प्रवेश करना, अन्यतीर्थिक अथवा प्रायश्चित्त दिया जाता था अपितु उसे यह कहा जाता था कि वे भिक्षु-सङ्घ गृहस्थ की संगति करना, शय्या अथवा आवास देने वाले मकान-मालिक या भिक्षुणी-संघ से पृथक् होकर निर्धारित तप पूर्ण करें। निर्धारित तप के यहाँ का आहार-पानी ग्रहण करना, आदि क्रियाएँ लघुमासिक प्रायश्चित्त को पूर्ण कर लेने पर उसे पुन: संघ में सम्मिलित कर लिया जाता के कारण हैं।
था। इस प्रकार परिहार का तात्पर्य था कि प्रायश्चित्त रूप तप की निर्धारित
अवधि के लिए सङ्घ से भिक्षु का पृथक्करण। परिहार तप की अवधि गुरुमासिक-योग्य अपराध
में वह भिक्षु भिक्षुसङ्घ के साथ रहते हुए भी अपना आहार-पानी अलग अङ्गादान का मर्दन करना, अङ्गादान के ऊपर की त्वचा दूर करना, करता था। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि परिहार प्रायश्चित्त में तथा अङ्गादान को नली में डालना, पुष्पादि सूंघना, पात्र आदि दूसरों से अनवस्थाप्य और पारांचिक प्रायश्चित्त में मूलभूत अन्तर था। अनवस्थाप्य साफ करवाना, सदोष आहार का उपभोग करना आदि क्रियायें गुरुमासिक प्रायश्चित्त में जहाँ उसे गृहस्थ-वेष धारण करवाकर के ही उपस्थापन प्रायश्चित्त के कारण हैं।
किया जाता था, वहाँ परिहार में ऐसा कोई विधान न था। यह केवल
प्रायश्चित्त की तपावधि के लिए मर्यादित पृथक्करण था। सम्भवत: लघु चातुर्मासिक-योग्य अपराध
प्राचीनकाल में तप नामक प्रायश्चित्त दो प्रकार से दिया जाता रहा होगा। प्रत्याख्यान का बार-बार भङ्ग करना, गृहस्थ के वस्त्र, शैय्या आदि परिहारपूर्वक और परिहाररहित। इसी आधार पर आगे चलकर जब का उपयोग करना, प्रथम प्रहर में ग्रहण किया हुआ आहार चतुर्थ प्रहर अनवस्थाप्य और पारांचिक प्रायश्चित्तों का प्रचलन समाप्त कर दिया तक रखना, अर्धयोजन अर्थात् दो कोस से आगे जाकर आहार लाना, गया। तब प्रायश्चित्तों की इस संख्या को पूर्ण करने के लिए यापनीय विरेचन लेना अथवा अकारण औषधि का सेवन करना, वाटिका आदि परम्परा में तप और परिहार की गणना अलग-अलग की जाने लगी। सार्वजनिक स्थानों में मल-मूत्र डालकर गन्दगी करना, गृहस्थ आदि परिहार नामक प्रायश्चित्त की अधिकतम अवधि छ: मास ही है। परिहार को आहार-पानी देना, समान आचार वाले निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी को स्थान का छेद प्रायश्चित्त से अन्तर यह है कि जहाँ छेद प्रायश्चित्त दिये जाने आदि की सुविधा न देना, गीत-गाना, वाद्य-यन्त्र बजाना, नृत्य करना, पर भिक्षुणी सङ्घ में वरीयता बदल जाती थी वहाँ परिहार प्रायश्चित्त अस्वाध्याय के काल में स्वाध्याय करना अथवा स्वाध्याय के काल से उसकी वरीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। मूलाचार में परिहार में स्वाध्याय न करना, अयोग्य को शास्त्र पढ़ाना, योग्य को शास्त्र को जो छेद और मूल के बाद स्थान दिया गया है, वह उचित प्रतीत न पढ़ाना, मिथ्यात्व-भावित अन्यतीर्थिक अथवा गृहस्थ को शास्त्र पढ़ाना नहीं होता क्योंकि कठोरता की दृष्टि से छेद और मूल की अपेक्षा अथवा उससे पढ़ना आदि क्रियायें लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त की परिहार प्रायश्चित्त कम कठोर था। वसुनन्दी की मूलाचार की टीका में कारण हैं।
परिहार की 'गण से पृथक् रहकर अनुष्ठान करना' ऐसी जो व्याख्या
की गई है वह समुचित एवं श्वेताम्बर परम्परा के अनुरूप ही है। फिर गुरुचातुर्मासिक-योग्य अपराध
भी यापनीय और श्वेताम्बर परम्परा में मूलभूत अन्तर इतना तो अवश्य __ मैथुन सम्बन्धी अतिचार या अनाचारों का सेवन करना, राजपिण्ड है कि श्वेताम्बर परम्परा परिहार को तप से पृथक् प्रायश्चित्त के रूप ग्रहण करना, आधाकर्मी आहार ग्रहण करना, रात्रिभोजन करना, रात्रि में स्वीकार नहीं करती है। यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org