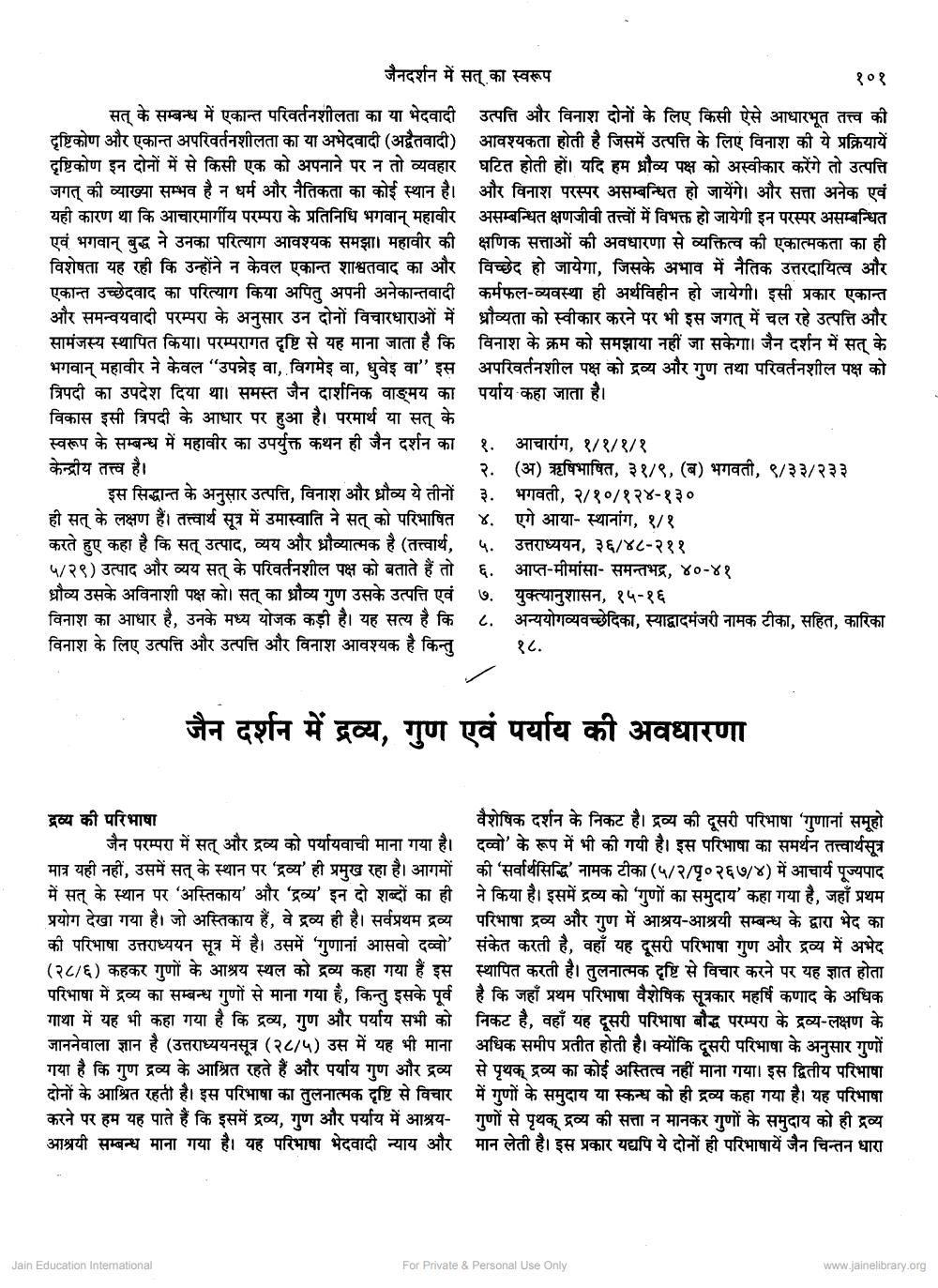________________
जैनदर्शन में सत् का स्वरूप
१०१
सत् के सम्बन्ध में एकान्त परिवर्तनशीलता का या भेदवादी उत्पत्ति और विनाश दोनों के लिए किसी ऐसे आधारभूत तत्त्व की दृष्टिकोण और एकान्त अपरिवर्तनशीलता का या अभेदवादी (अद्वैतवादी) आवश्यकता होती है जिसमें उत्पत्ति के लिए विनाश की ये प्रक्रियायें दृष्टिकोण इन दोनों में से किसी एक को अपनाने पर न तो व्यवहार घटित होती हों। यदि हम ध्रौव्य पक्ष को अस्वीकार करेंगे तो उत्पत्ति जगत् की व्याख्या सम्भव है न धर्म और नैतिकता का कोई स्थान है। और विनाश परस्पर असम्बन्धित हो जायेंगे। और सत्ता अनेक एवं यही कारण था कि आचारमार्गीय परम्परा के प्रतिनिधि भगवान् महावीर असम्बन्धित क्षणजीवी तत्त्वों में विभक्त हो जायेगी इन परस्पर असम्बन्धित एवं भगवान् बुद्ध ने उनका परित्याग आवश्यक समझा। महावीर की क्षणिक सत्ताओं की अवधारणा से व्यक्तित्व की एकात्मकता का ही विशेषता यह रही कि उन्होंने न केवल एकान्त शाश्वतवाद का और विच्छेद हो जायेगा, जिसके अभाव में नैतिक उत्तरदायित्व और एकान्त उच्छेदवाद का परित्याग किया अपितु अपनी अनेकान्तवादी कर्मफल-व्यवस्था ही अर्थविहीन हो जायेगी। इसी प्रकार एकान्त और समन्वयवादी परम्परा के अनुसार उन दोनों विचारधाराओं में ध्रौव्यता को स्वीकार करने पर भी इस जगत् में चल रहे उत्पत्ति और सामंजस्य स्थापित किया। परम्परागत दृष्टि से यह माना जाता है कि विनाश के क्रम को समझाया नहीं जा सकेगा। जैन दर्शन में सत् के भगवान् महावीर ने केवल “उपन्नेइ वा, विगमेइ वा, धुवेइ वा" इस अपरिवर्तनशील पक्ष को द्रव्य और गुण तथा परिवर्तनशील पक्ष को त्रिपदी का उपदेश दिया था। समस्त जैन दार्शनिक वाङ्मय का पर्याय कहा जाता है। विकास इसी त्रिपदी के आधार पर हुआ है। परमार्थ या सत् के स्वरूप के सम्बन्ध में महावीर का उपर्युक्त कथन ही जैन दर्शन का १. आचारांग, १/१/१/१ केन्द्रीय तत्त्व है।
२. (अ) ऋषिभाषित, ३१/९, (ब) भगवती, ९/३३/२३३ इस सिद्धान्त के अनुसार उत्पत्ति, विनाश और ध्रौव्य ये तीनों ३. भगवती, २/१०/१२४-१३० ही सत् के लक्षण हैं। तत्त्वार्थ सूत्र में उमास्वाति ने सत् को परिभाषित ४. एगे आया- स्थानांग, १/१ करते हुए कहा है कि सत् उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यात्मक है (तत्त्वार्थ, ५. उत्तराध्ययन, ३६/४८-२११ ५/२९) उत्पाद और व्यय सत् के परिवर्तनशील पक्ष को बताते हैं तो ६. आप्त-मीमांसा- समन्तभद्र, ४०-४१ ध्रौव्य उसके अविनाशी पक्ष को। सत् का ध्रौव्य गुण उसके उत्पत्ति एवं ७. युक्त्यानुशासन, १५-१६ विनाश का आधार है, उनके मध्य योजक कड़ी है। यह सत्य है कि ८. अन्ययोगव्यवच्छेदिका, स्याद्वादमंजरी नामक टीका, सहित, कारिका विनाश के लिए उत्पत्ति और उत्पत्ति और विनाश आवश्यक है किन्तु १८.
जैन दर्शन में द्रव्य, गुण एवं पर्याय की अवधारणा
सत्र में है। उस
क हा गया हैं इस
द्रव्य की परिभाषा
वैशेषिक दर्शन के निकट है। द्रव्य की दूसरी परिभाषा 'गुणानां समूहो जैन परम्परा में सत् और द्रव्य को पर्यायवाची माना गया है। दव्वो' के रूप में भी की गयी है। इस परिभाषा का समर्थन तत्त्वार्थसूत्र मात्र यही नहीं, उसमें सत् के स्थान पर 'द्रव्य' ही प्रमुख रहा है। आगमों की ‘सर्वार्थसिद्धि' नामक टीका (५/२/पृ०२६७/४) में आचार्य पूज्यपाद में सत् के स्थान पर 'अस्तिकाय' और 'द्रव्य' इन दो शब्दों का ही ने किया है। इसमें द्रव्य को 'गुणों का समुदाय' कहा गया है, जहाँ प्रथम प्रयोग देखा गया है। जो अस्तिकाय हैं, वे द्रव्य ही है। सर्वप्रथम द्रव्य परिभाषा द्रव्य और गुण में आश्रय-आश्रयी सम्बन्ध के द्वारा भेद का की परिभाषा उत्तराध्ययन सूत्र में है। उसमें 'गुणानां आसवो दव्वो' संकेत करती है, वहाँ यह दूसरी परिभाषा गुण और द्रव्य में अभेद (२८/६) कहकर गुणों के आश्रय स्थल को द्रव्य कहा गया हैं इस स्थापित करती है। तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर यह ज्ञात होता परिभाषा में द्रव्य का सम्बन्ध गुणों से माना गया है, किन्तु इसके पूर्व है कि जहाँ प्रथम परिभाषा वैशेषिक सूत्रकार महर्षि कणाद के अधिक गाथा में यह भी कहा गया है कि द्रव्य, गुण और पर्याय सभी को निकट है, वहाँ यह दूसरी परिभाषा बौद्ध परम्परा के द्रव्य-लक्षण के जाननेवाला ज्ञान है (उत्तराध्ययनसूत्र (२८/५) उस में यह भी माना अधिक समीप प्रतीत होती है। क्योंकि दूसरी परिभाषा के अनुसार गुणों गया है कि गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं और पर्याय गुण और द्रव्य से पृथक् द्रव्य का कोई अस्तित्व नहीं माना गया। इस द्वितीय परिभाषा दोनों के आश्रित रहती है। इस परिभाषा का तुलनात्मक दृष्टि से विचार में गुणों के समुदाय या स्कन्ध को ही द्रव्य कहा गया है। यह परिभाषा करने पर हम यह पाते हैं कि इसमें द्रव्य, गुण और पर्याय में आश्रय- गुणों से पृथक् द्रव्य की सत्ता न मानकर गुणों के समुदाय को ही द्रव्य आश्रयी सम्बन्ध माना गया है। यह परिभाषा भेदवादी न्याय और मान लेती है। इस प्रकार यद्यपि ये दोनों ही परिभाषायें जैन चिन्तन धारा
जहाँ प्रथम परिभा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org