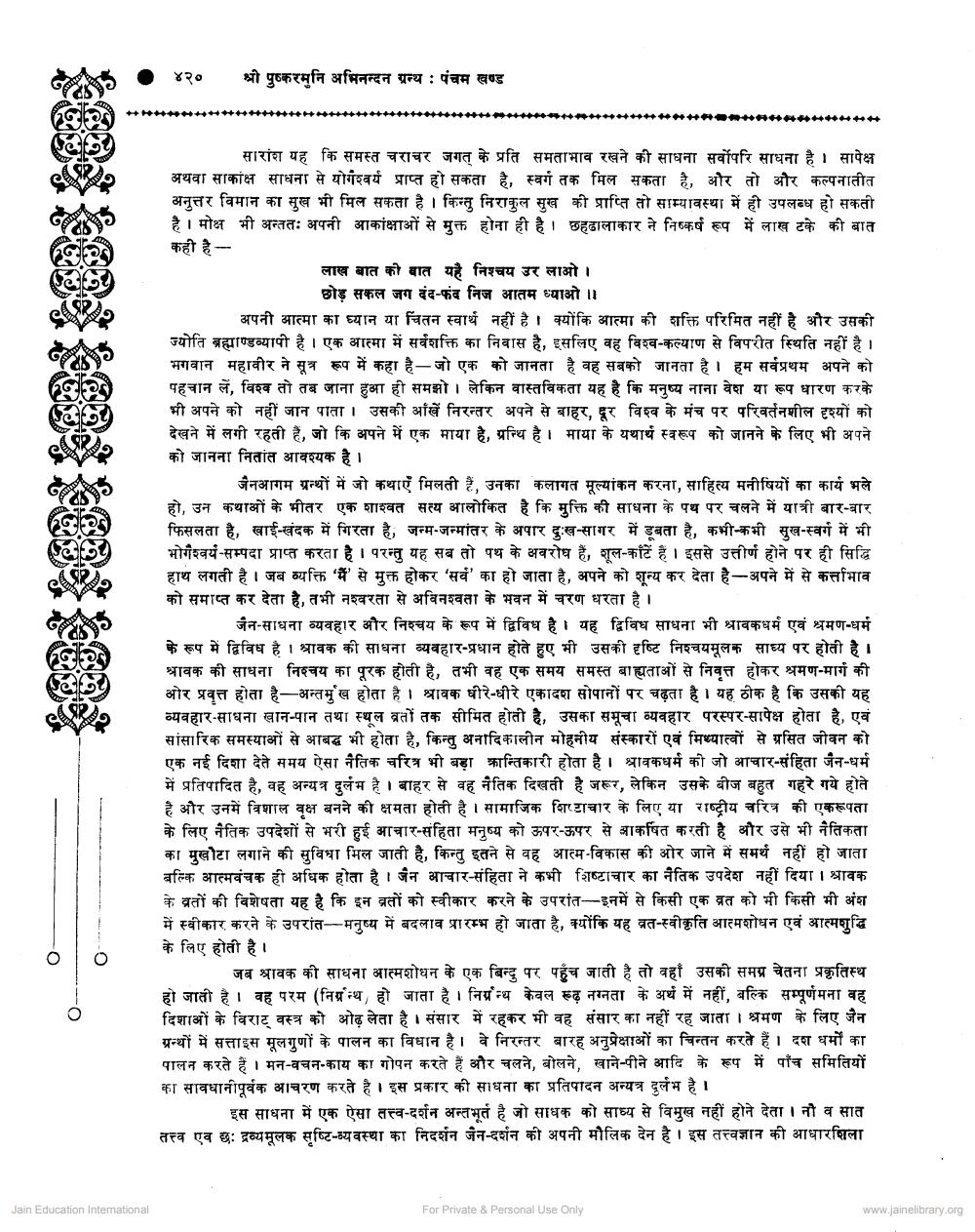________________
४२०
श्री पुष्करमुनि अभिनन्दन ग्रन्थ : पंचम खण्ड
सारांश यह कि समस्त चराचर जगत् के प्रति समताभाव रखने की साधना सर्वोपरि साधना है। सापेक्ष अथवा साकांक्ष साधना से योगश्वर्य प्राप्त हो सकता है, स्वर्ग तक मिल सकता है, और तो और कल्पनातीत अनुत्तर विमान का सुख भी मिल सकता है । किन्तु निराकुल सुख की प्राप्ति तो साम्यावस्था में ही उपलब्ध हो सकती है । मोक्ष भी अन्ततः अपनी आकांक्षाओं से मुक्त होना ही है। छहढालाकार ने निष्कर्ष रूप में लाख टके की बात कही है
लाख बात की बात यह निश्चय उर लाओ।
छोड सकल जग बंद-फंद निज आतम ध्याओ। अपनी आत्मा का ध्यान या चिंतन स्वार्थ नहीं है। क्योंकि आत्मा की शक्ति परिमित नहीं है और उसकी ज्योति ब्रह्माण्डव्यापी है । एक आत्मा में सर्वशक्ति का निवास है, इसलिए वह विश्व-कल्याण से विपरीत स्थिति नहीं है। भगवान महावीर ने सूत्र रूप में कहा है-जो एक को जानता है वह सबको जानता है। हम सर्वप्रथम अपने को पहचान लें, विश्व तो तब जाना हुआ ही समझो। लेकिन वास्तविकता यह है कि मनुष्य नाना वेश या रूप धारण करके भी अपने को नहीं जान पाता। उसकी आँखें निरन्तर अपने से बाहर, दूर विश्व के मंच पर परिवर्तनशील दृश्यों को देखने में लगी रहती हैं, जो कि अपने में एक माया है, प्रन्थि है। माया के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए भी अपने को जानना नितांत आवश्यक है।
जैनआगम ग्रन्थों में जो कथाएँ मिलती हैं, उनका कलागत मूल्यांकन करना, साहित्य मनीषियों का कार्य भले हो, उन कथाओं के भीतर एक शाश्वत सत्य आलोकित है कि मुक्ति की साधना के पथ पर चलने में यात्री बार-बार फिसलता है, खाई-खंदक में गिरता है, जन्म-जन्मांतर के अपार दुःख-सागर में डूबता है, कभी-कभी सुख-स्वर्ग में भी भोगैश्वर्य-सम्पदा प्राप्त करता है। परन्तु यह सब तो पथ के अवरोध हैं, शूल-काँटें हैं। इससे उत्तीर्ण होने पर ही सिद्धि हाथ लगती है। जब व्यक्ति 'मैं' से मुक्त होकर 'सर्व' का हो जाता है, अपने को शून्य कर देता है-अपने में से कर्ताभाव को समाप्त कर देता है, तभी नश्वरता से अविनश्वता के भवन में चरण धरता है।
जन-साधना व्यवहार और निश्चय के रूप में द्विविध है। यह द्विविध साधना भी श्रावकधर्म एवं श्रमण-धर्म के रूप में द्विविध है । श्रावक की साधना व्यवहार-प्रधान होते हुए भी उसकी दृष्टि निश्चयमूलक साध्य पर होती है । श्रावक की साधना निश्चय का पूरक होती है, तभी वह एक समय समस्त बाह्यताओं से निवृत्त होकर श्रमण-मार्ग की ओर प्रवृत्त होता है-अन्तर्मुख होता है। श्रावक धीरे-धीरे एकादश सोपानों पर चढ़ता है। यह ठीक है कि उसकी यह व्यवहार-साधना खान-पान तथा स्थूल व्रतों तक सीमित होती है, उसका समूचा व्यवहार परस्पर-सापेक्ष होता है, एवं सांसारिक समस्याओं से आबद्ध भी होता है, किन्तु अनादिकालीन मोहनीय संस्कारों एवं मिथ्यात्वों से ग्रसित जीवन को एक नई दिशा देते समय ऐसा नैतिक चरित्र भी बड़ा क्रान्तिकारी होता है। श्रावकधर्म को जो आचार-संहिता जैन-धर्म में प्रतिपादित है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। बाहर से वह नैतिक दिखती है जरूर, लेकिन उसके बीज बहुत गहरे गये होते है और उनमें विशाल वृक्ष बनने की क्षमता होती है । सामाजिक शिष्टाचार के लिए या राष्ट्रीय चरित्र की एकरूपता के लिए नैतिक उपदेशों से भरी हुई आचार-संहिता मनुष्य को ऊपर-ऊपर से आकर्षित करती है और उसे भी नैतिकता का मुखौटा लगाने की सुविधा मिल जाती है, किन्तु इतने से वह आत्म-विकास की ओर जाने में समर्थ नहीं हो जाता बल्कि आत्मवंचक ही अधिक होता है । जैन आचार-संहिता ने कभी शिष्टाचार का नैतिक उपदेश नहीं दिया । श्रावक के व्रतों की विशेषता यह है कि इन ब्रतों को स्वीकार करने के उपरांत-इनमें से किसी एक व्रत को भी किसी भी अंश में स्वीकार करने के उपरांत-मनुष्य में बदलाव प्रारम्भ हो जाता है, क्योंकि यह व्रत-स्वीकृति आत्मशोधन एवं आत्मशुद्धि के लिए होती है।
जब श्रावक की साधना आत्मशोधन के एक बिन्दु पर पहुंच जाती है तो वहाँ उसकी समग्र चेतना प्रकृतिस्थ हो जाती है। वह परम (निर्ग्रन्थ, हो जाता है । निर्ग्रन्थ केवल रूढ़ नग्नता के अर्थ में नहीं, बल्कि सम्पूर्णमना वह दिशाओं के विराट् वस्त्र को ओढ़ लेता है । संसार में रहकर भी वह संसार का नहीं रह जाता । श्रमण के लिए जैन ग्रन्थों में सत्ताइस मूलगुणों के पालन का विधान है। वे निरन्तर बारह अनुप्रेक्षाओं का चिन्तन करते हैं। दश धर्मों का पालन करते हैं । मन-वचन-काय का गोपन करते हैं और चलने, बोलने, खाने-पीने आदि के रूप में पाँच समितियों का सावधानीपूर्वक आचरण करते है। इस प्रकार की साधना का प्रतिपादन अन्यत्र दुर्लभ है।
इस साधना में एक ऐसा तत्त्व-दर्शन अन्तभूर्त है जो साधक को साध्य से विमुख नहीं होने देता । नौ व सात तत्त्व एव छः द्रव्यमूलक सृष्टि-व्यवस्था का निदर्शन जैन-दर्शन की अपनी मौलिक देन है। इस तत्त्वज्ञान की आधारशिला
००
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org