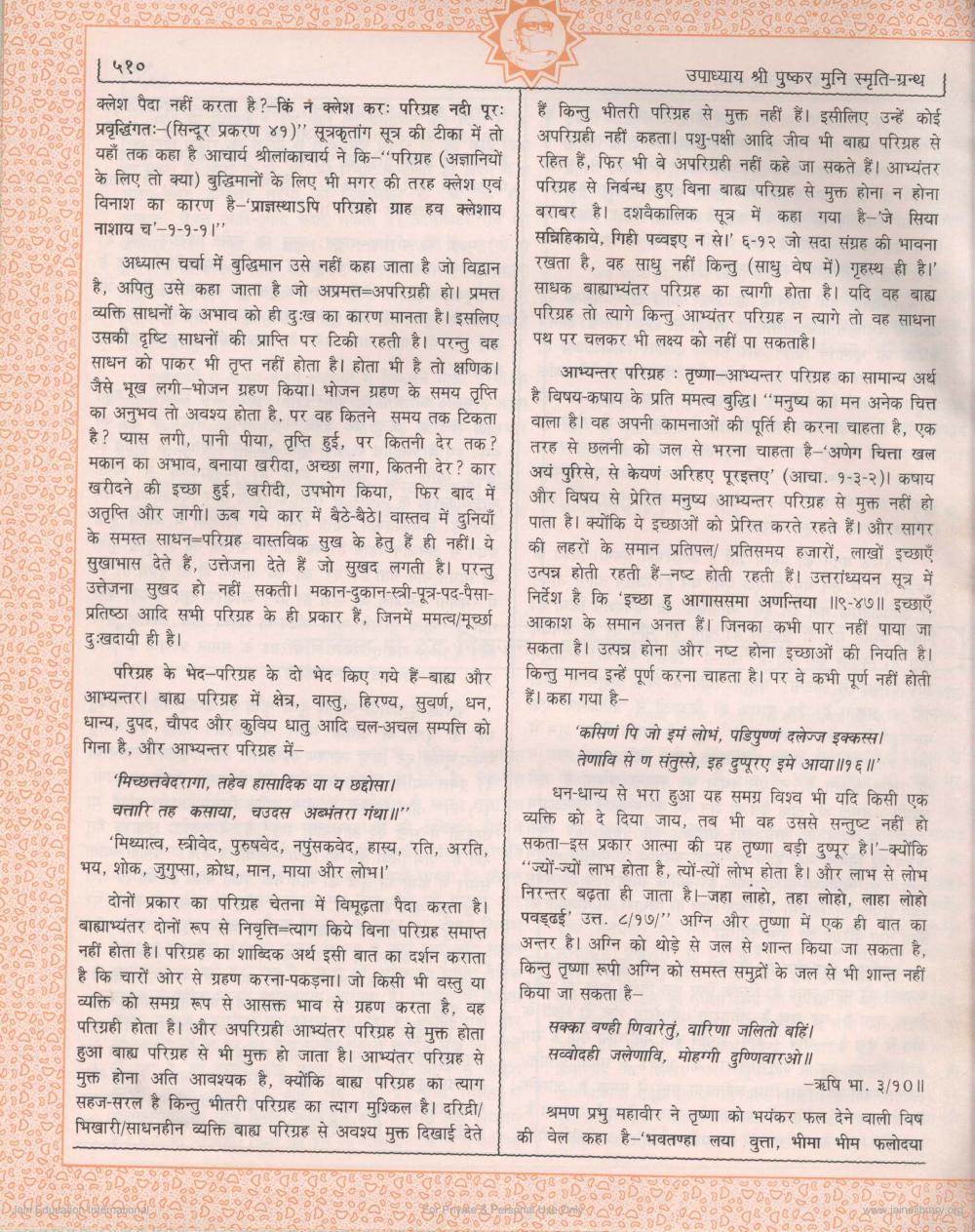________________
५१०
क्लेश पैदा नहीं करता है? किं ने क्लेश करः परिग्रह नदी पूर प्रवृद्धिंगत:- (सिन्दूर प्रकरण ४१) सूत्रकृतांग सूत्र की टीका में तो यहाँ तक कहा है आचार्य श्रीनांकाचार्य ने कि- "परिग्रह ( अज्ञानियों के लिए तो क्या ) बुद्धिमानों के लिए भी मगर की तरह क्लेश एवं विनाश का कारण है-प्राज्ञस्थाऽपि परिग्रहो ग्राह व क्लेशाय नाशाय च - १-१-१1"
अध्यात्म चर्चा में बुद्धिमान उसे नहीं कहा जाता है जो विद्वान है, अपितु उसे कहा जाता है जो अप्रमत्त अपरिग्रही हो । प्रमत्त व्यक्ति साधनों के अभाव को ही दुःख का कारण मानता है। इसलिए उसकी दृष्टि साधनों की प्राप्ति पर टिकी रहती है। परन्तु वह साधन को पाकर भी तृप्त नहीं होता है। होता भी है तो क्षणिक जैसे भूख लगी- भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण के समय तृप्ति का अनुभव तो अवश्य होता है, पर वह कितने समय तक टिकता है? प्यास लगी, पानी पीया, तृप्ति हुई, पर कितनी देर तक ? मकान का अभाव, बनाया खरीदा, अच्छा लगा, कितनी देर ? कार खरीदने की इच्छा हुई, खरीदी, उपभोग किया, फिर बाद में अतृप्ति और जागी । ऊब गये कार में बैठे-बैठे। वास्तव में दुनियाँ के समस्त साधन परिग्रह वास्तविक सुख के हेतु हैं ही नहीं ये सुखाभास देते हैं, उत्तेजना देते हैं जो सुखद लगती है। परन्तु उत्तेजना सुखद हो नहीं सकती। मकान-दुकान स्त्री- पुत्र-पद-पैसाप्रतिष्ठा आदि सभी परिग्रह के ही प्रकार हैं, जिनमें ममत्व / मूर्च्छा दुःखदायी ही है।
परिग्रह के भेद-परिग्रह के दो भेद किए गये हैं- बाह्य और आभ्यन्तर । बाह्य परिग्रह में क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दुपद, चौपद और कुविय धातु आदि चल-अचल सम्पत्ति को गिना है, और आभ्यन्तर परिग्रह में
'मिच्छत्तवेदरागा, तहेव हासादिक या य छद्दोसा । चत्तारि तह कसाया, चउदस अब्भंतरा गंथा ॥"
'मिथ्यात्व, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया और लोभा'
वह
दोनों प्रकार का परिग्रह चेतना में विमूढ़ता पैदा करता है। बाह्याभ्यंतर दोनों रूप से निवृत्ति त्याग किये बिना परिग्रह समाप्त नहीं होता है। परिग्रह का शाब्दिक अर्थ इसी बात का दर्शन कराता है कि चारों ओर से ग्रहण करना -पकड़ना। जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति को समग्र रूप से आसक्त भाव से ग्रहण करता है, परिग्रही होता है और अपरिग्रही आभ्यंतर परिग्रह से मुक्त होता हुआ बाह्य परिग्रह से भी मुक्त हो जाता है। आभ्यंतर परिग्रह से मुक्त होना अति आवश्यक है, क्योंकि बाह्य परिग्रह का त्याग सहज-सरल है किन्तु भीतरी परिग्रह का त्याग मुश्किल है। दरिद्री / भिखारी / साधनहीन व्यक्ति बाह्य परिग्रह से अवश्य मुक्त दिखाई देते
rational
उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि स्मृति ग्रन्थ
हैं किन्तु भीतरी परिग्रह से मुक्त नहीं हैं। इसीलिए उन्हें कोई अपरिग्रही नहीं कहता पशु-पक्षी आदि जीव भी बाह्य परिग्रह से रहित हैं, फिर भी वे अपरिग्रही नहीं कहे जा सकते हैं। आभ्यंतर परिग्रह से निर्बन्ध हुए बिना बाह्य परिग्रह से मुक्त होना न होना बराबर है। दशवैकालिक सूत्र में कहा गया है 'जे सिया सन्निहिकाये, गिही पव्वइए न से।' ६-१२ जो सदा संग्रह की भावना रखता है, वह साधु नहीं किन्तु (साधु वेष में) गृहस्थ ही है।' साधक बाह्याभ्यंतर परिग्रह का त्यागी होता है। यदि वह बाह्य परिग्रह तो त्यागे किन्तु आभ्यंतर परिग्रह न त्यागे तो वह साधना पथ पर चलकर भी लक्ष्य को नहीं पा सकता है।
आभ्यन्तर परिग्रह: तृष्णा-आभ्यन्तर परिग्रह का सामान्य अर्थ है विषय कषाय के प्रति ममत्व बुद्धि। "मनुष्य का मन अनेक चित्त वाला है। वह अपनी कामनाओं की पूर्ति ही करना चाहता है, एक तरह से छलनी को जल से भरना चाहता है-'अणेग चित्ता खल अयं पुरिसे से केयणं अरिहए पूरइत्तए' (आचा. १-३-२)। कषाय और विषय से प्रेरित मनुष्य आभ्यन्तर परिग्रह से मुक्त नहीं हो पाता है। क्योंकि ये इच्छाओं को प्रेरित करते रहते हैं। और सागर की लहरों के समान प्रतिपल / प्रतिसमय हजारों लाखों इच्छाएँ उत्पन्न होती रहती हैं-नष्ट होती रहती हैं। उत्तराध्ययन सूत्र में निर्देश है कि 'इच्छा हु आगाससमा अणन्तिया ॥९-४७॥ इच्छाएँ आकाश के समान अनत्त हैं। जिनका कभी पार नहीं पाया जा सकता है। उत्पन्न होना और नष्ट होना इच्छाओं की नियति है। किन्तु मानव इन्हें पूर्ण करना चाहता है। पर वे कभी पूर्ण नहीं होती हैं। कहा गया है
'कसिणं पि जो इमं लोभं, पडिपुण्णं दलेज्ज इक्कस्स । तेणावि से ण संतुस्से, इह दुप्पूरए इमे आया ॥ १६ ॥।'
9
धन-धान्य से भरा हुआ यह समग्र विश्व भी यदि किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाय तब भी वह उससे सन्तुष्ट नहीं हो सकता - इस प्रकार आत्मा की यह तृष्णा बड़ी दुष्पूर है।'- क्योंकि "ज्यों-ज्यों लाभ होता है, त्यों-त्यों लोभ होता है और लाभ से लोभ निरन्तर बढ़ता ही जाता है। जहा लाहो, तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई' उत्त. ८/१७/" अग्नि और तृष्णा में एक ही बात का अन्तर है। अग्नि को थोड़े से जल से शान्त किया जा सकता है, किन्तु तृष्णा रूपी अग्नि को समस्त समुद्रों के जल से भी शान्त नहीं किया जा सकता है
सक्का यही निवारेतुं वारिणा जलितो वहि। सव्योदही जलेणावि, मोहग्गी दुष्णिवारओ ॥
Personal she
-ऋषि भा. ३/१०॥
श्रमण प्रभु महावीर ने तृष्णा को भयंकर फल देने वाली विष की वेल कहा है- 'भवतण्हा लया वृत्ता, भीमा भीम फलोदया
www.jainelibrary
8:0