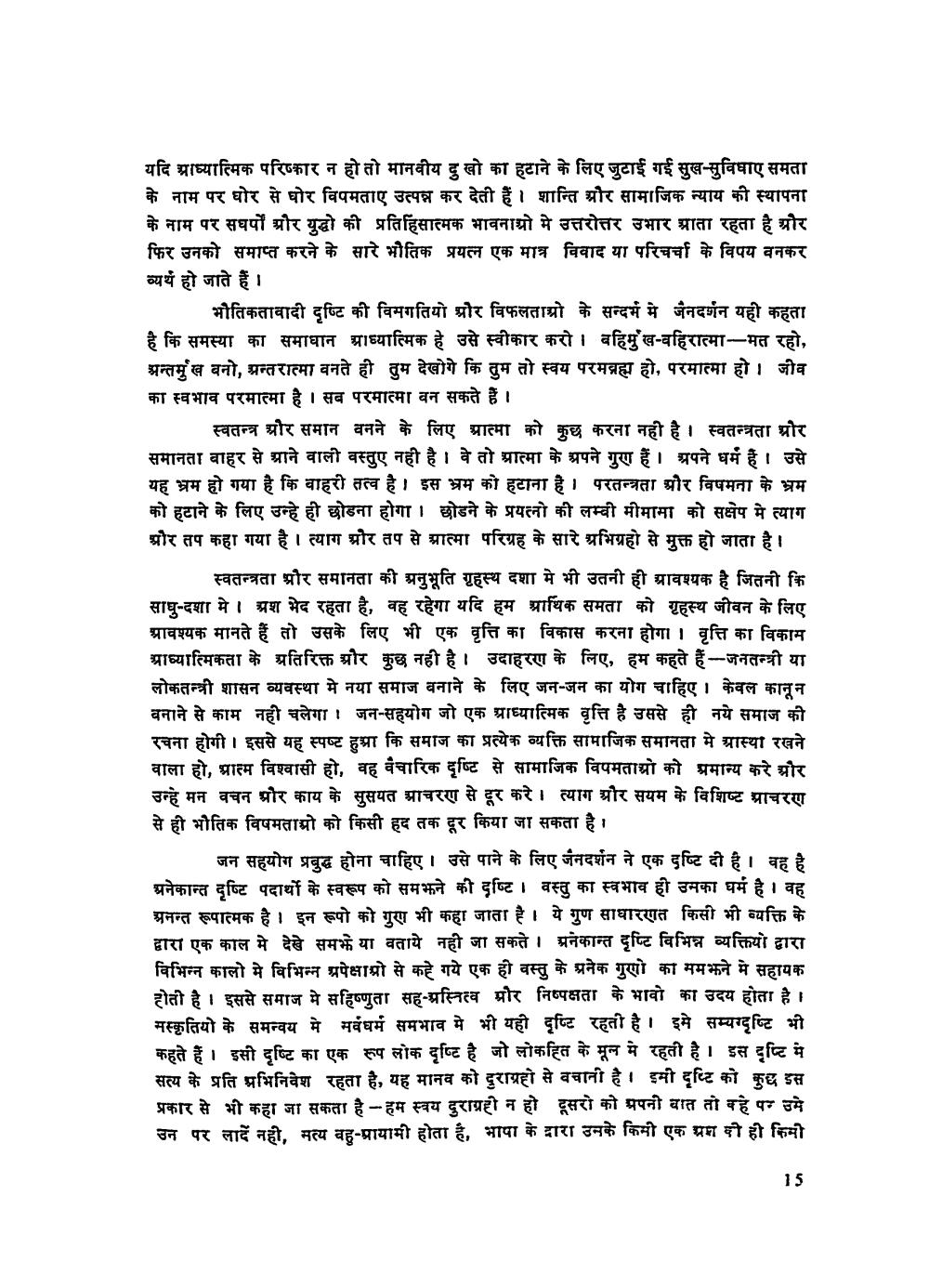________________
यदि प्राध्यात्मिक परिष्कार न हो तो मानवीय दुखो का हटाने के लिए जुटाई गई सुख-सुविधाए समता के नाम पर घोर से घोर विपमताए उत्पन्न कर देती हैं। शान्ति और सामाजिक न्याय की स्थापना के नाम पर सघों और युद्धो की प्रतिहिंसात्मक भावनायो मे उत्तरोत्तर उभार पाता रहता है और फिर उनको समाप्त करने के सारे भौतिक प्रयल एक मात्र विवाद या परिचर्चा के विपय वनकर व्यर्थ हो जाते हैं।
भौतिकतावादी दृष्टि की विमगतियो और विफलतापो के सन्दर्भ मे जैनदर्शन यही कहता है कि समस्या का समाधान आध्यात्मिक हे उसे स्वीकार करो। बहिर्मुख-वहिरात्मा-मत रहो, अन्तर्मुख बनो, अन्तरात्मा बनते ही तुम देखोगे कि तुम तो स्वय परमब्रह्म हो, परमात्मा हो। जीव का स्वभाव परमात्मा है । सब परमात्मा बन सकते हैं।
स्वतन्त्र और समान बनने के लिए प्रात्मा को कुछ करना नही है। स्वतन्त्रता और समानता बाहर से आने वाली वस्तुए नही है। वे तो आत्मा के अपने गुण हैं। अपने धर्म हैं। उसे यह भ्रम हो गया है कि बाहरी तत्व है। इस भ्रम को हटाना है। परतन्त्रता और विषमता के भ्रम को हटाने के लिए उन्हे ही छोडना होगा। छोडने के प्रयत्नो की लम्बी मीमामा को सक्षेप में त्याग और तप कहा गया है। त्याग और तप से आत्मा परिग्रह के सारे अभिग्रहो से मुक्त हो जाता है।
स्वतन्त्रता और समानता की अनुभूति गृहस्थ दशा मे भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि साधु-दशा मे। अश भेद रहता है, वह रहेगा यदि हम आर्थिक समता को गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक मानते हैं तो उसके लिए भी एक वृत्ति का विकास करना होगा। वृत्ति का विकास आध्यात्मिकता के अतिरिक्त और कुछ नही है। उदाहरण के लिए, हम कहते हैं-जनतन्त्री या लोकतन्त्री शासन व्यवस्था मे नया समाज बनाने के लिए जन-जन का योग चाहिए। केवल कानुन बनाने से काम नही चलेगा। जन-सहयोग जो एक आध्यात्मिक वृत्ति है उससे ही नये समाज की रचना होगी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक समानता मे आस्था रखने वाला हो, प्रात्म विश्वासी हो, वह वैचारिक दृष्टि से सामाजिक विषमतारो को अमान्य करे और उन्हे मन वचन और काय के सुसयत आचरण से दूर करे। त्याग और सयम के विशिष्ट आचरण से ही भौतिक विषमतामो को किसी हद तक दूर किया जा सकता है।
जन सहयोग प्रबुद्ध होना चाहिए। उसे पाने के लिए जनदर्शन ने एक दृष्टि दी है। वह है अनेकान्त दृष्टि पदार्थो के स्वरूप को समझने की दृष्टि । वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है। वह अनन्त रूपात्मक है। इन रूपो को गुण भी कहा जाता है। ये गुण साधारणत किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक काल मे देखे समझे या बताये नही जा सकते। अनेकान्त दृष्टि विभिन्न व्यक्तियो द्वारा विभिन्न कालो मे विभिन्न अपेक्षामो से कहे गये एक ही वस्तु के अनेक गुणो का ममझने में सहायक होती है। इससे समाज मे सहिष्णुता सह-अस्तित्व पोर निष्पक्षता के भावो का उदय होता है। मस्कृतियो के समन्वय मे मर्वधर्म समभाव मे भी यही दृष्टि रहती है। इमे सम्यग्दृष्टि भी कहते हैं । इसी दृष्टि का एक रूप लोक दृष्टि है जो लोकहित के मूल में रहती है। इस दृष्टि में सत्य के प्रति अभिनिवेश रहता है, यह मानव को दुराग्रहो से बचाती है। इमी दृष्टि को कुछ इस प्रकार से भी कहा जा सकता है -हम स्वय दुराग्रही न हो दूसरो को अपनी बात तो कहे पर उमे उन पर लादें नही, मत्य बहु-प्रायामी होता है, भाषा के द्वारा उनके किमी एक प्रश की ही किमी
15