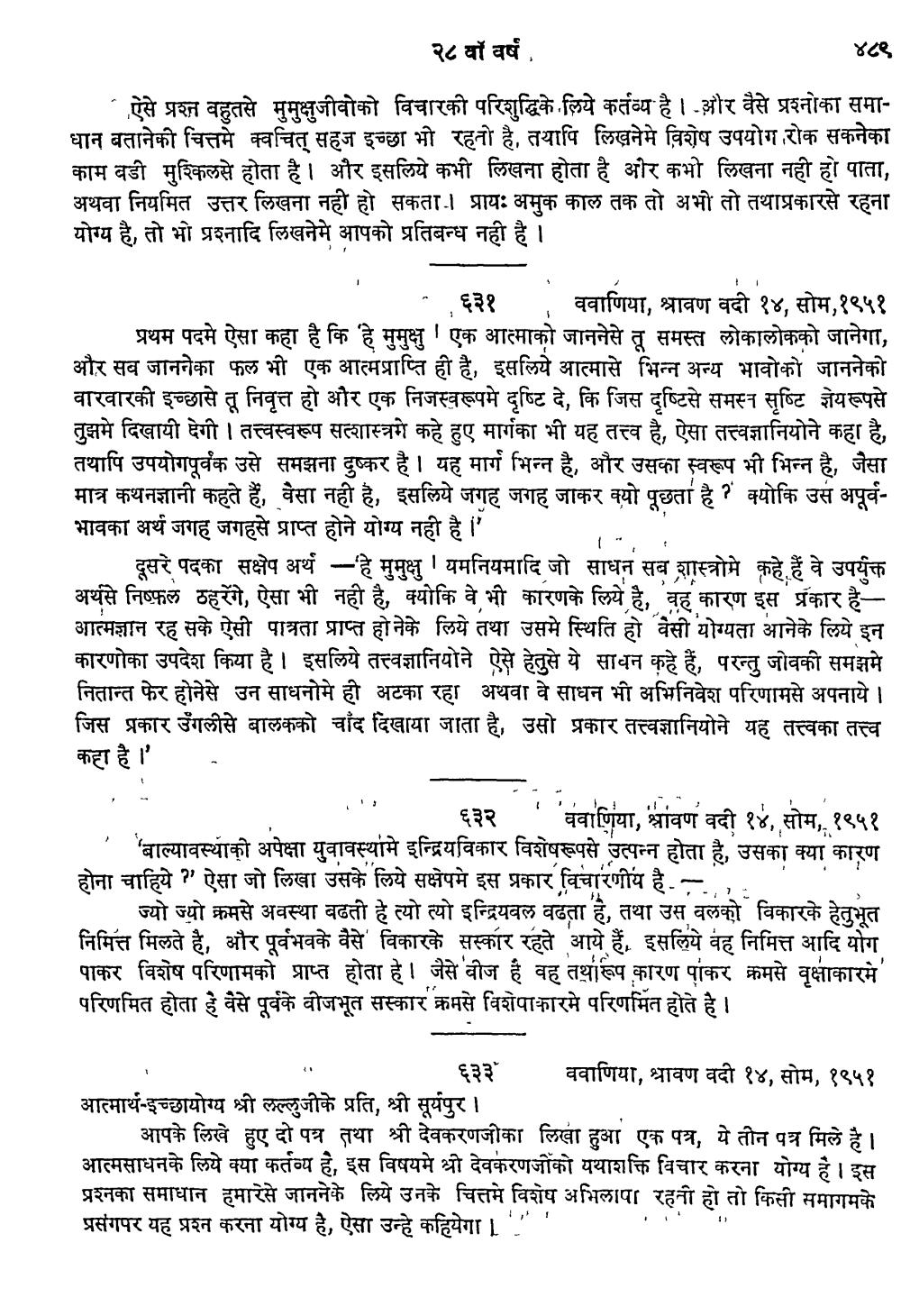________________
२८ वॉ वर्ष
४८९ ऐसे प्रश्न बहुतसे मुमुक्षुजीवोको विचारकी परिशुद्धिके लिये कर्तव्य है । और वैसे प्रश्नोका समाधान बतानेको चित्तमे क्वचित् सहज इच्छा भी रहती है, तयापि लिखनेमे विशेष उपयोग रोक सकनेका काम बडी मुश्किलसे होता है। और इसलिये कभी लिखना होता है और कभी लिखना नही हो पाता, अथवा नियमित उत्तर लिखना नही हो सकता.। प्रायः अमुक काल तक तो अभी तो तथाप्रकारसे रहना योग्य है, तो भो प्रश्नादि लिखनेमे आपको प्रतिबन्ध नही है।
- . ६३१ , ववाणिया, श्रावण वदी १४, सोम,१९५१ प्रथम पदमे ऐसा कहा है कि 'हे मुमुक्षु | एक आत्माको जाननेसे तू समस्त लोकालोकको जानेगा, और सब जाननेका फल भी एक आत्मप्राप्ति ही है, इसलिये आत्मासे भिन्न अन्य भावोको जाननेको वारवारकी इच्छासे तू निवृत्त हो और एक निजस्वरूपमे दृष्टि दे, कि जिस दृष्टिसे समस्त सृष्टि ज्ञेयरूपसे तुझमे दिखायी देगी । तत्त्वस्वरूप सत्शास्त्री कहे हुए मार्गका भी यह तत्त्व है, ऐसा तत्त्वज्ञानियोने कहा है, तथापि उपयोगपूर्वक उसे समझना दुष्कर है। यह मार्ग भिन्न है, और उसका स्वरूप भी भिन्न है, जैसा मात्र कथनज्ञानी कहते हैं, वैसा नहीं है, इसलिये जगह जगह जाकर क्यो पूछता है ? क्योकि उस अपूर्वभावका अर्थ जगह जगहसे प्राप्त होने योग्य नहीं है।'
दूसरे पदका सक्षेप अर्थ -'हे मुमुक्षु । यमनियमादि जो साधन सब शास्त्रोमे कहे हैं वे उपर्युक्त अर्थसे निष्फल ठहरेंगे, ऐसा भी नही है, क्योकि वे भी कारणके लिये है, वह कारण इस प्रकार हैआत्मज्ञान रह सके ऐसी पात्रता प्राप्त हो नेके लिये तथा उसमे स्थिति हो वैसी योग्यता आनेके लिये इन कारणोका उपदेश किया है। इसलिये तत्त्वज्ञानियोने ऐसे हेतुसे ये सावन कहे हैं, परन्तु जोवकी समझमे नितान्त फेर होनेसे उन साधनोमे ही अटका रहा अथवा वे साधन भी अभिनिवेश परिणामसे अपनाये । जिस प्रकार उँगलीसे बालकको चाँद दिखाया जाता है, उसी प्रकार तत्त्वज्ञानियोने यह तत्त्वका तत्त्व कहा है।' .
६३२ । 'वाणिया, श्रावण वदी १४, सोम, १९५१ 'बाल्यावस्थाको अपेक्षा युवावस्थामे इन्द्रियविकार विशेषरूपसे उत्पन्न होता है, उसका क्या कारण होना चाहिये " ऐसा जो लिखा उसके लिये सक्षेपमे इस प्रकार विचारणीय है.--,
ज्यो ज्यो क्रमसे अवस्था बढती हे त्यो त्यो इन्द्रियबल बढता है, तथा उस वलको विकारके हेतुभूत निमित्त मिलते है, और पूर्वभवके वैसे विकारके सस्कार रहते आये हैं, इसलिये वह निमित्त आदि योग पाकर विशेष परिणामको प्राप्त होता है। जैसे बीज है वह तथापि कारण पांकर क्रमसे वृक्षाकारमे परिणमित होता है वैसे पूर्वके वीजभूत सस्कार क्रमसे विशेपाकारमे परिणमित होते है।
६३३ ववाणिया, श्रावण वदी १४, सोम, १९५१ आत्मार्थ-इच्छायोग्य श्री लल्लुजीके प्रति, श्री सूर्यपुर ।
आपके लिखे हुए दो पत्र तथा श्री देवकरणजीका लिखा हुआ एक पत्र, ये तीन पत्र मिले है। आत्मसाधनके लिये क्या कर्तव्य है, इस विषयमे श्री देवकरणजोंको यथाशक्ति विचार करना योग्य है । इस प्रश्नका समाधान हमारेसे जाननेके लिये उनके चित्तमे विशेष अभिलापा रहती हो तो किसी समागमके प्रसंगपर यह प्रश्न करना योग्य है, ऐसा उन्हे कहियेगा।'