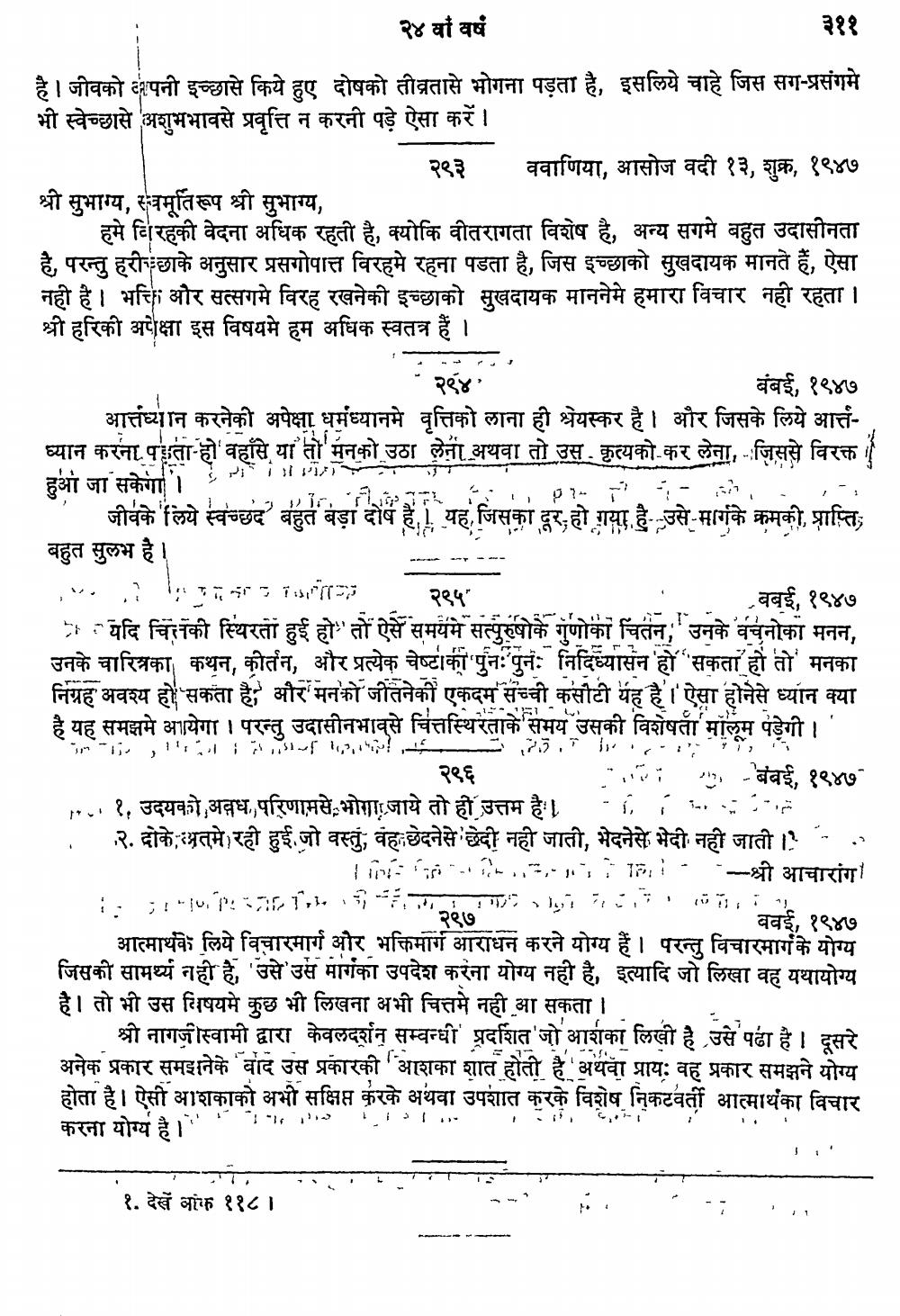________________
२४ वाँ वर्ष
३११
है । जीवको अपनी इच्छासे किये हुए दोषको तीव्रतासे भोगना पड़ता है, इसलिये चाहे जिस सग - प्रसंगमे भी स्वेच्छासे अशुभभावसे प्रवृत्ति न करनी पड़े ऐसा करें ।
२९३
वाणिया, आसोज वदी १३, शुक्र, १९४७
श्री सुभाग्य, स्त्रमूर्तिरूप श्री सुभाग्य, हमे
ही वेदना अधिक रहती है, क्योकि वीतरागता विशेष है, अन्य सगमे बहुत उदासीनता है, परन्तु हरीच्छा अनुसार प्रसंगोपात्त विरहमे रहना पडता है, जिस इच्छाको सुखदायक मानते हैं, ऐसा नही है । भक्ति और सत्सगमे विरह रखने की इच्छाको सुखदायक माननेमे हमारा विचार नही रहता । श्री हरिकी अपेक्षा इस विषय मे हम अधिक स्वतत्र हैं ।
२९४
बंबई, १९४७
आत्तंध्यान करनेकी अपेक्षा धर्मंध्यानमे वृत्तिको लाना ही श्रेयस्कर है । और जिसके लिये आध्यान करना पड़ता हो वहाँसे या तो मनको उठा लेना अथवा तो उस कृत्यको कर लेना, जिससे विरक्त ।। हुआ जा सकेगा।
ग
के
जीवके लिये स्वच्छंद बहुत बड़ा दोष हैं । यह, जिसका दूर हो गया है उसे मार्गके क्रमकी प्राप्ति, बहुत सुलभ है ।
"
उद
२९५
बबई, १९४७
2
यदि चितकी स्थिरतों हुई हो तो ऐसे समय मे सत्पुरुषोके गुणोका चितन, उनके वचनोका मनन, उनके चारित्रका कथन, कीर्तन, और प्रत्येक चेष्टा की पुनः पुनः निदिध्यासन हो सकता हो 'तो' मनका निग्रह अवश्य हो सकता है, और' मनको जीतनेकी एकदम सच्ची कसौटी यह है।' ऐसा होनेसे ध्यान क्या है यह समझमे आयेगा । परन्तु उदासीनभावसे चित्तस्थिरताके समय उसकी विशेषता मालूम पड़ेगी ।
F
11.
1
25.7
417
बंबई, १९४७
२९६
. . १, उदयको, अवध, परिणामसे, भोगा जाये तो ही उत्तम है।
२. दोके, अतमे) रही हुई, जो वस्तु, वह छेदने से छेदी नही जाती, भेदनेसे भेदी नही जाती | 2
1. TRU
-श्री आचारांग
121
ܐ ܸ ܕ ܯ
१. देखें ांक ११८ ।
"
7
ܐ
२९७
बबई, १९४७
आत्मार्थके लिये विचारमार्ग और भक्तिमार्ग आराधन करने योग्य हैं । परन्तु विचारमार्ग के योग्य जिसकी सामर्थ्य नही है, उसे उसे मार्गका उपदेश करना योग्य नही है, इत्यादि जो लिखा वह यथायोग्य है। तो भी उस विषयमे कुछ भी लिखना अभी चित्तमे नही आ सकता ।
श्री नागज़ स्वामी द्वारा केवलदर्शन सम्बन्धी प्रदर्शित जो आशका लिखी है उसे पढ़ा है । दूसरे अनेक प्रकार समझनेके "बाद उस प्रकारकी 'आशका शात होती है अथवा प्रायः वह प्रकार समझने योग्य होता है। ऐसी आशकाको अभी सक्षिप्त करके अथवा उपशात करके विशेष निकटवर्ती आत्मार्थंका विचार करना योग्य है ।
"""""
11
"