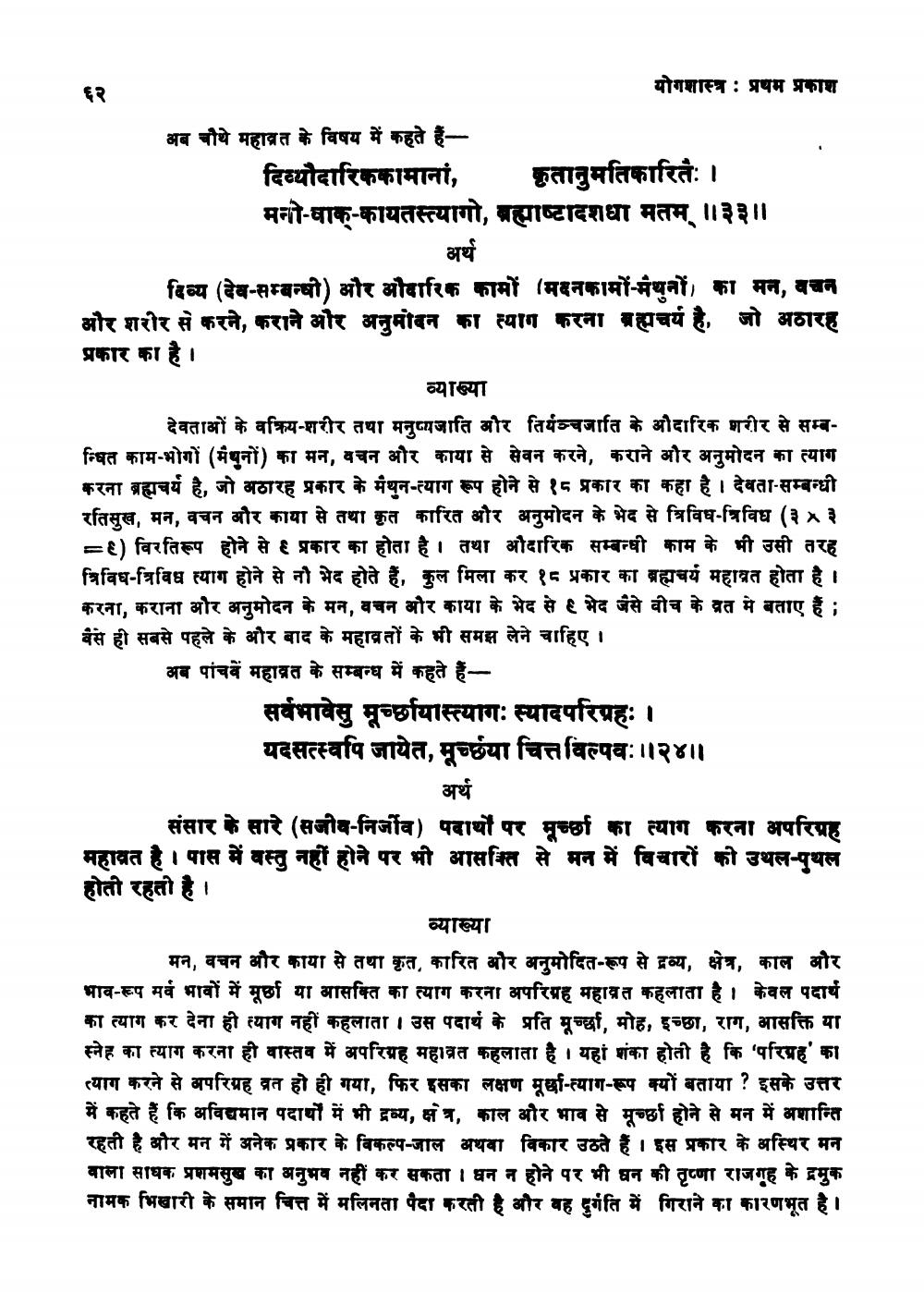________________
योगशास्त्र: प्रथम प्रकाश
अब चौथे महाव्रत के विषय में कहते हैं
दिव्यौदारिककामानां, कृतानुमतिकारितैः । मनो-वाक्-कायतस्त्यागो, ब्रह्माष्टादशधा मतम् ॥३३॥
अर्थ दिव्य (देव-सम्बन्धी) और औदारिक कामों (मनकामों-मैथुनों) का मन, बचन और शरीर से करने, कराने और अनुमोदन का त्याग करना ब्रह्मचर्य है, जो अठारह प्रकार का है।
व्याख्या देवताओं के वक्रिय-शरीर तथा मनुष्यजाति और तिर्यञ्चजाति के औदारिक शरीर से सम्बधित काम-भोगों (मैथुनों) का मन, वचन और काया से सेवन करने, कराने और अनुमोदन का त्याग करना ब्रह्मचर्य है, जो अठारह प्रकार के मथुन-त्याग रूप होने से १८ प्रकार का कहा है । देवता-सम्बन्धी रतिसुख, मन, वचन और काया से तथा कृत कारित और अनुमोदन के भेद से त्रिविध-त्रिविध (३ x ३ =९) विरतिरूप होने से ६ प्रकार का होता है। तथा औदारिक सम्बन्धी काम के भी उसी तरह त्रिविध-त्रिविध त्याग होने से नो भेद होते हैं, कुल मिला कर १८ प्रकार का ब्रह्मचर्य महावत होता है। करना, कराना और अनुमोदन के मन, वचन और काया के भेद से ९ भेद जैसे वीच के व्रत में बताए हैं। वैसे ही सबसे पहले के और बाद के महाव्रतों के भी समझ लेने चाहिए। अब पांचवें महावत के सम्बन्ध में कहते हैं
सर्वभावेसु मूर्छायास्त्यागः स्यादपरिग्रहः । यदसत्स्वपि जायेत, मूर्च्छया चित्तविल्पवः ।।२४॥
अर्थ संसार के सारे (सजीव-निर्जीव) पदार्थों पर मूर्छा का त्याग करना अपरिग्रह महावत है। पास में वस्तु नहीं होने पर भी आसक्ति से मन में विचारों को उथल-पुथल होती रहती है।
व्याख्या मन, वचन और काया से तथा कृत, कारित और अनुमोदित-रूप से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव-रूप मर्व भावों में मूळ या आसक्ति का त्याग करना अपरिग्रह महावत कहलाता है। केवल पदार्थ का त्याग कर देना ही त्याग नहीं कहलाता । उस पदार्थ के प्रति मूर्छा, मोह, इच्छा, राग, आसक्ति या स्नेह का त्याग करना ही वास्तव में अपरिग्रह महाव्रत कहलाता है । यहां शंका होती है कि 'परिग्रह का त्याग करने से अपरिग्रह व्रत हो ही गया, फिर इसका लक्षण मूर्या-त्याग-रूप क्यों बताया ? इसके उत्तर में कहते हैं कि अविद्यमान पदार्थों में भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से मूर्छा होने से मन में अशान्ति रहती है और मन में अनेक प्रकार के विकल्प-जाल अथवा विकार उठते हैं । इस प्रकार के अस्थिर मन वाला साधक प्रशमसुख का अनुभव नहीं कर सकता । धन न होने पर भी धन की तृष्णा राजगह के द्रमुक नामक भिखारी के समान चित्त में मलिनता पैदा करती है और वह दुर्गति में गिराने का कारणभूत है।