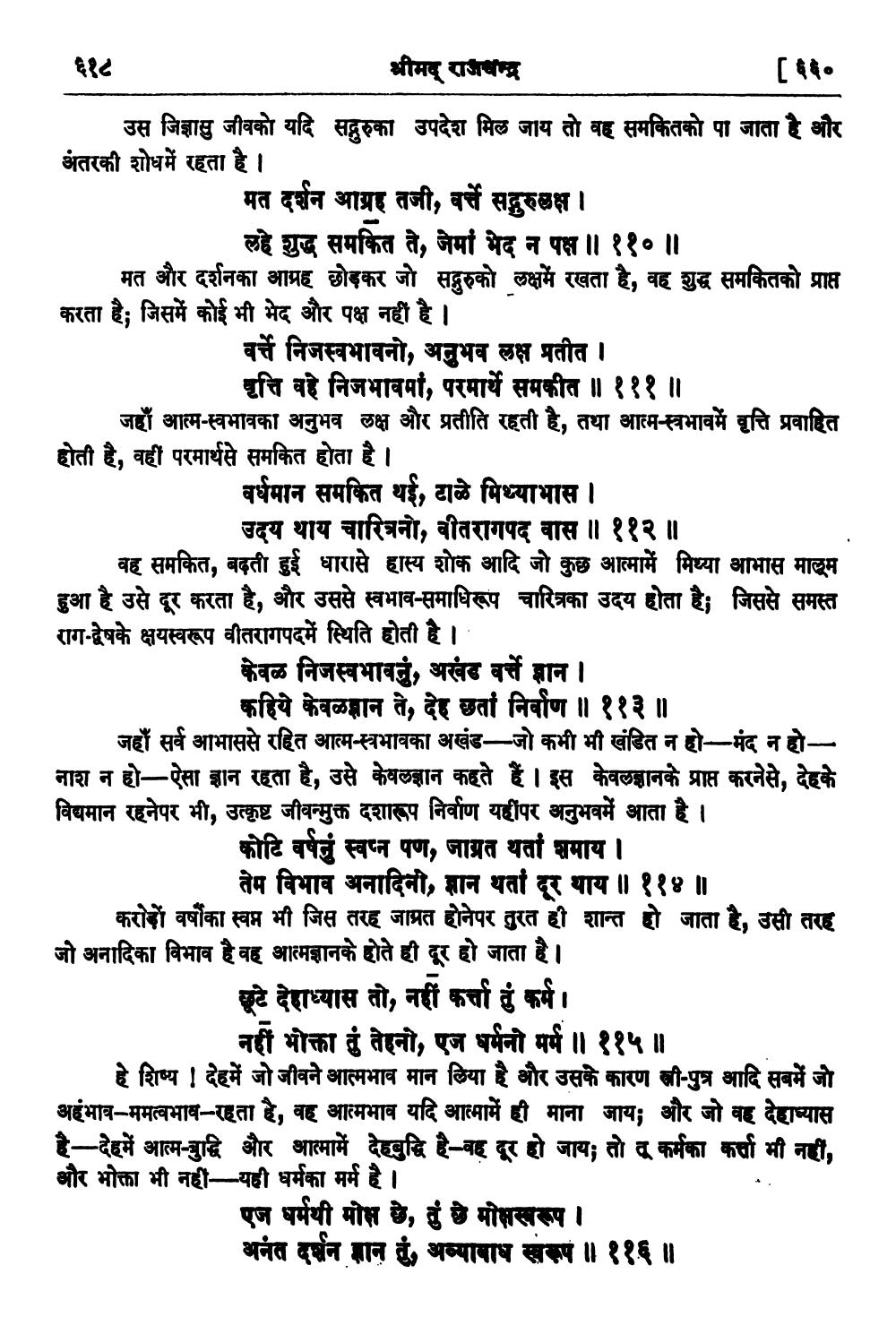________________
६१८
श्रीमद् राजचन्द्र
[६६० उस जिज्ञासु जीवको यदि सद्गुरुका उपदेश मिल जाय तो वह समकितको पा जाता है और अंतरकी शोधमें रहता है।
मत दर्शन आग्रह तजी, वर्षे सद्गुरुलक्ष ।
लहे शुद्ध समकित ते, जेमा भेद न पक्ष ॥ ११ ॥ मत और दर्शनका आग्रह छोड़कर जो सद्गुरुको लक्षमें रखता है, वह शुद्ध समकितको प्राप्त करता है, जिसमें कोई भी भेद और पक्ष नहीं है ।
वर्ने निजस्वभावनो, अनुभव लक्ष प्रतीत ।
वृत्ति वहे निजभावां, परमार्थे समकीत ॥ १११ ॥ जहाँ आत्म-स्वभावका अनुभव लक्ष और प्रतीति रहती है, तथा आत्म-स्वभावमें वृत्ति प्रवाहित होती है, वहीं परमार्थसे समकित होता है।
वर्धमान समकित थई, टाळे मिथ्याभास ।
उदय थाय चारित्रनो, वीतरागपद वास ॥ ११२ ॥ वह समकित, बढ़ती हुई धारासे हास्य शोक आदि जो कुछ आत्मामें मिथ्या आभास मालम हुआ है उसे दूर करता है, और उससे स्वभाव-समाधिरूप चारित्रका उदय होता है, जिससे समस्त राग-द्वेषके क्षयस्वरूप वीतरागपदमें स्थिति होती है।
केवळ निजस्वभावमुं, अखंड वर्ने ज्ञान ।
कहिये केवळज्ञान ते, देह छतां निर्वाण ॥ ११३ ॥ जहाँ सर्व आभाससे रहित आत्म-स्वभावका अखंड-जो कभी भी खंडित न हो-मंद न होनाश न हो-ऐसा ज्ञान रहता है, उसे केवलज्ञान कहते हैं । इस केवलज्ञानके प्राप्त करनेसे, देहके विद्यमान रहनेपर भी, उत्कृष्ट जीवन्मुक्त दशारूप निर्वाण यहींपर अनुभवमें आता है ।
कोटि वर्षनुं स्वप्न पण, जाग्रत था शमाय ।
तेम विभाव अनादिनी, ज्ञान थतां दूर थाय ॥ ११ ॥ करोड़ों वर्षों का स्वम भी जिस तरह जाग्रत होनेपर तुरत ही शान्त हो जाता है, उसी तरह जो अनादिका विभाव है वह आत्मज्ञानके होते ही दूर हो जाता है।
छूटे देहाध्यास तो, नहीं कर्ता तुं कर्म।
नहीं भोक्ता तुं तेहनो, एज धर्मनो मर्म ॥ ११५ ॥ हे शिष्य ! देहमें जो जीवने आत्मभाव मान लिया है और उसके कारण स्त्री-पुत्र आदि सबमें जो अहंभाव-ममत्वभाव-रहता है, वह आत्मभाव यदि आत्मामें ही माना जाय; और जो वह देहाभ्यास है-देहमें आत्म-बुद्धि और आत्मामें देहबुद्धि है-वह दूर हो जाया तो तू कर्मका कर्ता भी नहीं, और भोक्ता भी नहीं-यही धर्मका मर्म है।
एज धर्मयी मोल छ, तुं छे मोशखरूप । अनंत दर्शन शान हूँ, अन्यावाष खरूप ॥ ११६ ॥