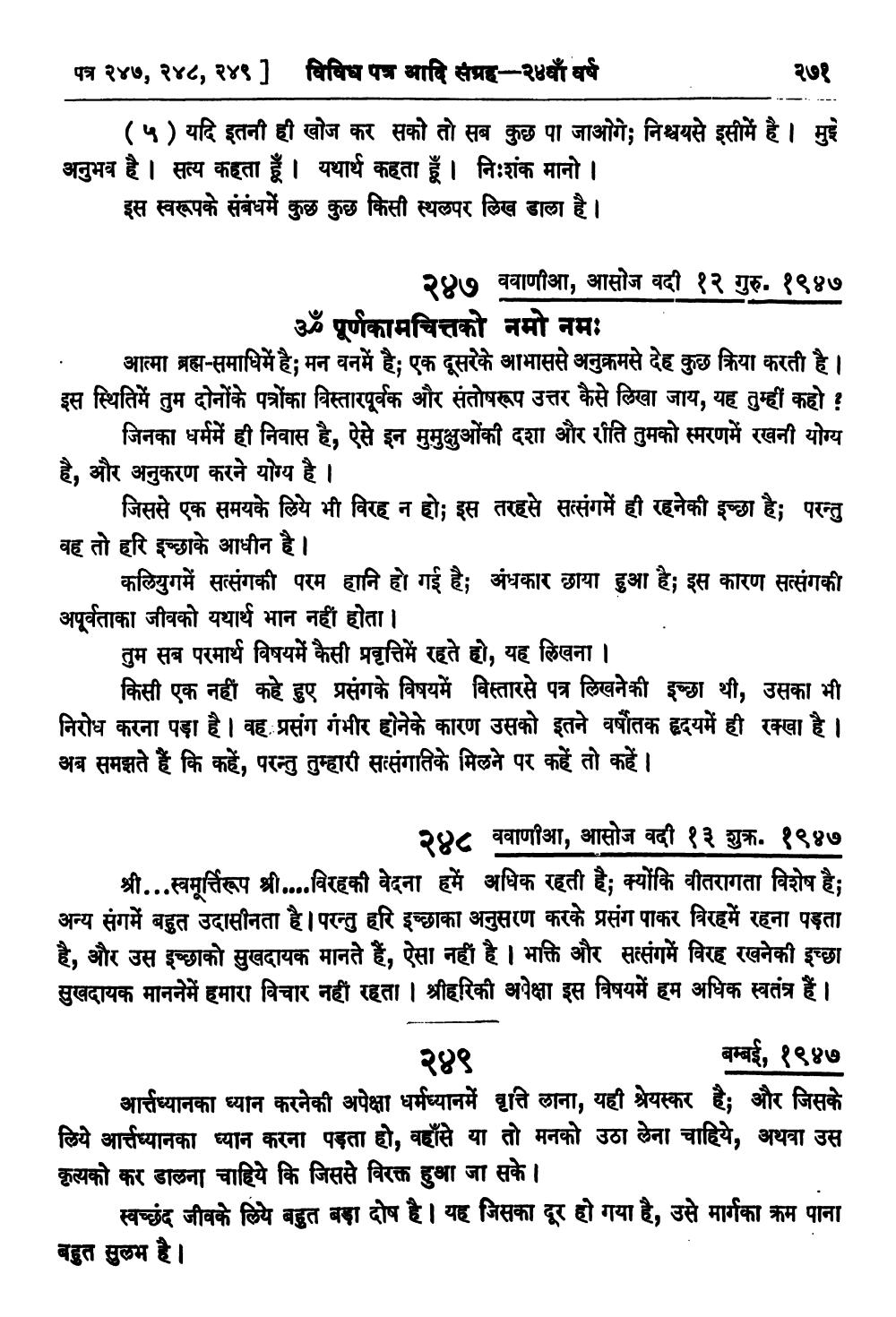________________
पत्र २४७, २४८, २४९] विविध पत्र आदि संग्रह-२४वाँ वर्ष
२७१ (५) यदि इतनी ही खोज कर सको तो सब कुछ पा जाओगे; निश्चयसे इसीमें है। मुई अनुभव है। सत्य कहता हूँ। यथार्थ कहता हूँ। निःशंक मानो ।
इस स्वरूपके संबंधमें कुछ कुछ किसी स्थलपर लिख डाला है।
२४७ ववाणीआ, आसोज वदी १२ गुरु. १९४७
ॐ पूर्णकामचित्तको नमो नमः . आत्मा ब्रह्म-समाधिमें है; मन वनमें है; एक दूसरेके आभाससे अनुक्रमसे देह कुछ क्रिया करती है। इस स्थितिमें तुम दोनोंके पत्रोंका विस्तारपूर्वक और संतोषरूप उत्तर कैसे लिखा जाय, यह तुम्हीं कहो ?
जिनका धर्ममें ही निवास है, ऐसे इन मुमुक्षुओंकी दशा और रीति तुमको स्मरणमें रखनी योग्य है, और अनुकरण करने योग्य है ।
जिससे एक समयके लिये भी विरह न हो; इस तरहसे सत्संगमें ही रहनेकी इच्छा है; परन्तु वह तो हरि इच्छाके आधीन है।
कलियुगमें सत्संगकी परम हानि हो गई है; अंधकार छाया हुआ है। इस कारण सत्संगकी अपूर्वताका जीवको यथार्थ भान नहीं होता।
तुम सब परमार्थ विषयमें कैसी प्रवृत्तिमें रहते हो, यह लिखना ।
किसी एक नहीं कहे हुए प्रसंगके विषयमें विस्तारसे पत्र लिखनेकी इच्छा थी, उसका भी निरोध करना पड़ा है। वह प्रसंग गंभीर होनेके कारण उसको इतने वर्षोंतक हृदयमें ही रक्खा है। अब समझते हैं कि कहें, परन्तु तुम्हारी सत्संगतिके मिलने पर कहें तो कहें।
२४८ ववाणीआ, आसोज वदी १३ शुक्र. १९४७ श्री...स्वमूर्तिरूप श्री....विरहकी वेदना हमें अधिक रहती है; क्योंकि वीतरागता विशेष है; अन्य संगमें बहुत उदासीनता है। परन्तु हरि इच्छाका अनुसरण करके प्रसंग पाकर विरहमें रहना पड़ता है, और उस इच्छाको सुखदायक मानते हैं, ऐसा नहीं है । भक्ति और सत्संगमें विरह रखनेकी इच्छा सुखदायक माननेमें हमारा विचार नहीं रहता । श्रीहरिकी अपेक्षा इस विषयमें हम अधिक स्वतंत्र हैं।
२४९
___ बम्बई, १९४७ आर्तध्यानका ध्यान करनेकी अपेक्षा धर्मध्यानमें वृत्ति लाना, यही श्रेयस्कर है; और जिसके लिये आर्तध्यानका ध्यान करना पड़ता हो, वहाँसे या तो मनको उठा लेना चाहिये, अथवा उस कृत्यको कर डालना चाहिये कि जिससे विरक्त हुआ जा सके।
स्वच्छंद जीवके लिये बहुत बड़ा दोष है। यह जिसका दूर हो गया है, उसे मार्गका क्रम पाना बहुत सुलभ है।