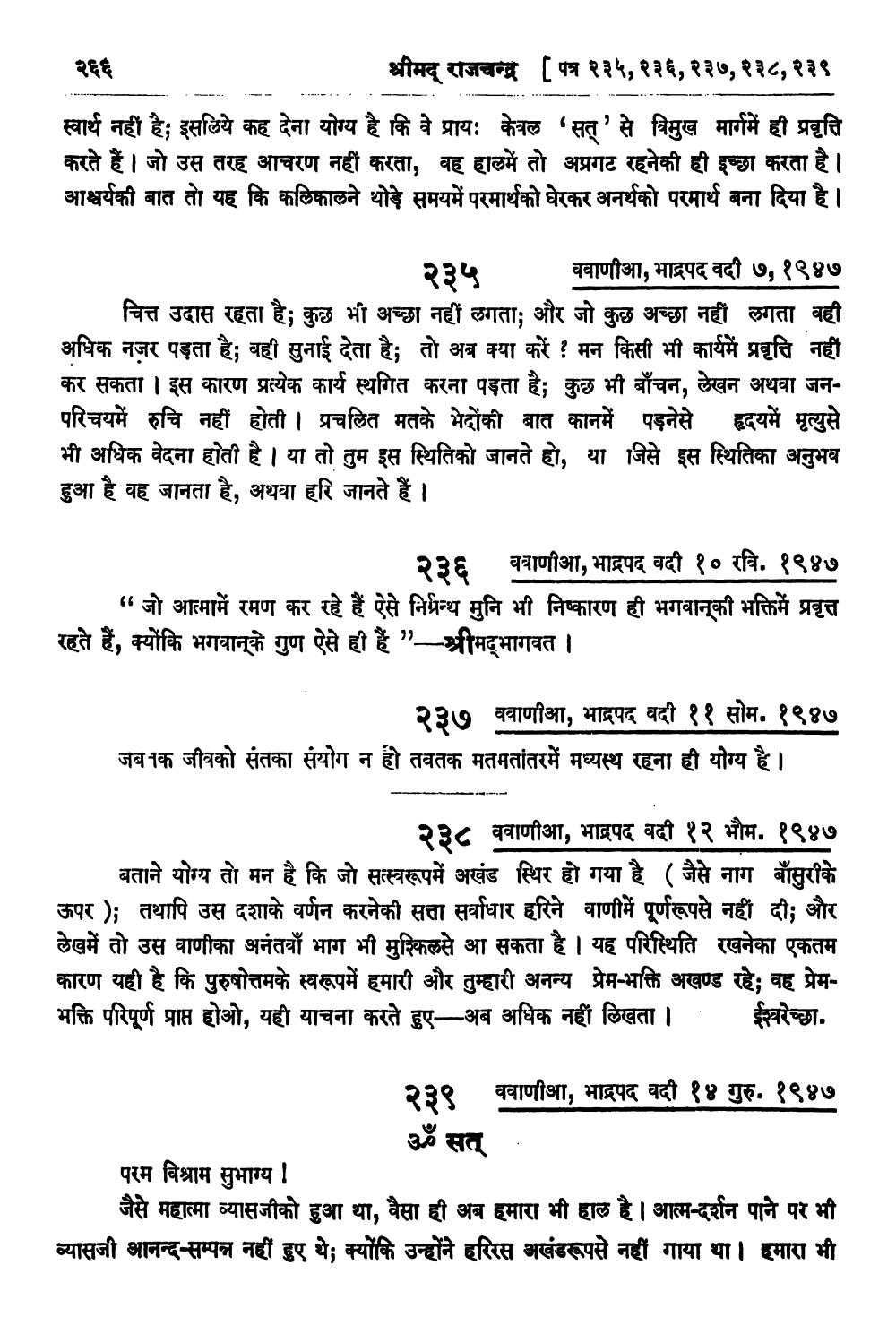________________
२६६
श्रीमद् राजचन्द्र [ पत्र २३५, २३६, २३७, २३८, २३९
स्वार्थ नहीं है; इसलिये कह देना योग्य है कि वे प्रायः केवल ' सत्' से त्रिमुख मार्ग में ही प्रवृत्ति करते हैं । जो उस तरह आचरण नहीं करता, वह हालमें तो अप्रगट रहनेकी ही इच्छा करता है । आश्चर्य की बात तो यह कि कलिकालने थोड़े समयमें परमार्थको घेरकर अनर्थको परमार्थ बना दिया है ।
२३५
ववाणी, भाद्रपद वदी ७, १९४७ चित्त उदास रहता है; कुछ भी अच्छा नहीं लगता; और जो कुछ अच्छा नहीं लगता वही अधिक नज़र पड़ता है; वही सुनाई देता है; तो अब क्या करें ? मन किसी भी कार्य में प्रवृत्ति नहीं कर सकता । इस कारण प्रत्येक कार्य स्थगित करना पड़ता है; कुछ भी बाँचन, लेखन अथवा जनपरिचयमें रुचि नहीं होती । प्रचलित मतके भेदोंकी बात कानमें पड़नेसे हृदयमें मृत्युसे भी अधिक वेदना होती है । या तो तुम इस स्थितिको जानते हो, या जिसे इस स्थितिका अनुभव हुआ है वह जानता है, अथवा हरि जानते हैं ।
२३६
वत्राणी, भाद्रपद वदी १० रवि. १९४७ " जो आत्मामें रमण कर रहे हैं ऐसे निर्ग्रन्थ मुनि भी निष्कारण ही भगवान्की भक्तिमें प्रवृत्त रहते हैं, क्योंकि भगवान्के गुण ऐसे ही हैं " - श्रीमद्भागवत ।
२३७ ववाणी, भाद्रपद वदी ११ सोम. १९४७ जब तक जीवको संतका संयोग न हो तबतक मतमतांतर में मध्यस्थ रहना ही योग्य है ।
२३८ ववाणी, भाद्रपद वदी १२ भौम. १९४७ बताने योग्य तो मन है कि जो सत्स्वरूपमें अखंड स्थिर हो गया है ( जैसे नाग बाँसुरीके ऊपर ); तथापि उस दशाके वर्णन करनेकी सत्ता सर्वाधार हरिने वाणीमें पूर्णरूपसे नहीं दी ; और लेखमें तो उस वाणीका अनंतवाँ भाग भी मुश्किलसे आ सकता है । यह परिस्थिति रखनेका एकतम कारण यही है कि पुरुषोत्तमके स्वरूपमें हमारी और तुम्हारी अनन्य प्रेम-भक्ति अखण्ड रहे; वह प्रेमभक्ति परिपूर्ण प्राप्त होओ, यही याचना करते हुए- -अब अधिक नहीं लिखता । ईश्वरेच्छा.
---
ववाणीआ, भाद्रपद वदी १४ गुरु. १९४७
२३९ ॐ सत्
परम विश्राम सुभाग्य !
जैसे महात्मा व्यासजीको हुआ था, वैसा ही अब हमारा भी हाल है। आत्म-दर्शन पाने पर भी व्यासजी आनन्द - सम्पन्न नहीं हुए थे; क्योंकि उन्होंने हरिरस अखंडरूपसे नहीं गाया था । हमारा भी