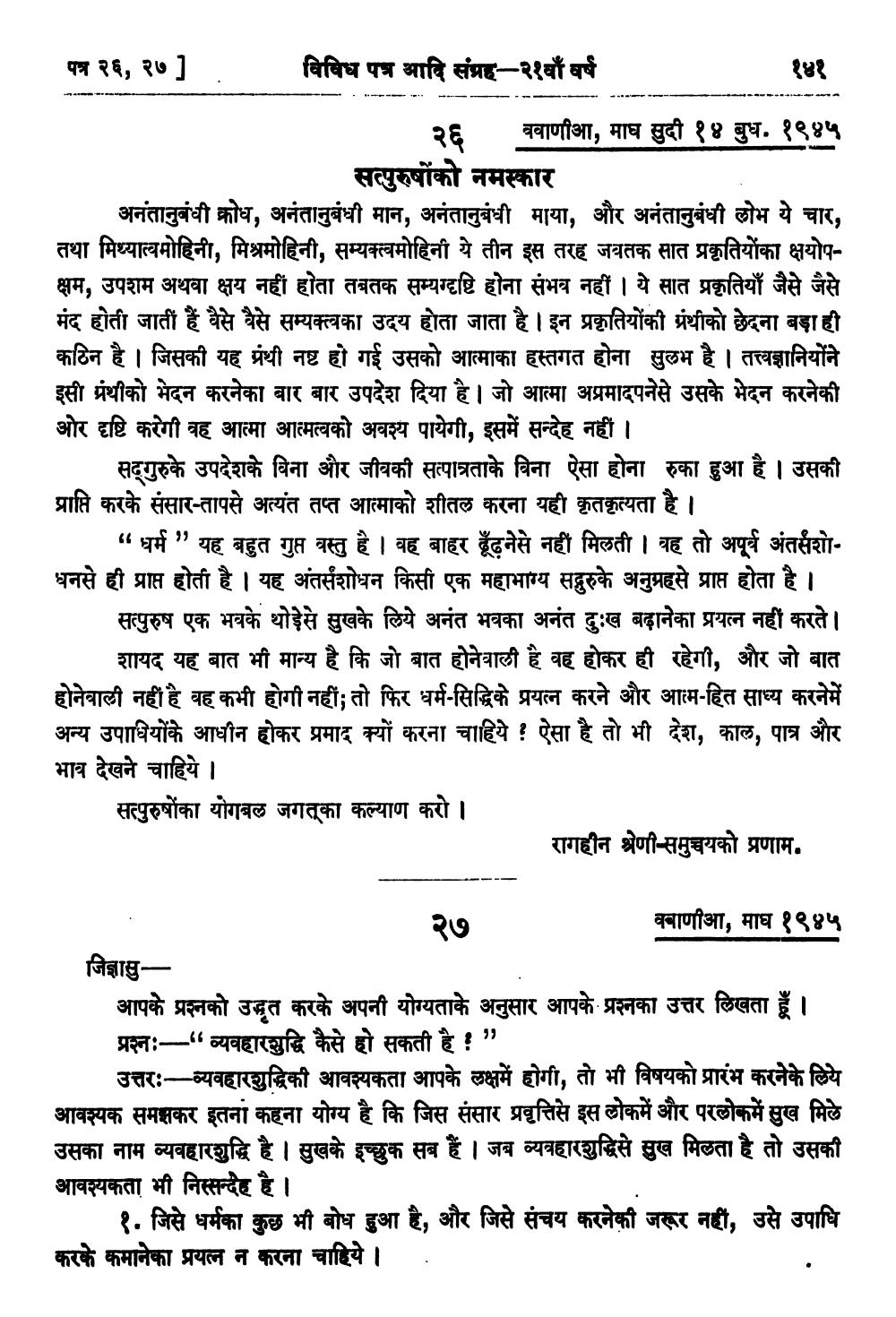________________
पत्र २६, २७]
विविध पत्र आदि संग्रह-२१वाँ वर्ष
२६ ववाणीआ, माघ सुदी १४ बुध. १९४५
सत्पुरुषोंको नमस्कार अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, और अनंतानुबंधी लोभ ये चार, तथा मिथ्यात्वमोहिनी, मिश्रमोहिनी, सम्यक्त्वमोहिनी ये तीन इस तरह जबतक सात प्रकृतियोंका क्षयोपक्षम, उपशम अथवा क्षय नहीं होता तबतक सम्यग्दृष्टि होना संभव नहीं । ये सात प्रकृतियाँ जैसे जैसे मंद होती जाती हैं वैसे वैसे सम्यक्त्वका उदय होता जाता है । इन प्रकृतियोंकी ग्रंथीको छेदना बड़ा ही कठिन है । जिसकी यह ग्रंथी नष्ट हो गई उसको आत्माका हस्तगत होना सुलभ है । तत्त्वज्ञानियोंने इसी ग्रंथीको भेदन करनेका बार बार उपदेश दिया है। जो आत्मा अप्रमादपनेसे उसके भेदन करनेकी ओर दृष्टि करेगी वह आत्मा आत्मत्वको अवश्य पायेगी, इसमें सन्देह नहीं ।
सद्गुरुके उपदेशके विना और जीवकी सत्पात्रताके विना ऐसा होना रुका हुआ है । उसकी प्राप्ति करके संसार-तापसे अत्यंत तप्त आत्माको शीतल करना यही कृतकृत्यता है।
"धर्म" यह बहुत गुप्त वस्तु है । वह बाहर ढूँढनेसे नहीं मिलती । वह तो अपूर्व अंतसंशोधनसे ही प्राप्त होती है । यह अंतर्संशोधन किसी एक महाभाग्य सद्गुरुके अनुग्रहसे प्राप्त होता है।
सत्पुरुष एक भवके थोड़ेसे सुखके लिये अनंत भवका अनंत दुःख बढ़ानेका प्रयत्न नहीं करते।
शायद यह बात भी मान्य है कि जो बात होनेवाली है वह होकर ही रहेगी, और जो बात होनेवाली नहीं है वह कभी होगी नहीं; तो फिर धर्म-सिद्धिके प्रयत्न करने और आत्म-हित साध्य करने में अन्य उपाधियोंके आधीन होकर प्रमाद क्यों करना चाहिये ! ऐसा है तो भी देश, काल, पात्र और भाव देखने चाहिये। सत्पुरुषोंका योगबल जगत्का कल्याण करो ।
रागहीन श्रेणी-समुच्चयको प्रणाम.
ववाणीआ, माघ १९४५ जिज्ञासु
आपके प्रश्नको उद्धृत करके अपनी योग्यताके अनुसार आपके प्रश्नका उत्तर लिखता हूँ। प्रश्न:-" व्यवहारशुद्धि कैसे हो सकती है !"
उत्तरः-व्यवहारशुद्धिकी आवश्यकता आपके लक्षमें होगी, तो भी विषयको प्रारंभ करनेके लिये आवश्यक समझकर इतना कहना योग्य है कि जिस संसार प्रवृत्तिसे इस लोकमें और परलोकमें सुख मिले उसका नाम व्यवहारशुद्धि है । सुखके इच्छुक सब हैं । जब व्यवहारशुद्धिसे सुख मिलता है तो उसकी आवश्यकता भी निस्सन्देह है।
१. जिसे धर्मका कुछ भी बोध हुआ है, और जिसे संचय करनेकी जरूर नहीं, उसे उपाधि करके कमानेका प्रयत्न न करना चाहिये। .