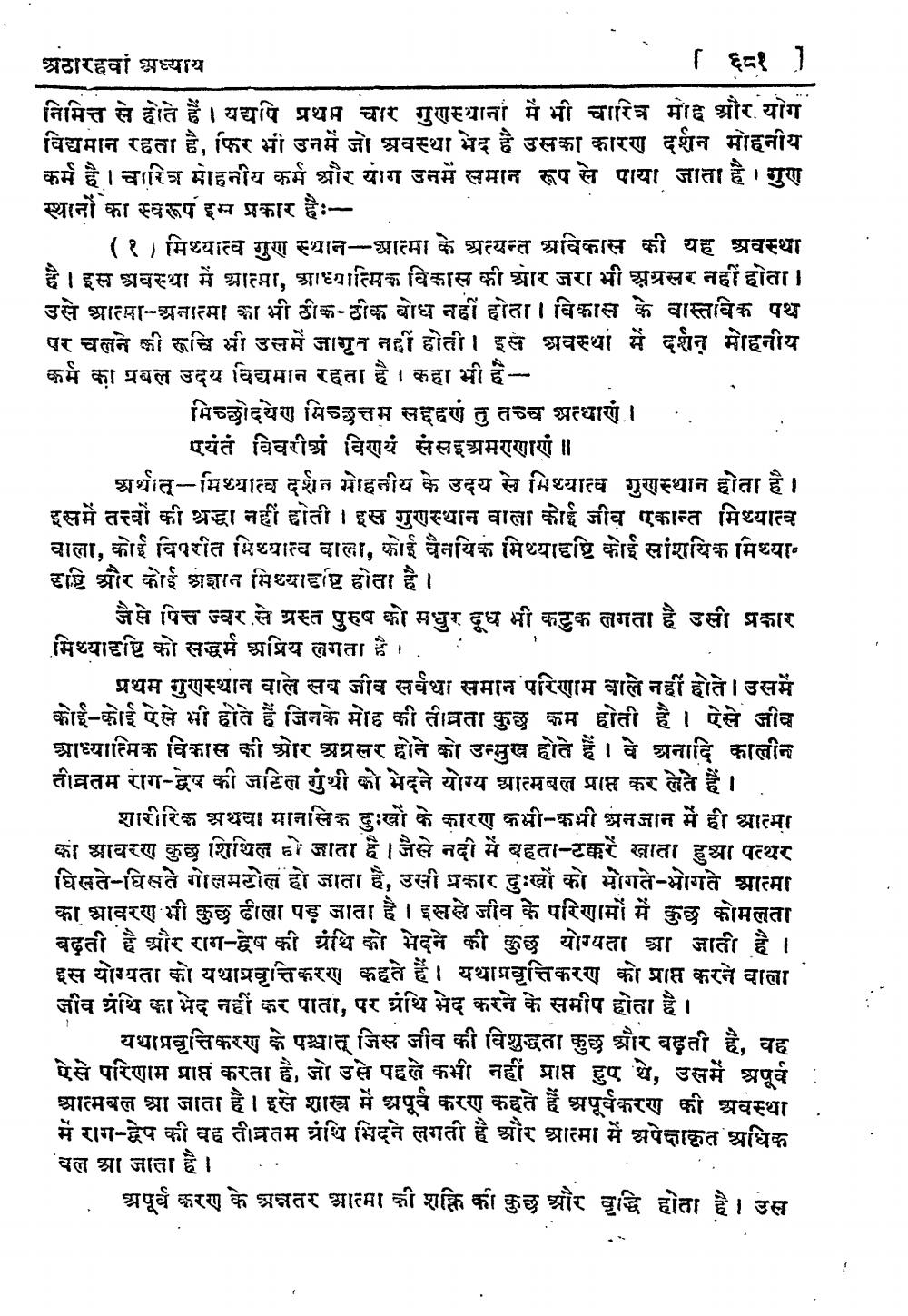________________
-
अठारहवां अध्याय
। ६८१ ] निमित्त से होते हैं। यद्यपि प्रथम चार गुणस्थानों में भी चारित्र मोह और योग विद्यमान रहता है, फिर भी उनमें जो अवस्था भेद है उसका कारण दर्शन मोहनीय कर्म है । चारित्र मोहनीय कर्म और योग उनमें समान रूप से पाया जाता है । गुण स्थानों का स्वरूप इस प्रकार है:
(१) मिथ्यात्व गुण स्थान-श्रात्मा के अत्यन्त अविकास की यह अवस्था है। इस अवस्था में श्रात्मा, आध्यात्मिक विकास की और जरा भी अग्रसर नहीं होता। उसे श्रात्मा-अनात्मा का भी ठीक-ठीक बोध नहीं होता। विकास के वास्तविक पथ पर चलने की रूचि भी उसमें जागृत नहीं होती। इसे अवस्था में दर्शन मोहनीय कर्म का प्रबल उदय विद्यमान रहता है। कहा भी है
मिच्छोदयेण मिच्छत्तम सद्दहणं तु तच्च अत्थाणं । ..
एयंतं विवरीअं विणयं संसइअमराणाणं ॥ अर्थात्-मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय के उदय से मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। इलमें तत्त्वों की श्रद्धा नहीं होती । इस गुणस्थान वाला कोई जीव एकान्त मिथ्यात्व वाला, कोई विपरीत मिथ्यात्व वाला, कोई वैनयिक मिथ्यादृष्टि कोई सांशयिक मिथ्या० दृष्टि और कोई अज्ञान मिथ्याष्टि होता है।
जैले पित्त ज्वर ले ग्रस्त पुरुष को मधुर दूध भी कटुक लगता है उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि को सद्धर्म अप्रिय लगता है। .
प्रथम गुणस्थान वाले लब जीव सर्वथा समान परिणाम वाले नहीं होते। उसमें कोई-कोई ऐसे भी होते हैं जिनके मोह की तीव्रता कुछ कम होती है। ऐसे जीव श्राध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर होने को उन्मुख होते हैं । वे अनादि कालीन तीव्रतम राग-द्वेष की जटिल गुंथी को भेदने योग्य प्रात्मबल प्राप्त कर लेते हैं। .
__शारीरिक अथवा मानसिक दुःखों के कारण कभी-कभी अनजान में ही श्रात्मा का आवरण कुछ शिथिल हो जाता है। जैसे नदी में बहता-टक्करें खाता हुश्रा पत्थर घिसते-घिसते गोलमटोल हो जाता है, उसी प्रकार दुःखों को भोगते-भोगते श्रात्मा का श्रावरण भी कुछ ढीला पड़ जाता है । इलले जीव के परिणामों में कुछ कोमलता बढ़ती है और राग-द्वेष की ग्रंथि को भेदने की कुछ योग्यता आ जाती है। इस योग्यता को यथाप्रवृत्तिकरण कहते हैं। यथाप्रवृत्तिकरण को प्राप्त करने वाला जीव ग्रंथि का भेद नहीं कर पाता, पर ग्रंथि भेद करने के समीप होता है। - यथाप्रवृत्तिकरण के पश्चात् जिस जीव की विशुद्धता कुछ और बढ़ती है, वह ऐसे परिणाम प्राप्त करता है, जो उसे पहले कभी नहीं प्राप्त हुए थे, उसमें अपूर्व : आत्मबल श्रा जाता है। इसे शास्त्र में अपूर्व करण कहते हैं अपूर्वकरण की अवस्था . में राग-द्वेप की वह तीव्रतम ग्रंथि भिदने लगती है और श्रात्मा में अपेक्षाकृत अधिक वल आ जाता है।
अपूर्व करण के अन्नतर भात्मा की शक्ति की कुछ और वृद्धि होता है। उस