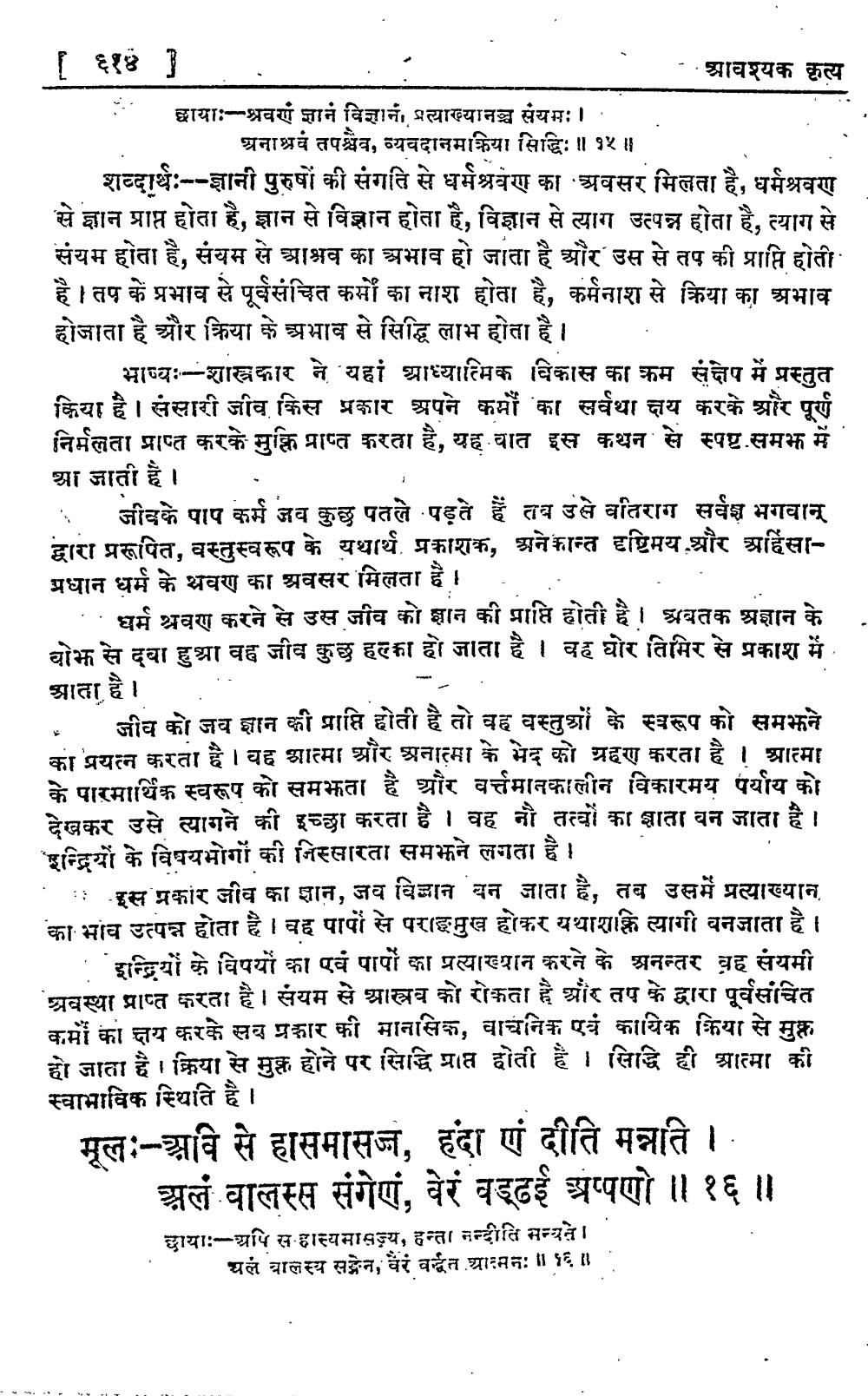________________
[ ६१४ ]
छाया:-- श्रवणं ज्ञानं विज्ञानं प्रत्याख्यानञ्च संयमः । श्रनाश्रवं तपश्चैव, व्यवदानमक्रिया सिद्धिः ॥ १५ ॥
श्रावश्यक कृत्य
शब्दार्थः-- ज्ञानी पुरुषों की संगति से धर्मश्रवण का अवसर मिलता है, धर्मश्रवण से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से विज्ञान होता है, विज्ञान से त्याग उत्पन्न होता है, त्याग से संयम होता है, संयम से आश्रव का अभाव हो जाता है और उस से तप की प्राप्ति होती है । तप के प्रभाव से पूर्वसंचित कर्मों का नाश होता है, कर्मनाश से क्रिया का अभाव होजाता है और क्रिया के अभाव से सिद्धि लाभ होता है ।
भाग्यः- शास्त्रकार ने यहां श्राध्यात्मिक विकास का क्रम संक्षेप में प्रस्तुत किया है । संसारी जीव किस प्रकार अपने कर्मों का सर्वथा क्षय करके और पूर्ण निर्मलता प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त करता है, यह बात इस कथन से स्पष्ट समझ में आ जाती है ।
जीवके पाप कर्म जब कुछ पतले पढ़ते हैं तब उसे वतिराग सर्वज्ञ भगवान् द्वारा प्ररूपित, वस्तुस्वरूप के यथार्थ प्रकाशक, अनेकान्त दृष्टिमय और अहिंसाप्रधान धर्म के श्रवण का अवसर मिलता है ।
धर्म श्रवण करने से उस जीव को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अबतक अज्ञान के बोझ से दबा हुआ वह जीव कुछ हल्का हो जाता है । वह घोर तिमिर से प्रकाश में आता है ।
जीव को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह वस्तुओं के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करता है | वह श्रात्मा और अनात्मा के भेद को ग्रहण करता है । श्रात्मा के पारमार्थिक स्वरूप को समझता है और वर्त्तमानकालीन विकारमय पर्याय को देखकर उसे त्यागने की इच्छा करता है । वह नौ तत्वों का ज्ञाता बन जाता है । इन्द्रियों के विषयभोगों की जिस्सारता समझने लगता है ।
::
- इस प्रकार जीव का ज्ञान, जय विज्ञान बन जाता है, तब उसमें प्रत्याख्यान का भाव उत्पन्न होता है । वह पापों से परराङ्मुख होकर यथाशक्ति त्यागी बनजाता है ।
1
इन्द्रियों के विषयों का एवं पापों का प्रत्याख्यान करने के अनन्तर वह संयमी अवस्था प्राप्त करता है । संयम से श्रास्त्रव को रोकता है और तप के द्वारा पूर्वसंचित कर्मों का क्षय करके सब प्रकार की मानसिक, वाचनिक एवं कायिक क्रिया से मुक्त हो जाता है । क्रिया से मुक्त होने पर सिद्धि प्राप्त होती हैं । सिद्धि ही श्रात्मा की स्वाभाविक स्थिति है ।
I
मूलः - अवि से हासमासज्ज, हंदा णं दीति मन्नति ।
अलं वालस्स संगेणं, वेरं वड्ढई अप्पणो ॥ १६ ॥
छाया:-अपि स हास्यमासज्य, हन्ता नन्दीति मन्यते । चल बालस्य सङ्गेन वैरं वर्द्धत यामनः ॥ १६ ॥