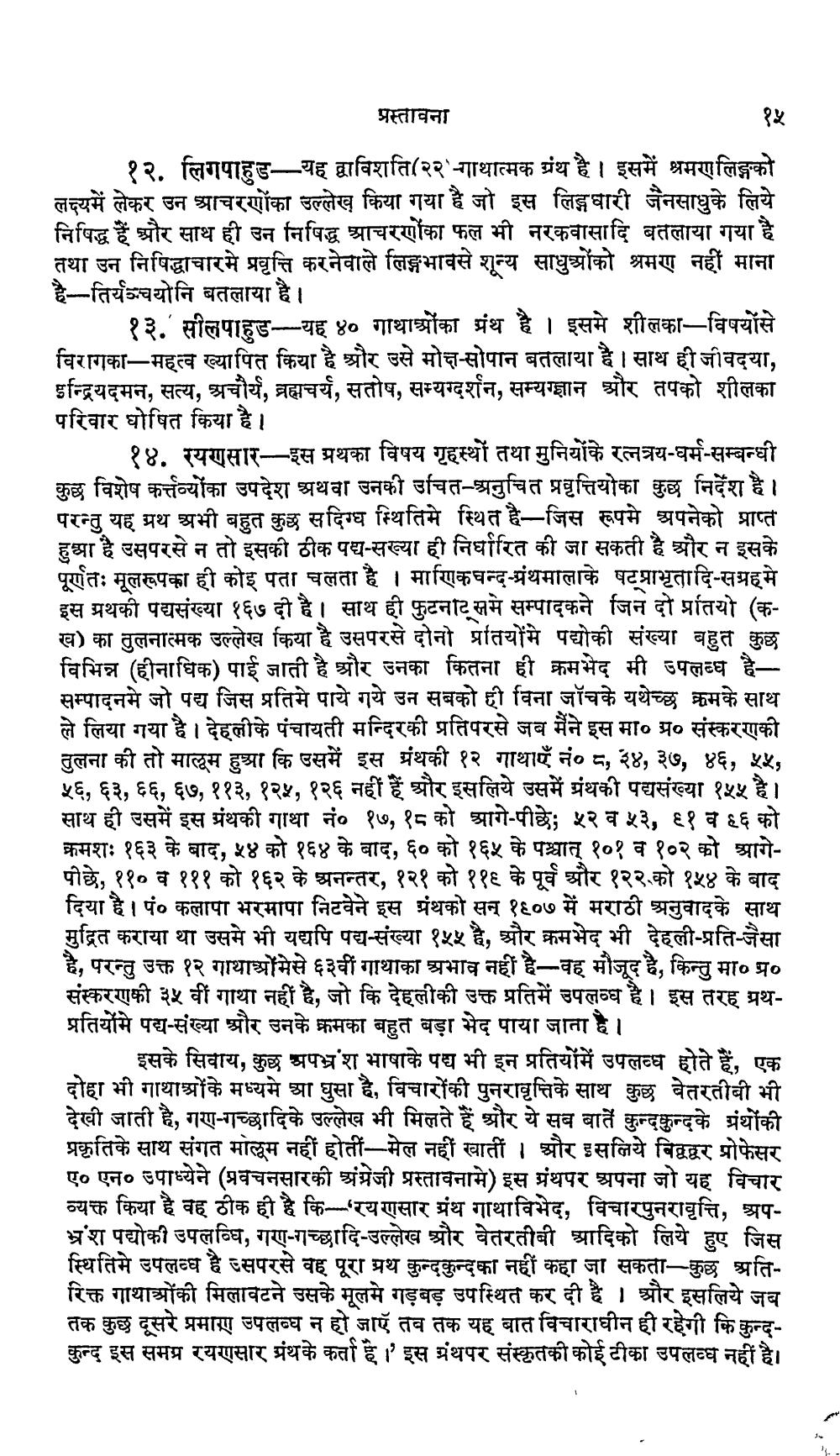________________
प्रस्तावना
१५
१२. लिगपाहुड—यह वाविशति(२२'-गाथात्मक ग्रंथ है। इसमें श्रमणलिङ्गको लक्ष्यमें लेकर उन आचरणोंका उल्लेख किया गया है जो इस लिङ्गधारी जैनसाधुके लिये निषिद्ध हैं और साथ ही उन निषिद्ध आचरणोंका फल भी नरकवासादि बतलाया गया है तथा उन निषिद्धाचारमे प्रवृत्ति करनेवाले लिङ्गभावसे शून्य साधुओंको श्रमण नहीं माना है-तिर्यञ्चयोनि बतलाया है।
१३. सीलपाहुड-यह ४० गाथाओंका ग्रंथ है । इसमे शीलका-विषयोंसे विरागका महत्व ख्यापित किया है और उसे मोक्ष-सोपान बतलाया है। साथ ही जीवदया, इन्द्रियदमन, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, सतोष, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और तपको शीलका परिवार घोषित किया है।
१४. रयणसार-इस प्रथका विषय गृहस्थों तथा मुनियोंके रत्नत्रय-धर्म-सम्बन्धी कुछ विशेष कर्तव्योंका उपदेश अथवा उनकी उचित-अनुचित प्रवृत्तियोका कुछ निर्देश है। परन्तु यह प्रथ अभी बहुत कुछ सदिग्ध स्थितिमे स्थित है-जिस रूपमे अपनेको प्राप्त हुआ है उसपरसे न तो इसकी ठीक पद्य-सख्या ही निर्धारित की जा सकती है और न इसके पूर्णतः मूलरूपका ही कोइ पता चलता है । माणिकचन्द-ग्रंथमालाके षटप्राभृतादि-सग्रहमे इस प्रथकी पद्यसंख्या १६७ दी है। साथ ही फुटनाटसमे सम्पादकने जिन दो प्रतियो (कख) का तुलनात्मक उल्लेख किया है उसपरसे दोनो प्रतियोंमे पद्योकी संख्या बहुत कुछ विभिन्न (हीनाधिक) पाई जाती है और उनका कितना ही क्रमभेद मी उपलब्ध हैसम्पादनमे जो पद्य जिस प्रतिमे पाये गये उन सबको ही विना जॉचके यथेच्छ क्रमके साथ ले लिया गया है। देहलीके पंचायती मन्दिरकी प्रतिपरसे जब मैंने इस मा० प्र० संस्करणकी तुलना की तो मालूम हुआ कि उसमें इस ग्रंथकी १२ गाथाएँ नं०८, ३४, ३७, ४६, ५५, ५६, ६३, ६६, ६७, ११३, १२५, १२६ नहीं हैं और इसलिये उसमें ग्रंथकी पद्यसंख्या १५५ है। साथ ही उसमें इस ग्रंथकी गाथा नं० १७, १८ को आगे-पीछे; ५२ व ५३, ६१ व ६६ को क्रमशः १६३ के बाद, ५४ को १६४ के बाद, ६० को १६५ के पश्चात् १०१ व १०२ को आगेपोछे, ११० व १११ को १६२ के अनन्तर, १२१ को ११६ के पूर्व और १२२.को १५४ के बाद दिया है। पं० कलापा भरमापा निटवेने इस ग्रंथको सन् १६०७ में मराठी अनुवादके साथ मुद्रित कराया था उसमे भी यद्यपि पद्य-संख्या १५५ है, और क्रमभेद भी देहली-प्रति-जैसा है, परन्तु उक्त १२ गाथाओंमेसे ६३वीं गाथाका अभाव नहीं है-वह मौजूद है, किन्तु मा० प्र० संस्करणकी ३५ वीं गाथा नहीं है, जो कि देहलीकी उक्त प्रतिमें उपलब्ध है। इस तरह प्रथप्रतियोंमे पद्य-संख्या और उनके क्रमका बहुत बड़ा भेद पाया जाता है।
इसके सिवाय, कुछ अपभ्रंश भाषाके पद्य भी इन प्रतियोंमें उपलब्ध होते हैं, एक दोहा भी गाथाओं के मध्यमे आ घुसा है, विचारोंकी पुनरावृत्तिके साथ कुछ बेतरतीबी भी देखी जाती है, गण-गच्छादिके उल्लेख भी मिलते हैं और ये सब बातें कुन्दकुन्दके ग्रंथोंकी प्रकृतिके साथ संगत मालूम नहीं होतीं-मेल नहीं खातीं । और इसलिये विवर प्रोफेसर ए० एन० उपाध्येने (प्रवचनसारकी अंग्रेजी प्रस्तावनामे) इस ग्रंथपर अपना जो यह विचार व्यक्त किया है वह ठीक ही है कि-'रयणसार ग्रंथ गाथाविभेद, विचारपुनरावृत्ति, अपभ्रंश पद्योकी उपलब्धि, गण-गच्छादि-उल्लेख और बेतरतीबी आदिको लिये हुए जिस स्थितिमे उपलब्ध है उसपरसे वह पूरा प्रथ कुन्दकुन्दका नहीं कहा जा सकता-कुछ अतिरिक्त गाथाओंकी मिलावटने उसके मूलमे गड़बड़ उपस्थित कर दी है । और इसलिये जब तक कुछ दूसरे प्रमाण उपलब्ध न हो जाएँ तब तक यह बात विचाराधीन ही रहेगी कि कुन्दकुन्द इस समग्र रयणसार ग्रंथके कर्ता है। इस ग्रंथपर संस्कृतकी कोई टीका उपलब्ध नहीं है।