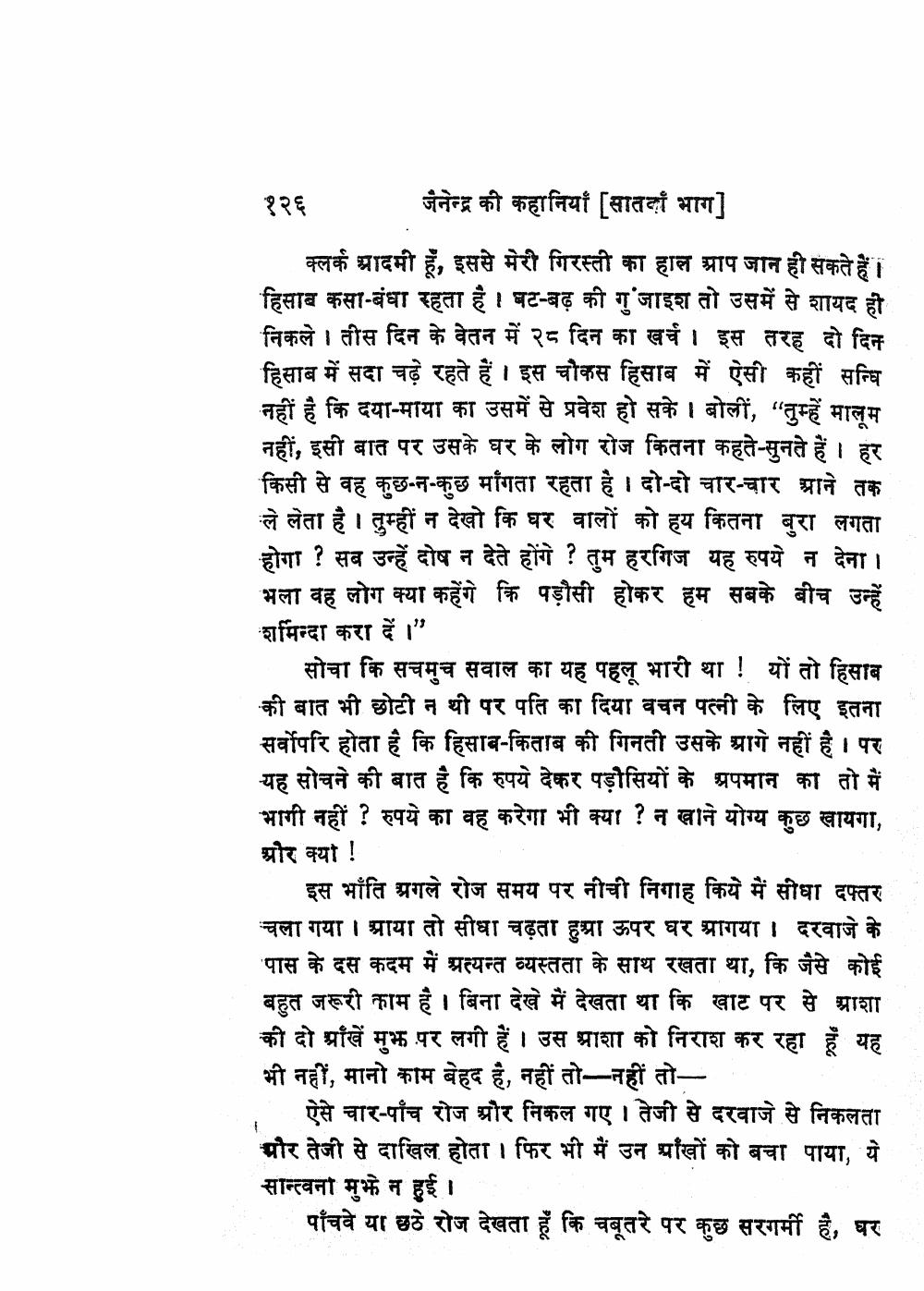________________
१२६ जनेन्द्र की कहानियाँ [सातदाँ भाग]
क्लर्क आदमी हूँ, इससे मेरी गिरस्ती का हाल आप जान ही सकते हैं। हिसाब कसा-बंधा रहता है । घट-बढ़ की गुजाइश तो उसमें से शायद ही निकले । तीस दिन के वेतन में २८ दिन का खर्च । इस तरह दो दिन हिसाब में सदा चढ़े रहते हैं । इस चौकस हिसाब में ऐसी कहीं सन्धि नहीं है कि दया-माया का उसमें से प्रवेश हो सके । बोली, "तुम्हें मालूम नहीं, इसी बात पर उसके घर के लोग रोज कितना कहते-सुनते हैं। हर किसी से वह कुछ-न-कुछ मांगता रहता है । दो-दो चार-चार आने तक ले लेता है । तुम्हीं न देखो कि घर वालों को हय कितना बुरा लगता होगा ? सब उन्हें दोष न देते होंगे ? तुम हरगिज यह रुपये न देना। भला वह लोग क्या कहेंगे कि पड़ोसी होकर हम सबके बीच उन्हें शर्मिन्दा करा दें।"
सोचा कि सचमुच सवाल का यह पहलू भारी था ! यों तो हिसाब की बात भी छोटी न थी पर पति का दिया वचन पत्नी के लिए इतना सर्वोपरि होता है कि हिसाब-किताब की गिनती उसके आगे नहीं है। पर यह सोचने की बात है कि रुपये देकर पड़ोसियों के अपमान का तो मैं भागी नहीं ? रुपये का वह करेगा भी क्या ? न खाने योग्य कुछ खायगा, और क्यो!
इस भाँति अगले रोज समय पर नीची निगाह किये मैं सीधा दफ्तर चला गया। प्राया तो सीधा चढ़ता हुआ ऊपर घर आगया। दरवाजे के पास के दस कदम में अत्यन्त व्यस्तता के साथ रखता था, कि जैसे कोई बहुत जरूरी काम है। बिना देखे मैं देखता था कि खाट पर से आशा की दो आँखें मुझ पर लगी हैं । उस प्राशा को निराश कर रहा हूँ यह भी नहीं, मानो काम बेहद है, नहीं तो-नहीं तो। ऐसे चार-पाँच रोज और निकल गए। तेजी से दरवाजे से निकलता
और तेजी से दाखिल होता । फिर भी मैं उन आँखों को बचा पाया, ये सान्त्वना मुझे न हुई।
पाँचवे या छठे रोज देखता हूँ कि चबूतरे पर कुछ सरगर्मी है, घर