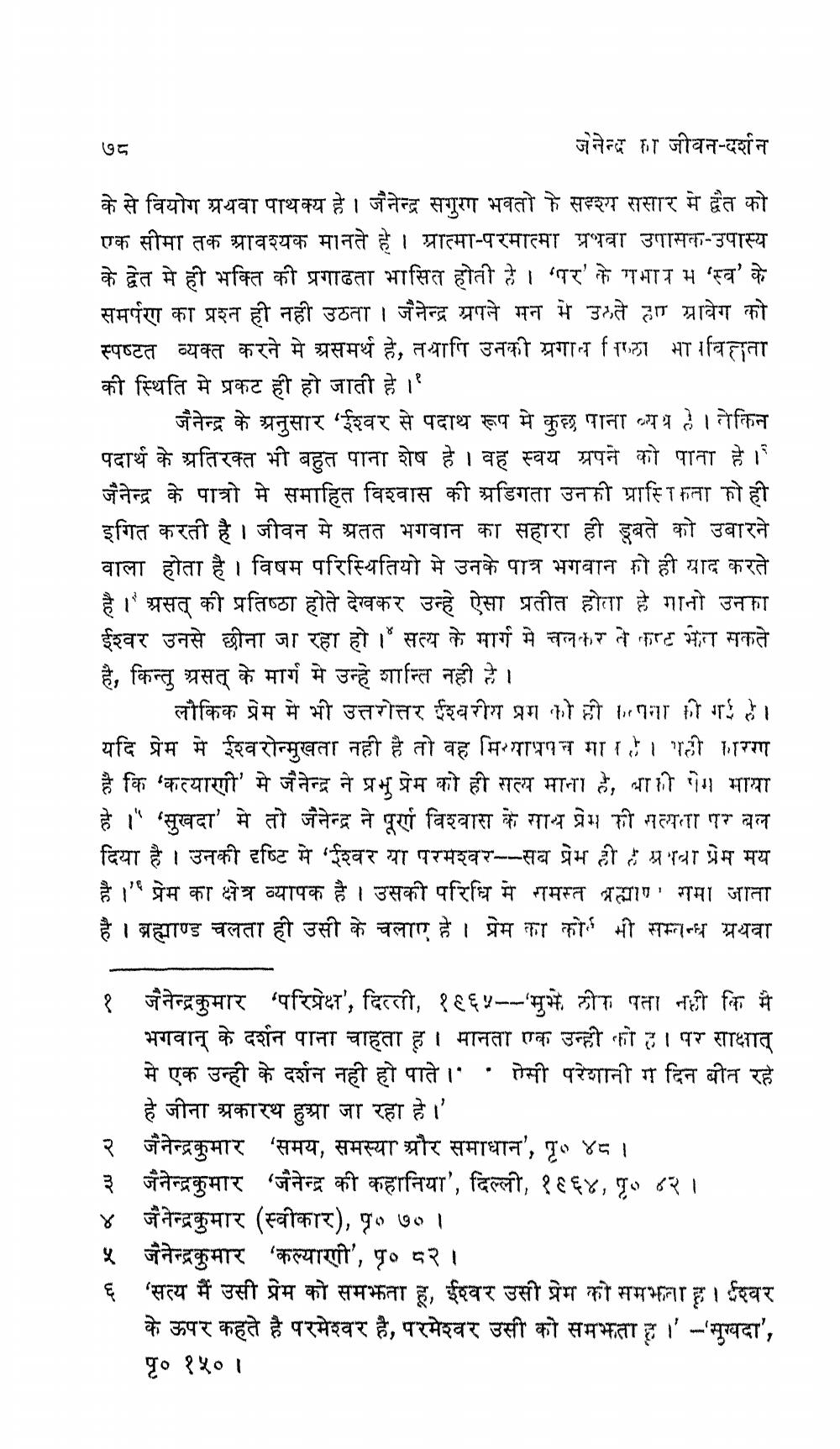________________
जेनेन्द्र का जीवन-दर्शन
के से वियोग अथवा पाथक्य है । जैनेन्द्र सगुराग भवतो के सहश्य ससार मे द्वैत को एक सीमा तक आवश्यक मानते हैं। प्रात्मा-परमात्मा अथवा उपासक-उपास्य के द्वेत मे ही भक्ति की प्रगाढता भासित होती है। पर' के पभान म 'स्व' के समर्पण का प्रश्न ही नही उठता। जैनेन्द्र अपने मन में उठते हा यावेग को स्पष्टत व्यक्त करने में असमर्थ है, तथापि उनकी प्रगान मिठा भा विहता की स्थिति में प्रकट ही हो जाती है।'
जैनेन्द्र के अनुसार 'ईश्वर से पदाथ रूप मे कुछ पाना व्यय है । लेकिन पदार्थ के अतिरक्त भी बहुत पाना शेष है। वह स्वय अपने को पाता है। जैनेन्द्र के पात्रो मे समाहित विश्वास की अडिगता उनकी प्रास्तिकता को ही इगित करती है। जीवन मे अतत भगवान का सहारा ही डूबते को उबारने वाला होता है । विषम परिस्थितियो मे उनके पात्र भगवान को ही याद करते है । असत् की प्रतिष्ठा होते देवकर उन्हे ऐसा प्रतीत होता हे गानो उनका ईश्वर उनसे छीना जा रहा हो। सत्य के मार्ग मे चलकर ने काट भत सकते है, किन्तु असत् के मार्ग मे उन्हे शान्ति नही है।
___ लौकिक प्रेम में भी उत्तरोत्तर ईश्वरीय प्रम को ही ना की गई है। यदि प्रेम में ईश्वरोन्मुखता नही है तो वह मियाप्रपच मा । ती कारण है कि 'कल्याणी' मे जैनेन्द्र ने प्रभु प्रेम को ही सत्य माना है, बाकी गेम माया हे । 'सुखदा' मे तो जैनेन्द्र ने पूर्ण विश्वास के साथ प्रेम की सत्यता पर बल दिया है। उनकी दृष्टि में ईश्वर या परमश्वर--सब प्रेमही अपवा प्रेम मय है। प्रेम का क्षेत्र व्यापक है। उसकी परिधि में समस्त ब्रह्माण। समा जाता है । ब्रह्माण्ड चलता ही उसी के चलाए है। प्रेम का कोई भी सम्बन्ध अथवा
१ जैनेन्द्र कुमार 'परिप्रेक्ष', दित्ती, १९६५---'मुझे ठीक पता नही कि मैं
भगवान् के दर्शन पाना चाहता है। मानता एक उन्ही को हपर साक्षात् मे एक उन्ही के दर्शन नही हो पाते। - ऐसी परेशानी में दिन बीत रहे
हे जीना अकारथ हुआ जा रहा है।' २ जैनेन्द्रकुमार 'समय, समस्या और समाधान', पृ० ४८ । ३ जैनेन्द्रकुमार 'जैनेन्द्र की कहानिया', दिल्ली, १९६४, पृ० ४२ । ४ जैनेन्द्रकुमार (स्वीकार), पृ० ७० । ५ जैनेन्द्रकुमार कल्याणी', पृ० ८२ । ६ 'सत्य मैं उसी प्रेम को समझता ह, ईश्वर उसी प्रेम को समझना ह। ईश्वर
के ऊपर कहते है परमेश्वर है, परमेश्वर उसी को समझता हु ।' - 'मुग्वदा', पृ० १५० ।