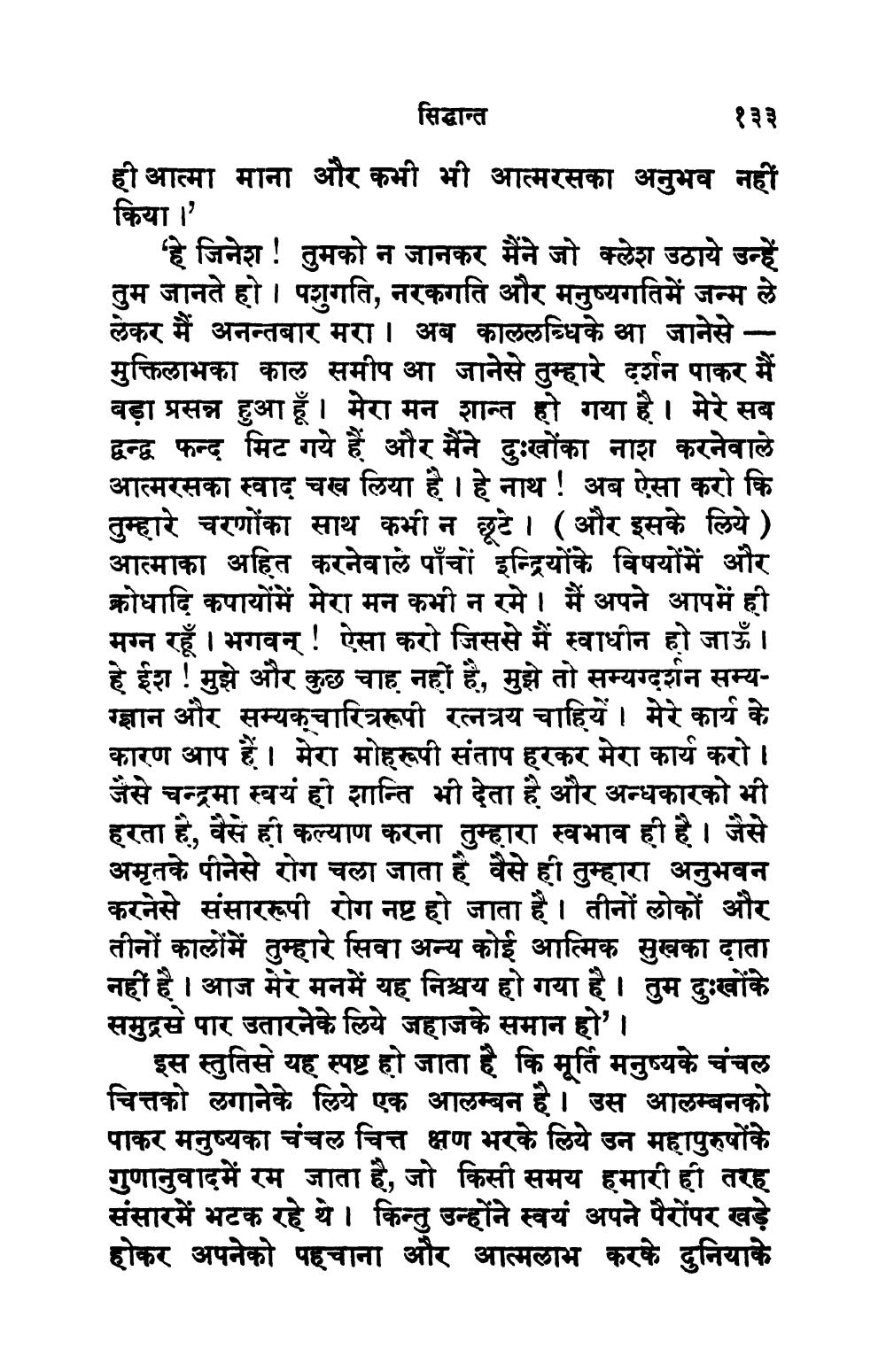________________
सिद्धान्त
१३३ ही आत्मा माना और कभी भी आत्मरसका अनुभव नहीं किया। __ 'हे जिनेश ! तुमको न जानकर मैंने जो क्लेश उठाये उन्हें तुम जानते हो। पशुगति, नरकगति और मनुष्यगतिमें जन्म ले लेकर मैं अनन्तबार मरा। अब काललब्धिके आ जानेसेमुक्तिलाभका काल समीप आ जानेसे तुम्हारे दर्शन पाकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। मेरा मन शान्त हो गया है। मेरे सब द्वन्द्व फन्द मिट गये हैं और मैंने दुःखोंका नाश करनेवाले आत्मरसका स्वाद चख लिया है । हे नाथ ! अब ऐसा करो कि तुम्हारे चरणोंका साथ कभी न छूटे । (और इसके लिये ) आत्माका अहित करनेवाले पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंमें और क्रोधादि कपायोंमें मेरा मन कभी न रमे । मैं अपने आपमें ही मग्न रहूँ । भगवन् ! ऐसा करो जिससे मैं स्वाधीन हो जाऊँ । हे ईश ! मुझे और कुछ चाह नहीं है, मुझे तो सम्यग्दर्शन सम्यरज्ञान और सम्यकचारित्ररूपी रत्नत्रय चाहिये। मेरे कार्य के कारण आप हैं। मेरा मोहरूपी संताप हरकर मेरा कार्य करो। जैसे चन्द्रमा स्वयं हो शान्ति भी देता है और अन्धकारको भी हरता है, वैसे ही कल्याण करना तुम्हारा स्वभाव ही है। जैसे अमृतके पीनेसे रोग चला जाता है वैसे ही तुम्हारा अनुभवन करनेसे संसाररूपी रोग नष्ट हो जाता है। तीनों लोकों और तीनों कालोंमें तुम्हारे सिवा अन्य कोई आत्मिक सुखका दाता नहीं है । आज मेरे मनमें यह निश्चय हो गया है। तुम दुःखोंके समुद्रसे पार उतारनेके लिये जहाजके समान हो। __इस स्तुतिसे यह स्पष्ट हो जाता है कि मूर्ति मनुष्यके चंचल चित्तको लगानेके लिये एक आलम्बन है। उस आलम्बनको पाकर मनुष्यका चंचल चित्त क्षण भरके लिये उन महापुरुषोंके गुणानुवादमें रम जाता है, जो किसी समय हमारी ही तरह संसारमें भटक रहे थे। किन्तु उन्होंने स्वयं अपने पैरोंपर खड़े होकर अपनेको पहचाना और आत्मलाभ करके दुनियाके