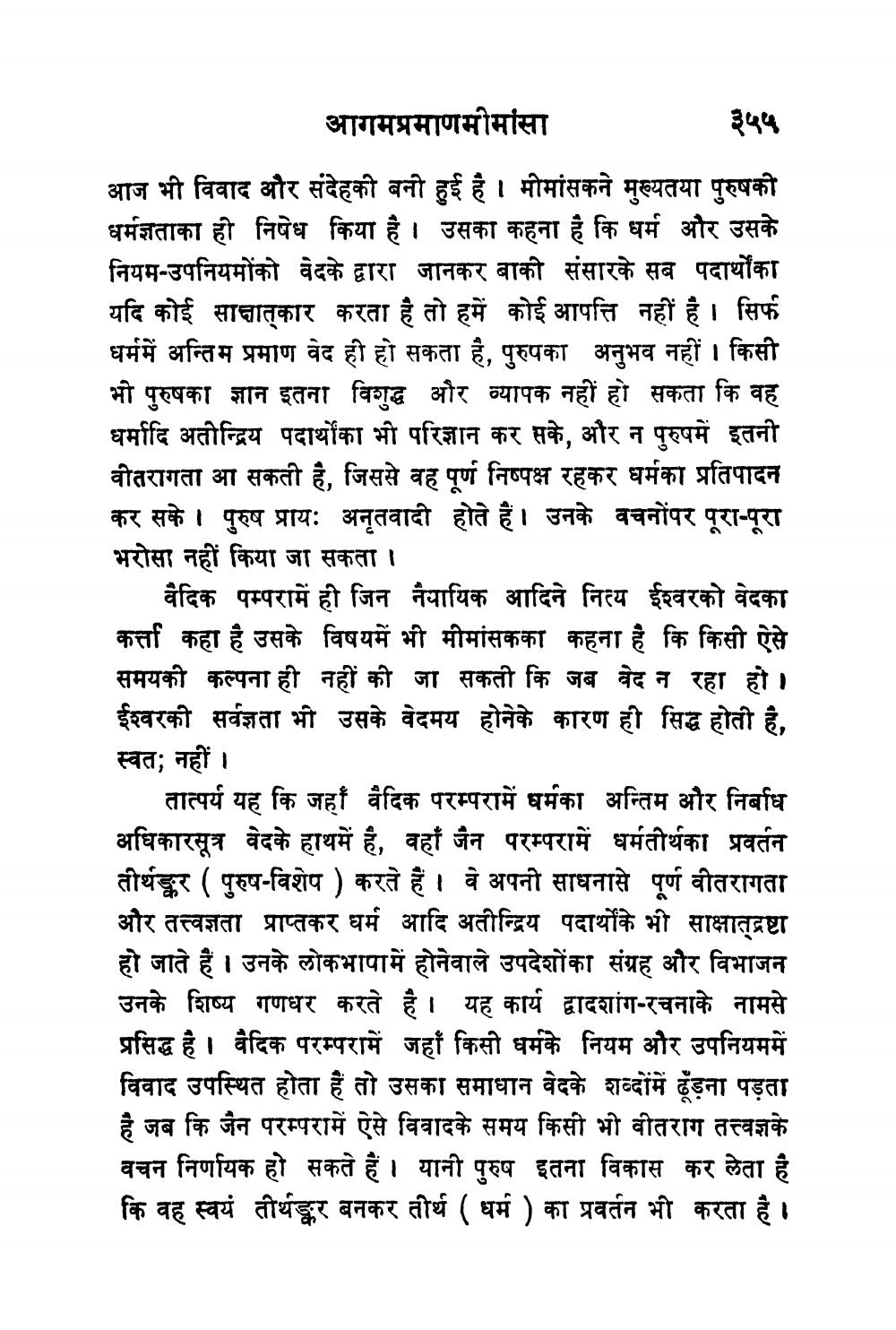________________
आगमप्रमाणमीमांसा
३५५
1
आज भी विवाद और संदेहकी बनी हुई है । मीमांसकने मुख्यतया पुरुषकी धर्मज्ञताका ही निषेध किया है । उसका कहना है कि धर्म और उसके नियम - उपनियमोंको वेदके द्वारा जानकर बाकी संसारके सब पदार्थोंका यदि कोई साक्षात्कार करता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है । सिर्फ धर्म में अन्तिम प्रमाण वेद ही हो सकता है, पुरुपका अनुभव नहीं । किसी भी पुरुषका ज्ञान इतना विशुद्ध और व्यापक नहीं हो सकता कि वह धर्मादि अतीन्द्रिय पदार्थों का भी परिज्ञान कर सके, और न पुरुषमें इतनी वीतरागता आ सकती है, जिससे वह पूर्ण निष्पक्ष रहकर धर्मका प्रतिपादन कर सके । पुरुष प्रायः अनृतवादी होते हैं । उनके वचनोंपर पूरा-पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता ।
वैदिक पम्परामें ही जिन नैयायिक आदिने नित्य ईश्वरको वेदका कर्त्ता कहा है उसके विषयमें भी मीमांसकका कहना है कि किसी ऐसे समयकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि जब वेद न रहा हो । ईश्वरकी सर्वज्ञता भी उसके वेदमय होनेके कारण ही सिद्ध होती है, स्वत; नहीं ।
तात्पर्य यह कि जहाँ वैदिक परम्परामें धर्मका अन्तिम और निर्बाध अधिकारसूत्र वेदके हाथमें है, वहाँ जैन परम्परामें धर्मतीर्थका प्रवर्तन तीर्थङ्कर ( पुरुष - विशेष ) करते हैं । वे अपनी साधनासे पूर्ण वीतरागता और तत्त्वज्ञता प्राप्तकर धर्म आदि अतीन्द्रिय पदार्थोंके भी साक्षाद्रष्टा हो जाते हैं । उनके लोकभाषा में होनेवाले उपदेशों का संग्रह और विभाजन उनके शिष्य गणधर करते है । यह कार्य द्वादशांग - रचनाके नामसे प्रसिद्ध है । वैदिक परम्परामें जहाँ किसी धर्मके नियम और उपनियममें विवाद उपस्थित होता हैं तो उसका समाधान वेदके शब्दोंमें ढूंड़ना पड़ता है जब कि जैन परम्परामें ऐसे विवादके समय किसी भी वीतराग तत्त्वज्ञके वचन निर्णायक हो सकते हैं । यानी पुरुष इतना विकास कर लेता है कि वह स्वयं तीर्थङ्कर बनकर तीर्थ ( धर्म ) का प्रवर्तन भी करता है ।