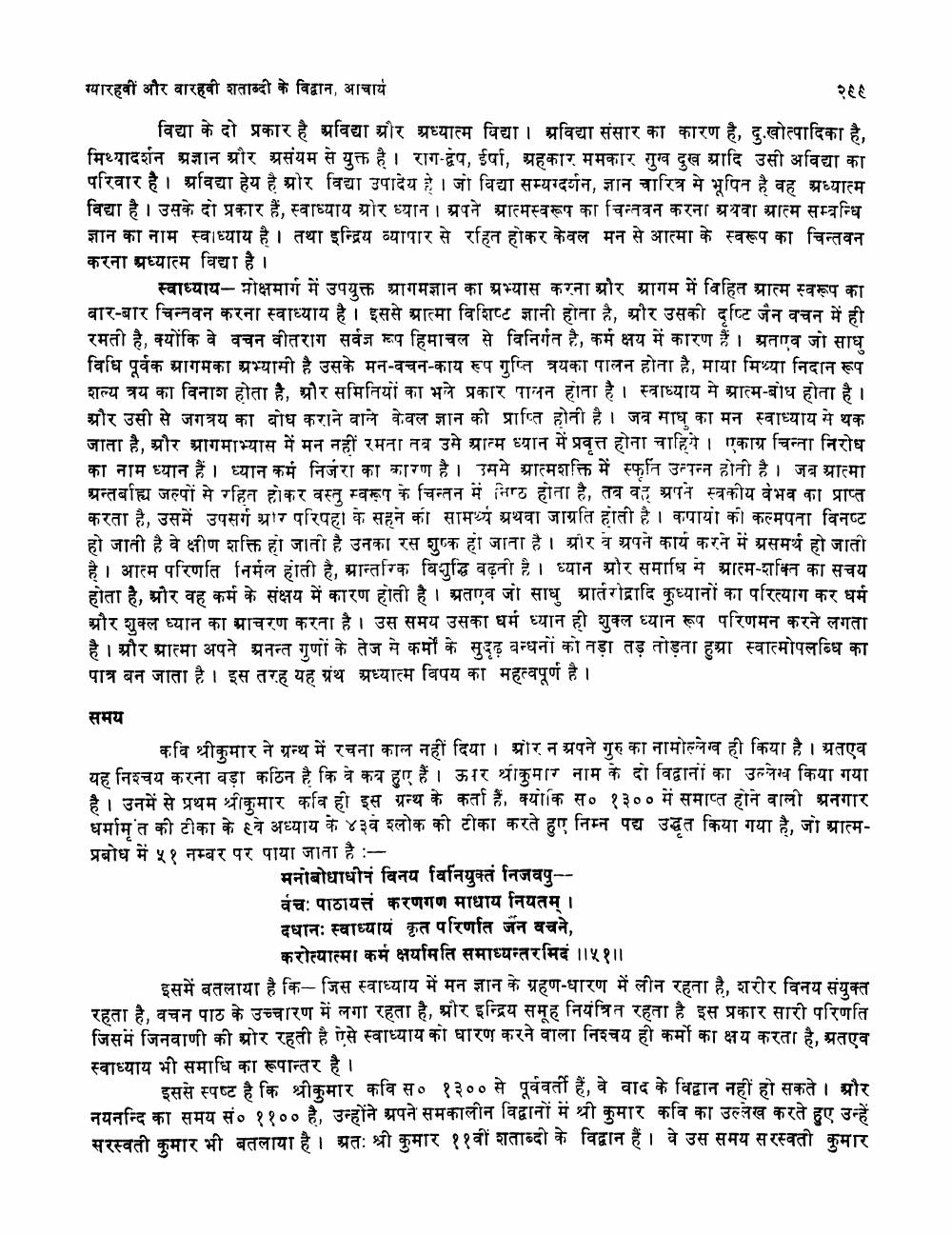________________
२६६
ग्यारहवीं और बारहवी शताब्दी के विद्वान आचार्य
विद्या के दो प्रकार है अविद्या और अध्यात्म विद्या अविद्या संसार का कारण है, दु.खोत्पादिका है, मिथ्यादर्शन अज्ञान और असंयम से युक्त है। राग-द्वेष, ईर्षा, ग्रहकार ममकार सुख दुख प्रादि उसी अविद्या का परिवार है। अविद्या हेय है और विद्या उपादेय है । जो विद्या सम्यग्दर्शन, ज्ञान चारित्र मे भूपित है वह अध्यात्म विद्या है। उसके दो प्रकार हैं, स्वाध्याय ओर ध्यान । अपने आत्मस्वरूप का चिन्तवन करना अथवा ग्रात्म सम्बन्धि ज्ञान का नाम स्वाध्याय है । तथा इन्द्रिय व्यापार से रहित होकर केवल मन से आत्मा के स्वरूप का चिन्तवन करना अध्यात्म विद्या है ।
स्वाध्याय - मोक्षमार्ग में उपयुक्त श्रागमज्ञान का अभ्यास करना और आगम में विहित प्रात्म स्वरूप का बार-बार चिन्नवन करना स्वाध्याय है। इससे आत्मा विशिष्ट ज्ञानी होता है, और उसकी दृष्टि जैन वचन में ही रमती है, क्योंकि वे वचन वीतराग सर्वज्ञ रूप हिमाचल से विनिर्गत है, कर्म क्षय में कारण हैं। अतएव जो साधु विधिपूर्वक आगमका अभ्यासी है उसके मन-वचन-काय रूप गुप्ति त्रयका पालन होता है, माया मिथ्या निदान रूप शल्यत्रय का विनाश होता है, और समितियों का भने प्रकार पालन होता है । स्वाध्याय मे ग्रात्म-बोध होता है । और उसी से जगत्रय का बोध कराने वाले केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है । जब साधु का मन स्वाध्याय से थक जाता है, और आगमाभ्यास में मन नहीं रमता तब उसे ग्रात्म ध्यान में प्रवृत्त होना चाहिये । एकाग्र चिन्ता निरोध का नाम ध्यान हैं। ध्यान कर्म निर्जरा का कारण है । उसमे आत्मशक्ति में स्कृति उत्पन्न होती है। जब आत्मा अन्तर्बाह्य जल्पों से रहित होकर वस्तु स्वरूप के चिन्तन में निष्ठ होता है, तब वह अपने स्वकीय वैभव का प्राप्त करता है, उसमें उपसर्ग भार परियहाँ के सहने की सामर्थ्य अथवा जाग्रति होती है । कपायों की कल्पता विनष्ट हो जाती है वे क्षीण शक्ति हो जाती है उनका रस शुष्क हो जाता है । और वे अपने कार्य करने में असमर्थ हो जाती है । आत्म परिणति निर्मल होती है, आन्तरिक विशुद्धि बढ़ती है। ध्यान और समाधि में आत्म-शक्ति का सचय होता है, और वह कर्म के संक्षय में कारण होती है । अतएव जो साधु श्रार्तराद्रादि कुध्यानों का परित्याग कर धर्म
र शुक्ल ध्यान का प्राचरण करता है। उस समय उसका धर्म ध्यान ही शुक्ल ध्यान रूप परिणमन करने लगता है । और आत्मा अपने अनन्त गुणों के तेज से कर्मों के सुदृढ़ बन्धनों को तड़ातड़ तोड़ता हुआ स्वात्मोपलब्धि का पात्र बन जाता है । इस तरह यह ग्रंथ अध्यात्म विषय का महत्वपूर्ण है ।
समय
और न अपने गुरु का नामोल्लेख ही किया है। अतएव ऊपर श्रीकुमार नाम के दो विद्वानों का उल्लेख किया गया कर्ता हैं, क्योंकि स० १३०० में समाप्त होने वाली अनगार टीका करते हुए निम्न पद्य उद्धृत किया गया है, जो आत्म
कवि श्रीकुमार ने ग्रन्थ में रचना काल नहीं दिया। यह निश्चय करना बड़ा कठिन है कि वे कब हुए हैं। है । उनमें से प्रथम श्रीकुमार कवि ही इस ग्रन्थ के धर्मामृत की टीका के हवे अध्याय के ४३वं श्लोक की प्रबोध में ५१ नम्बर पर पाया जाता है: मनोबोधाधीनं विनय विनियुक्तं निजवपु-वंच: पाठायत्तं करणगण माधाय नियतम् । दधानः स्वाध्यायं कृत परिणति जैन वचने, करोत्यात्मा कर्मक्षयमति समाध्यन्तरमिदं ॥ ५१ ॥
इसमें बतलाया है कि – जिस स्वाध्याय में मन ज्ञान के ग्रहण-धारण में लीन रहता है, शरीर विनय संयुक्त रहता है, वचन पाठ के उच्चारण में लगा रहता है, और इन्द्रिय समूह नियंत्रित रहता है इस प्रकार सारी परिणति जिसमें जिनवाणी की ओर रहती है ऐसे स्वाध्याय को धारण करने वाला निश्चय ही कर्मो का क्षय करता है, अतएव स्वाध्याय भी समाधि का रूपान्तर है ।
इससे स्पष्ट है कि श्रीकुमार कवि स० १३०० से पूर्ववर्ती हैं, वे वाद के विद्वान नहीं हो सकते । श्रर नयनन्दि का समय सं० ११०० है, उन्होंने अपने समकालीन विद्वानों में श्री कुमार कवि का उल्लेख करते हुए उन्हें सरस्वती कुमार : भी बतलाया है। अतः श्री कुमार ११वीं शताब्दी के विद्वान हैं। वे उस समय सरस्वती कुमार