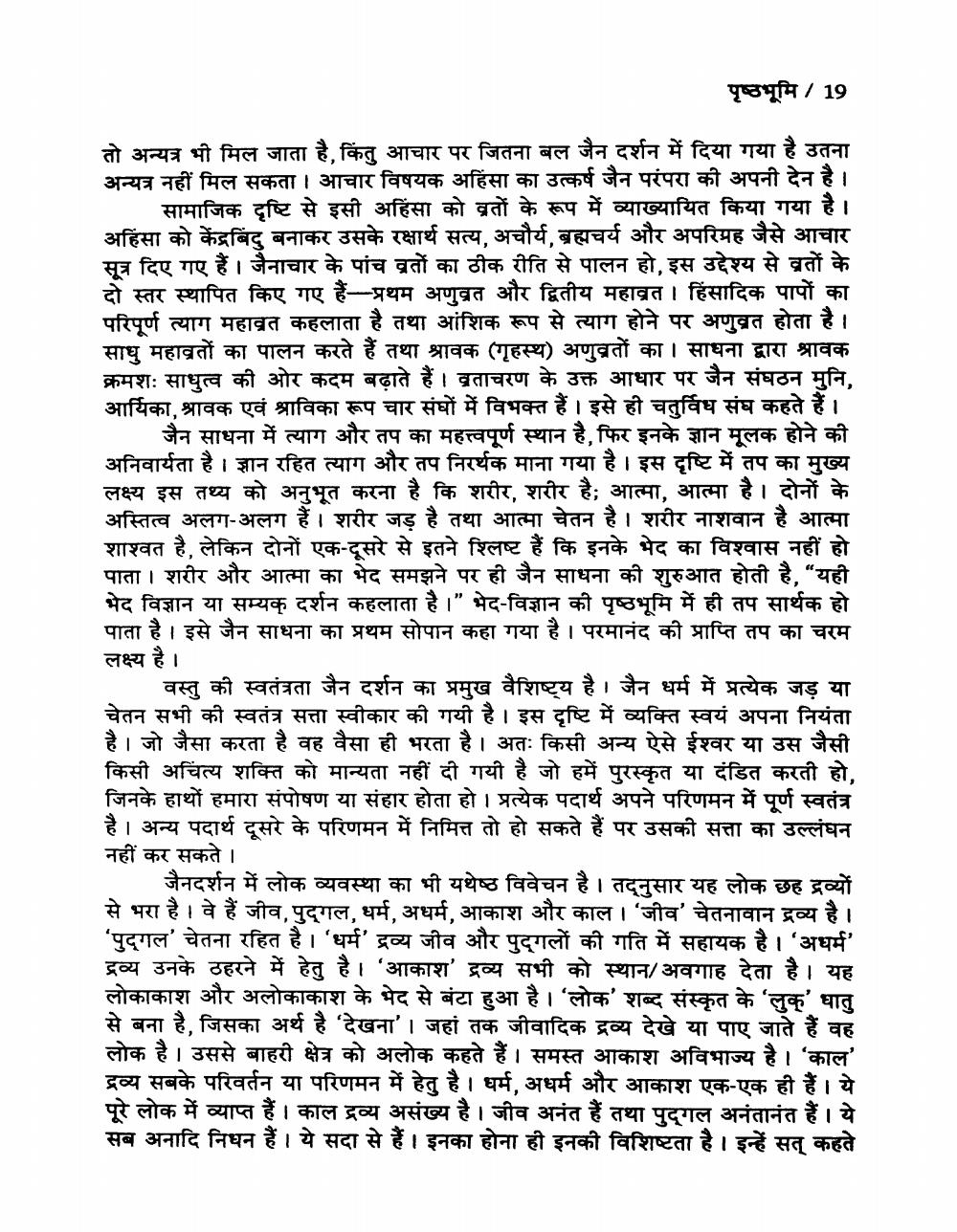________________
पृष्ठभूमि / 19
तो अन्यत्र भी मिल जाता है, किंतु आचार पर जितना बल जैन दर्शन में दिया गया है उतना अन्यत्र नहीं मिल सकता। आचार विषयक अहिंसा का उत्कर्ष जैन परंपरा की अपनी देन है।
सामाजिक दृष्टि से इसी अहिंसा को व्रतों के रूप में व्याख्यायित किया गया है। अहिंसा को केंद्रबिंदु बनाकर उसके रक्षार्थ सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे आचार सूत्र दिए गए हैं। जैनाचार के पांच व्रतों का ठीक रीति से पालन हो, इस उद्देश्य से व्रतों के दो स्तर स्थापित किए गए हैं-प्रथम अणुव्रत और द्वितीय महाव्रत । हिंसादिक पापों का परिपूर्ण त्याग महाव्रत कहलाता है तथा आंशिक रूप से त्याग होने पर अणुव्रत होता है। साधु महाव्रतों का पालन करते हैं तथा श्रावक (गृहस्थ) अणुव्रतों का । साधना द्वारा श्रावक क्रमशः साधुत्व की ओर कदम बढ़ाते हैं। व्रताचरण के उक्त आधार पर जैन संघठन मुनि, आर्यिका, श्रावक एवं श्राविका रूप चार संघों में विभक्त हैं। इसे ही चतुर्विध संघ कहते हैं।
जैन साधना में त्याग और तप का महत्त्वपर्ण स्थान है.फिर इनके ज्ञान मलक होने की अनिवार्यता है । ज्ञान रहित त्याग और तप निरर्थक माना गया है। इस दृष्टि में तप का मुख्य लक्ष्य इस तथ्य को अनुभूत करना है कि शरीर, शरीर है; आत्मा, आत्मा है। दोनों के अस्तित्व अलग-अलग हैं। शरीर जड़ है तथा आत्मा चेतन है। शरीर नाशवान है आत्मा शाश्वत है, लेकिन दोनों एक-दूसरे से इतने श्लिष्ट हैं कि इनके भेद का विश्वास नहीं हो पाता । शरीर और आत्मा का भेद समझने पर ही जैन साधना की शुरुआत होती है, “यही भेद विज्ञान या सम्यक दर्शन कहलाता है।" भेद-विज्ञान की पृष्ठभूमि में ही तप सार्थक हो पाता है। इसे जैन साधना का प्रथम सोपान कहा गया है। परमानंद की प्राप्ति तप का चरम लक्ष्य है।
वस्तु की स्वतंत्रता जैन दर्शन का प्रमुख वैशिष्ट्य है। जैन धर्म में प्रत्येक जड़ या चेतन सभी की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गयी है। इस दृष्टि में व्यक्ति स्वयं अपना नियंता है। जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। अतः किसी अन्य ऐसे ईश्वर या उस जैसी किसी अचिंत्य शक्ति को मान्यता नहीं दी गयी है जो हमें पुरस्कृत या दंडित करती हो, जिनके हाथों हमारा संपोषण या संहार होता हो । प्रत्येक पदार्थ अपने परिणमन में पूर्ण स्वतंत्र है। अन्य पदार्थ दूसरे के परिणमन में निमित्त तो हो सकते हैं पर उसकी सत्ता का उल्लंघन नहीं कर सकते।
जैनदर्शन में लोक व्यवस्था का भी यथेष्ठ विवेचन है । तद्नुसार यह लोक छह द्रव्यों से भरा है। वे हैं जीव,पुद्गल,धर्म, अधर्म, आकाश और काल । 'जीव' चेतनावान द्रव्य है। 'पुद्गल' चेतना रहित है। 'धर्म' द्रव्य जीव और पुद्गगलों की गति में सहायक है। 'अधर्म' द्रव्य उनके ठहरने में हेतु है। 'आकाश' द्रव्य सभी को स्थान/अवगाह देता है। यह लोकाकाश और अलोकाकाश के भेद से बंटा हुआ है। 'लोक' शब्द संस्कृत के 'लुक्' धातु से बना है, जिसका अर्थ है 'देखना' । जहां तक जीवादिक द्रव्य देखे या पाए जाते हैं वह लोक है। उससे बाहरी क्षेत्र को अलोक कहते हैं। समस्त आकाश अविभाज्य है। 'काल' द्रव्य सबके परिवर्तन या परिणमन में हेतु है। धर्म, अधर्म और आकाश एक-एक ही हैं। ये पूरे लोक में व्याप्त हैं। काल द्रव्य असंख्य है । जीव अनंत हैं तथा पुद्गल अनंतानंत हैं । ये सब अनादि निधन हैं। ये सदा से हैं। इनका होना ही इनकी विशिष्टता है। इन्हें सत् कहते