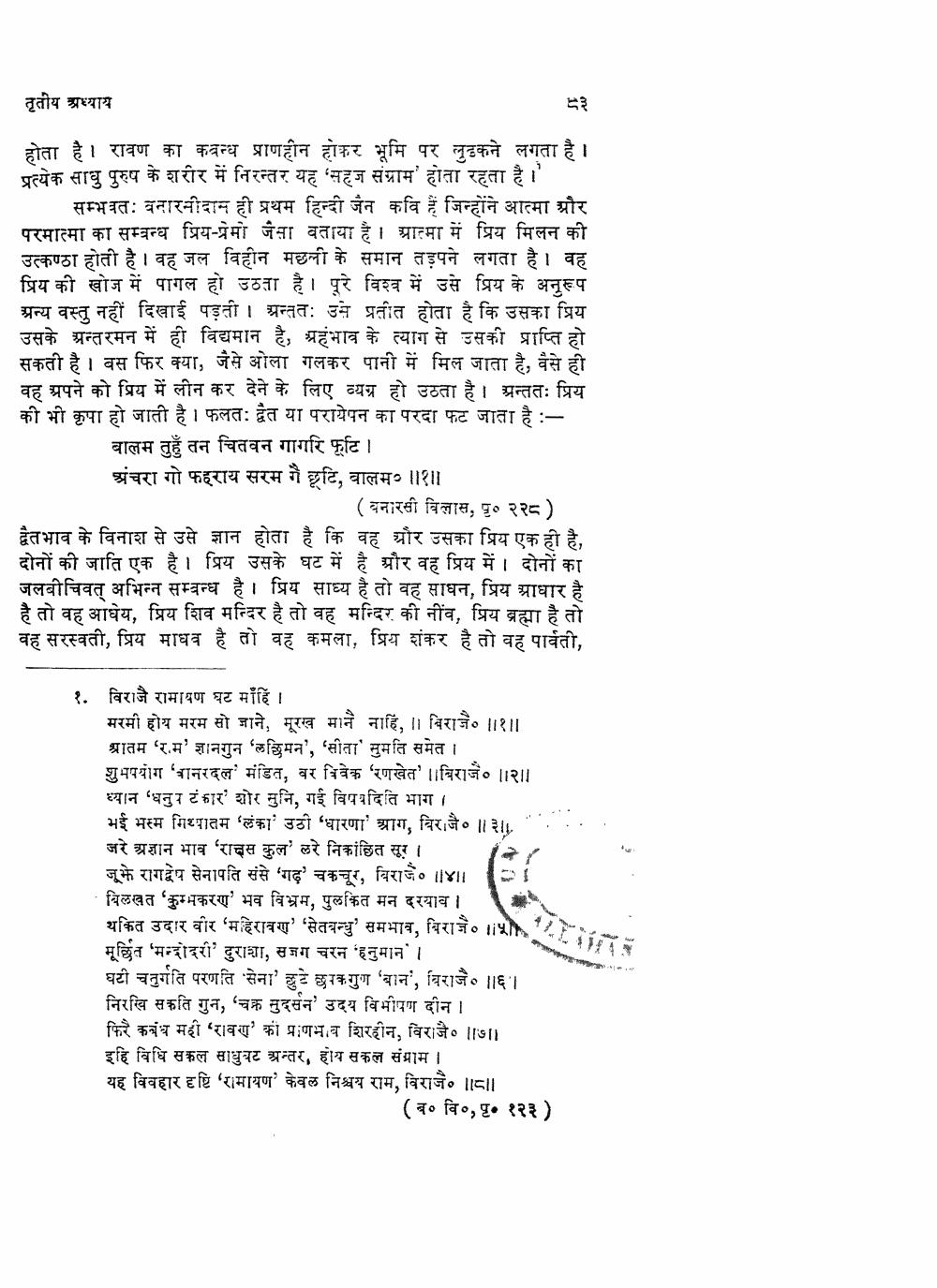________________
तृतीय अध्याय
होता है। रावण का कवन्ध प्राणहीन होकर भूमि पर लुढकने लगता है। प्रत्येक साधु पुरुष के शरीर में निरन्तर यह 'सहज संग्राम होता रहता है।
सम्भवत: बनारनीदान ही प्रथम हिन्दी जैन कवि हैं जिन्होंने आत्मा और परमात्मा का सम्बन्ध प्रिय-प्रेमो जैसा बताया है। प्रात्मा में प्रिय मिलन की उत्कण्ठा होती है। वह जल विहीन मछली के समान तड़पने लगता है। वह प्रिय की खोज में पागल हो उठता है। पूरे विश्व में उसे प्रिय के अनुरूप अन्य वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। अन्तत: उसे प्रतीत होता है कि उसका प्रिय उसके अन्तरमन में ही विद्यमान है, अहंभाव के त्याग से उसकी प्राप्ति हो सकती है। बस फिर क्या, जैसे ओला गलकर पानी में मिल जाता है, वैसे ही वह अपने को प्रिय में लीन कर देने के लिए व्यग्र हो उठता है। अन्ततः प्रिय की भी कृपा हो जाती है। फलतः द्वैत या परायेपन का परदा फट जाता है :
बालम तुहुँ तन चितवन गागरि फूटि । अंचरा गो फहराय सरम गै छुटि, बालम० ॥१॥
(बनारसी विलास, पृ० २२८) द्वैतभाव के विनाश से उसे ज्ञान होता है कि वह और उसका प्रिय एक ही है, दोनों की जाति एक है। प्रिय उसके घट में है और वह प्रिय में। दोनों का जलबीचिवत् अभिन्न सम्बन्ध है। प्रिय साध्य है तो वह साधन, प्रिय आधार है है तो वह आधेय, प्रिय शिव मन्दिर है तो वह मन्दिर की नींव, प्रिय ब्रह्मा है तो वह सरस्वती, प्रिय माधव है तो वह कमला, प्रिय शंकर है तो वह पार्वती,
विराजै रामायण घट माहिं । मरमी होय मरम सो जाने, मूरख मानै नाहि, ।। बिराजै० ॥१॥ श्रातम 'र.म' ज्ञानगुन 'लछिमन', 'सीता' मुमति समेत । शुभपयोग 'वानरदल' मंडित, वर विवेक रणखेत' ।।बिराजै ।।२।। ध्यान 'धनुष टंकार' शोर मुनि, गई विषयदिति भाग। भई भस्म मिथ्यातम 'लंका' उठी 'धारणा' श्राग, बिर जै॥३ जरे अज्ञान भाव 'राक्षस कुल' लरे निकांछित सूर । जूझे रागद्वेष सेनापति संसे 'गढ़' चकचूर, विराजे० ॥४॥ बिलखत 'कुम्भकरण' भव विभ्रम, पुलकित मन दरयाव।। थकित उदार वीर 'महिरावण' 'सेतबन्धु' समभाव, बिराजै ।। मूर्छित 'मन्दोदरी' दुराशा, सजग चरन 'हनुमान । घटी चतुर्गति परणति 'सेना' छुटे छपक गुण 'बान', बिराजै ॥६॥ निरखि स कति गुन, 'चक्र सुदर्सन' उदय विभीपण दीन । फिरै कबंध मही 'रावण' की प्राणभाव शिरहीन, विराजै ॥७॥ इहि विधि सकल साधुवट अन्तर, होय सकल संग्राम । यह विवहार दृष्टि 'रामायण' केवल निश्चय राम, विराजै ॥८॥
(ब० वि०, पृ. १२३)
13