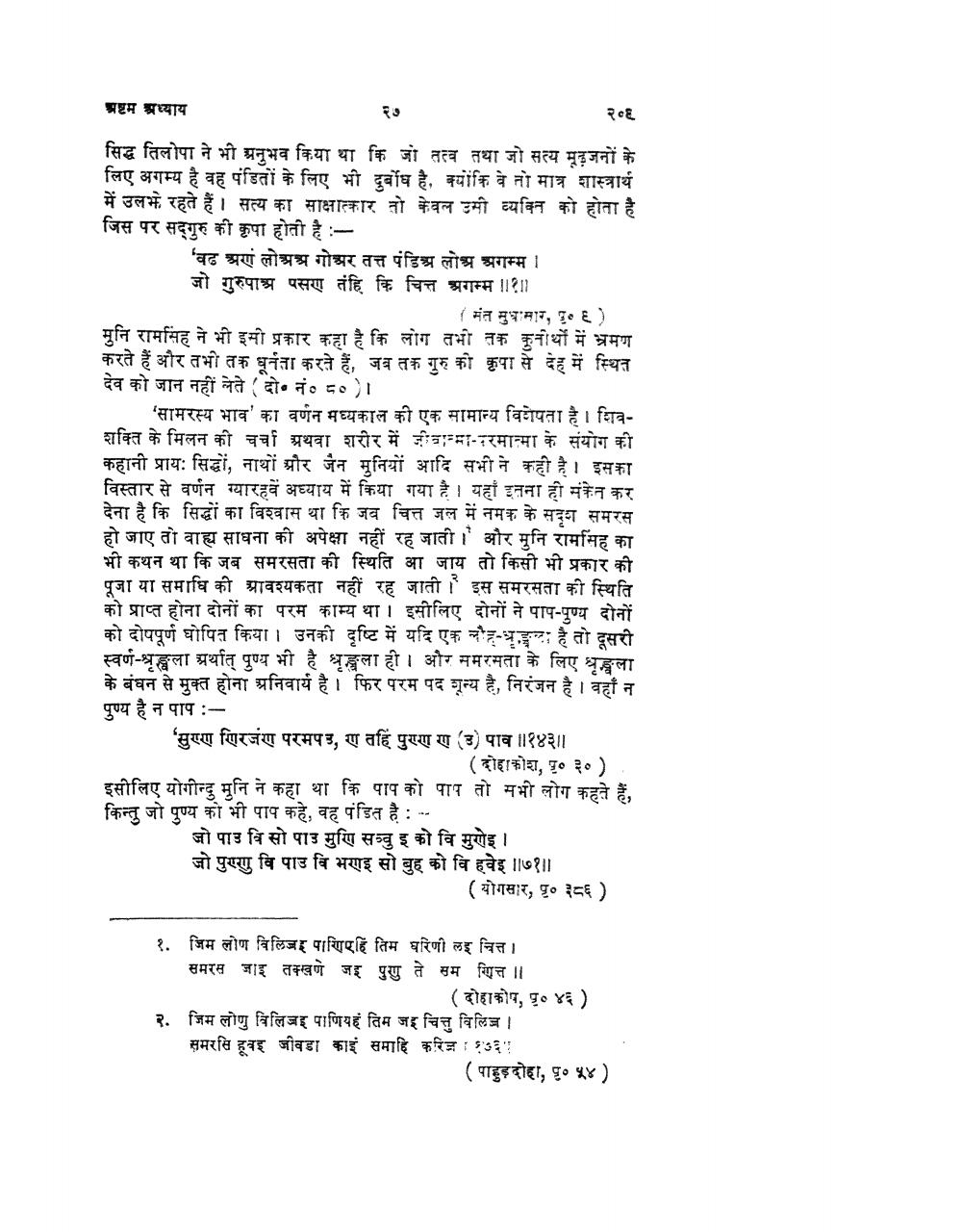________________
अष्टम अध्याय
२०६
सिद्ध तिलोपा ने भी अनुभव किया था कि जो तत्व तथा जो सत्य मूढजनों के लिए अगम्य है वह पंडितों के लिए भी दुर्बोध है, क्योंकि वे तो मात्र शास्त्रार्थ में उलझे रहते हैं। सत्य का साक्षात्कार तो केवल उसी व्यक्ति को होता है जिस पर सद्गुरु की कृपा होती है :
'वढ अणं लोअप गोअर तत्त पंडिअलोभ अगम्म । जो गुरुपाअ पसण तंहि कि चित्त अगम्म ||2||
मंत मुधामार, पृ०६) मुनि रामसिंह ने भी इमो प्रकार कहा है कि लोग तभी तक कुनीथों में भ्रमण करते हैं और तभी तक धूर्तता करते हैं, जब तक गुरु की कृपा से देह में स्थित देव को जान नहीं लेते (दो. नं०८०)।
'सामरस्य भाव' का वर्णन मध्यकाल की एक सामान्य विशेषता है। शिवशक्ति के मिलन की चर्चा अथवा शरीर में जीवात्मा-परमात्मा के संयोग की कहानी प्रायः सिद्धों, नाथों और जैन मुनियों आदि सभी ने कही है। इसका विस्तार से वर्णन ग्यारहवें अध्याय में किया गया है। यहाँ इतना ही संकेत कर देना है कि सिद्धों का विश्वास था कि जब चित्त जल में नमक के सदृश समरस हो जाए तो बाह्य साधना की अपेक्षा नहीं रह जाती।' और मुनि रामसिंह का भी कथन था कि जब समरसता की स्थिति आ जाय तो किसी भी प्रकार की पूजा या समाधि की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस समरसता की स्थिति को प्राप्त होना दोनों का परम काम्य था। इसीलिए दोनों ने पाप-पुण्य दोनों को दोषपूर्ण घोपित किया। उनकी दृष्टि में यदि एक दोह-अङ्कला है तो दूसरी स्वर्ण-श्रङ्खला अर्थात् पुण्य भी है श्रृङ्खला ही। और ममरमता के लिए श्रङ्गला के बंधन से मुक्त होना अनिवार्य है। फिर परम पद शून्य है, निरंजन है। वहाँ न पुण्य है न पाप :'सुण्ण णिरजण परमपउ, ण तहिं पुरण ण (उ) पाव ॥१४३।।
(दोहाकोश, पृ०३०) इसीलिए योगीन्दु मुनि ने कहा था कि पाप को पाप तो सभी लोग कहते हैं, किन्तु जो पुण्य को भी पाप कहे, वह पंडित है : ...
जो पाउ विसो पाउ मुणि सञ्चु इ को वि मुणेइ। जो पुण्णु वि पाउ वि भणइ सो बुह को वि हवेइ ॥७१॥
(योगसार, पृ० ३८६)
१. जिम लोण विलिजह पाणिएहिं तिम घरिणी लइ चित्त । समरस जाइ तखणे जइ पुणु ते सम पित्त ।।
(दोहाकोप, पृ० ४६) २. जिम लोणु विलिजइ पाणियहं तिम जइ चित्तु विलिन । समरसि हूवइ जीवडा काई समाहि करिज : १७६"
(पाहुड़दोहा, पृ०५४)