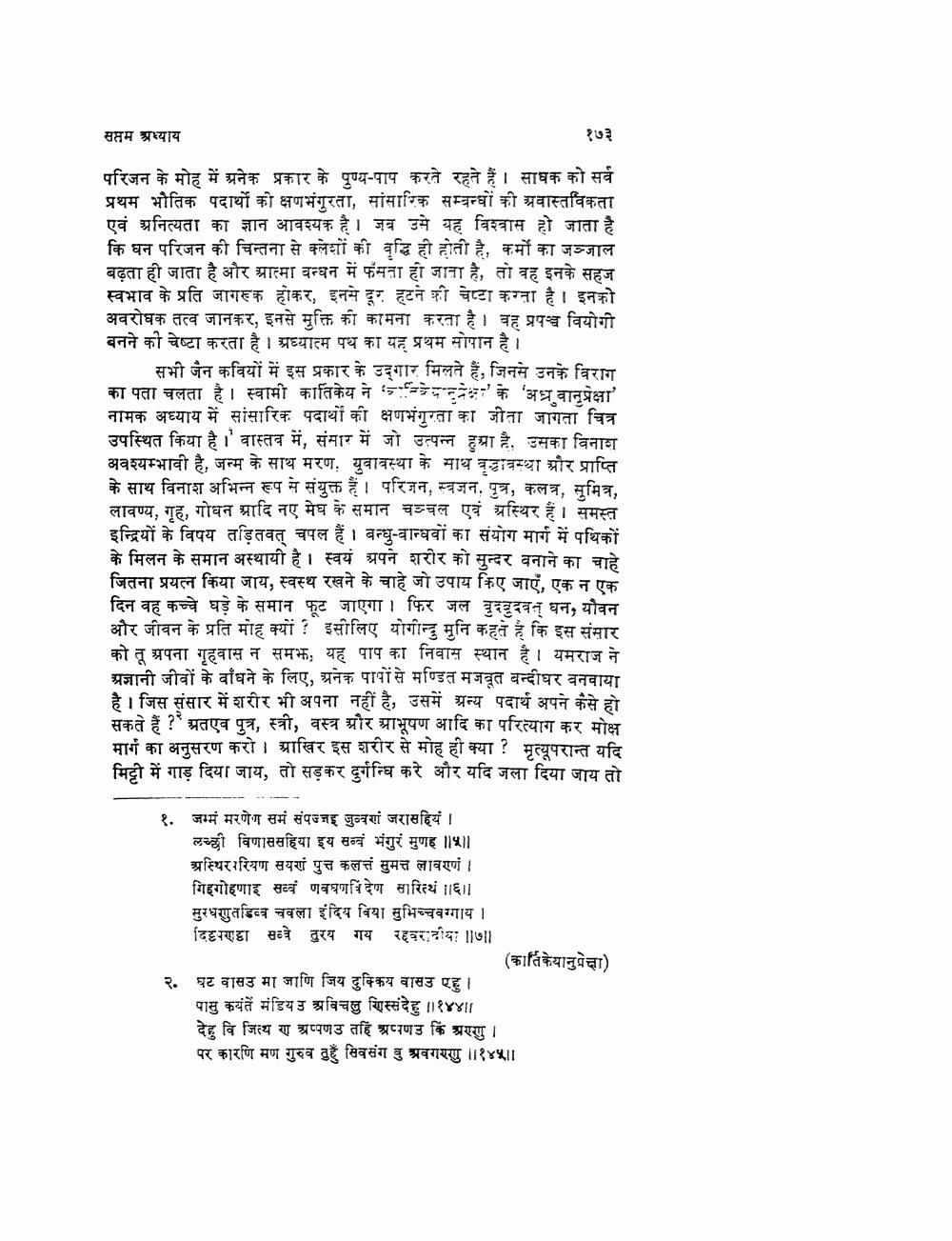________________
सप्तम अध्याय
१७३
परिजन के मोह में अनेक प्रकार के पुण्य-पाप करते रहते हैं। साधक को सर्व प्रथम भौतिक पदार्थों की क्षणभंगुरता, सांसारिक सम्बन्धों की अवास्तविकता एवं अनित्यता का ज्ञान आवश्यक है। जब उसे यह विश्वास हो जाता है कि धन परिजन की चिन्तना से क्लेशों की वृद्धि ही होती है, कर्मों का जञ्जाल बढ़ता ही जाता है और आत्मा बन्धन में फंसता ही जाता है, तो वह इनके सहज स्वभाव के प्रति जागरूक होकर, इनसे दूर हटने की चेष्टा करता है। इनको अवरोधक तत्व जानकर, इनसे मुक्ति की कामना करता है। वह प्रपञ्च वियोगी बनने की चेष्टा करता है। अध्यात्म पथ का यह प्रथम सोपान है।
सभी जैन कवियों में इस प्रकार के उद्गार मिलते हैं, जिनसे उनके विराग का पता चलता है। स्वामी कातिकेय ने नोभा' के 'अध्र वानप्रेक्षा' नामक अध्याय में सांसारिक पदार्थों की क्षणभंगुरता का जीता जागता चित्र उपस्थित किया है। वास्तव में, संमार में जो उत्पन्न हया है, उसका विनाश अवश्यम्भावी है, जन्म के साथ मरण, युवावस्था के माथ वृद्धावस्था और प्राप्ति के साथ विनाश अभिन्न रूप से संयुक्त हैं। परिजन, स्वजन, पुत्र, कलत्र, सुमित्र, लावण्य, गृह, गोधन आदि नए मेघ के समान चञ्चल एवं अस्थिर हैं। समस्त इन्द्रियों के विषय तड़ितवत् चपल हैं। बन्धु-वान्धवों का संयोग मार्ग में पथिकों के मिलन के समान अस्थायी है। स्वयं अपने शरीर को सुन्दर बनाने का चाहे जितना प्रयत्न किया जाय, स्वस्थ रखने के चाहे जो उपाय किए जाएँ, एक न एक दिन वह कच्चे घड़े के समान फूट जाएगा। फिर जल बुदबुदवत् धन, यौवन और जीवन के प्रति मोह क्यों? इसीलिए योगीन्दु मुनि कहते है कि इस संसार को तू अपना गृहवास न समझ, यह पाप का निवास स्थान है। यमराज ने अज्ञानी जीवों के बाँधने के लिए, अनेक पापों से मण्डित मजबूत बन्दीघर बनवाया है। जिस संसार में शरीर भी अपना नहीं है, उसमें अन्य पदार्थ अपने कैसे हो सकते हैं ? अतएव पुत्र, स्त्री, वस्त्र और आभूषण आदि का परित्याग कर मोक्ष मार्ग का अनुसरण करो। आखिर इस शरीर से मोह ही क्या? मृत्यूपरान्त यदि मिट्री में गाड़ दिया जाय, तो सड़कर दुर्गन्धि करे और यदि जला दिया जाय तो
१. जम्म मरणेण समं संपज्जइ जुब्वणं जरासहियं ।
लच्छी विणाससहिया इय सव्वं भंगुरं मुणह ॥५॥ अस्थिरररियण सयणं पुत्त कलत्तं सुमत्त लावएणं । गिइगोहणाइ सव्वं णवघणविदेण सारित्थं ।।६।। मुरधणुतडिव चवला इंदिय विया सुभिच्चवग्गाय । दिडपण्डा सव्वे तुरय गय रहबर दीयः ॥७॥
(कार्तिकेयानुप्रेक्षा) घट वासउ मा जाणि जिय दुक्किय वासउ एहु । पासु कयंतें मंडिय उ अविचलु हिस्संदेहु ॥१४४।। देहु वि जित्य ण अप्पणउ तहिं अपणउ किं अण्णु । पर कारणि मण गुरुव तुहुँ सिवसंग वु अवगएणु ।।१४५।।