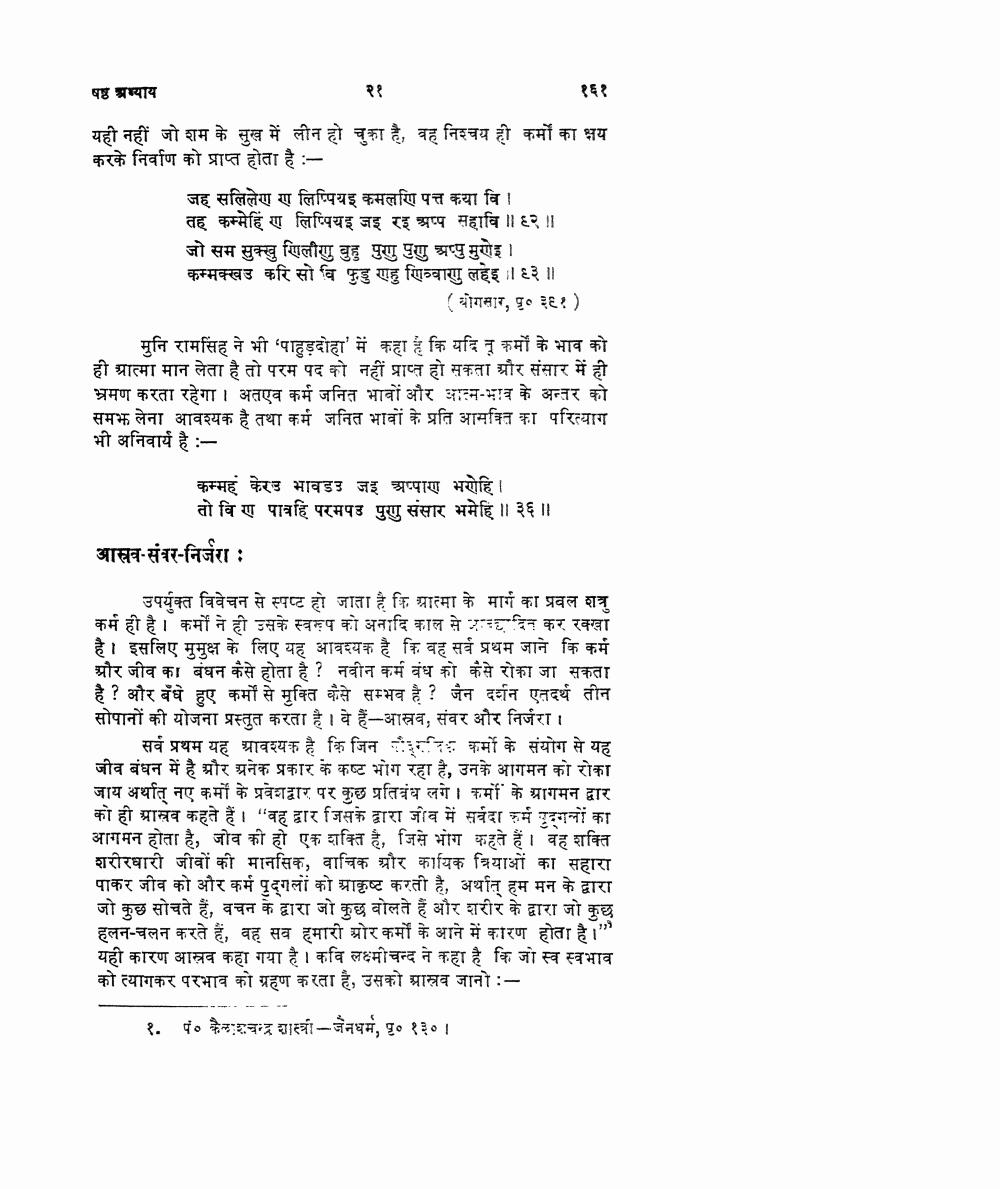________________
षष्ठ अध्याय
२१
१६१
यही नहीं जो शम के सुख में लीन हो चुका है, वह निश्चय ही कर्मों का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त होता है :
जह सलिलेण ण लिप्पियइ कमलपित्त क्या वि । तह कम्मेहिंग लिप्पियइ जइ रइ अप्प महावि ॥ ६२ ॥ जो सम सुक्खु गिली बहु पुगु पुणु अप्पु मुणेइ | कम्मक्खउ करि सो वि फुड राहु त्रिवागु लहेइ ॥ ६३ ॥ ( योगसार, पृ० ३६१ )
मुनि रामसिंह ने भी 'पाहुड़दोहा' में कहा है कि यदि तु कर्मों के भाव को ही श्रात्मा मान लेता है तो परम पद को नहीं प्राप्त हो सकता और संसार में ही भ्रमण करता रहेगा । अतएव कर्म जनित भावों और आत्म-भाव के अन्तर को समझ लेना आवश्यक है तथा कर्म जनित भावों के प्रति आसक्ति का परित्याग भी अनिवार्य है
--
कम्महं केरउ भावडर जइ अप्पा भणेहि । तो वि पात्रहि परमपउ पुगु संसार भमेहिं ॥ ३६ ॥ आस्रव-संवर-निर्जरा :
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि श्रात्मा के मार्ग का प्रबल शत्रु कर्म ही है । कर्मों ने ही उसके स्वरूप को अनादि काल से कर रक्खा है । इसलिए मुमुक्ष के लिए यह आवश्यक है कि वह सर्व प्रथम जाने कि कर्म और जीव का बंधन कैसे होता है ? नवीन कर्म बंध को कैसे रोका जा सकता है ? और बंधे हुए कर्मों से मुक्ति कैसे सम्भव है ? जैन दर्शन एतदर्थं तीन सोपानों की योजना प्रस्तुत करता है । वे हैं-आस्रव, संवर और निर्जरा |
सर्व प्रथम यह आवश्यक है कि जिन
I
कर्मो के संयोग से यह जीव बंधन में है और अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहा है, उनके आगमन को रोका जाय अर्थात् नए कर्मों के प्रवेशद्वार पर कुछ प्रतिबंध लगे । कर्मों के ग्रागमन द्वार को ही आस्रव कहते हैं । "वह द्वार जिसके द्वारा जीव में सर्वदा कर्म युगलों का आगमन होता है, जोव की हो एक शक्ति जिसे भोग कहते हैं। वह शक्ति शरीरधारी जीवों की मानसिक, वाचिक और कायिक क्रियाओं का सहारा पाकर जीव को और कर्म पुद्गलों को आकृष्ट करती है, अर्थात् हम मन के द्वारा जो कुछ सोचते हैं, वचन के द्वारा जो कुछ बोलते हैं और शरीर के द्वारा जो कुछ हलन चलन करते हैं, वह सब हमारी ओर कर्मों के आने में कारण होता है।" यही कारण आस्रव कहा गया है । कवि लक्ष्मीचन्द ने कहा है कि जो स्व स्वभाव को त्यागकर परभाव को ग्रहण करता है, उसको आस्रव जानो :
पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री —– जैनधर्म, पृ० १३० ।
१.