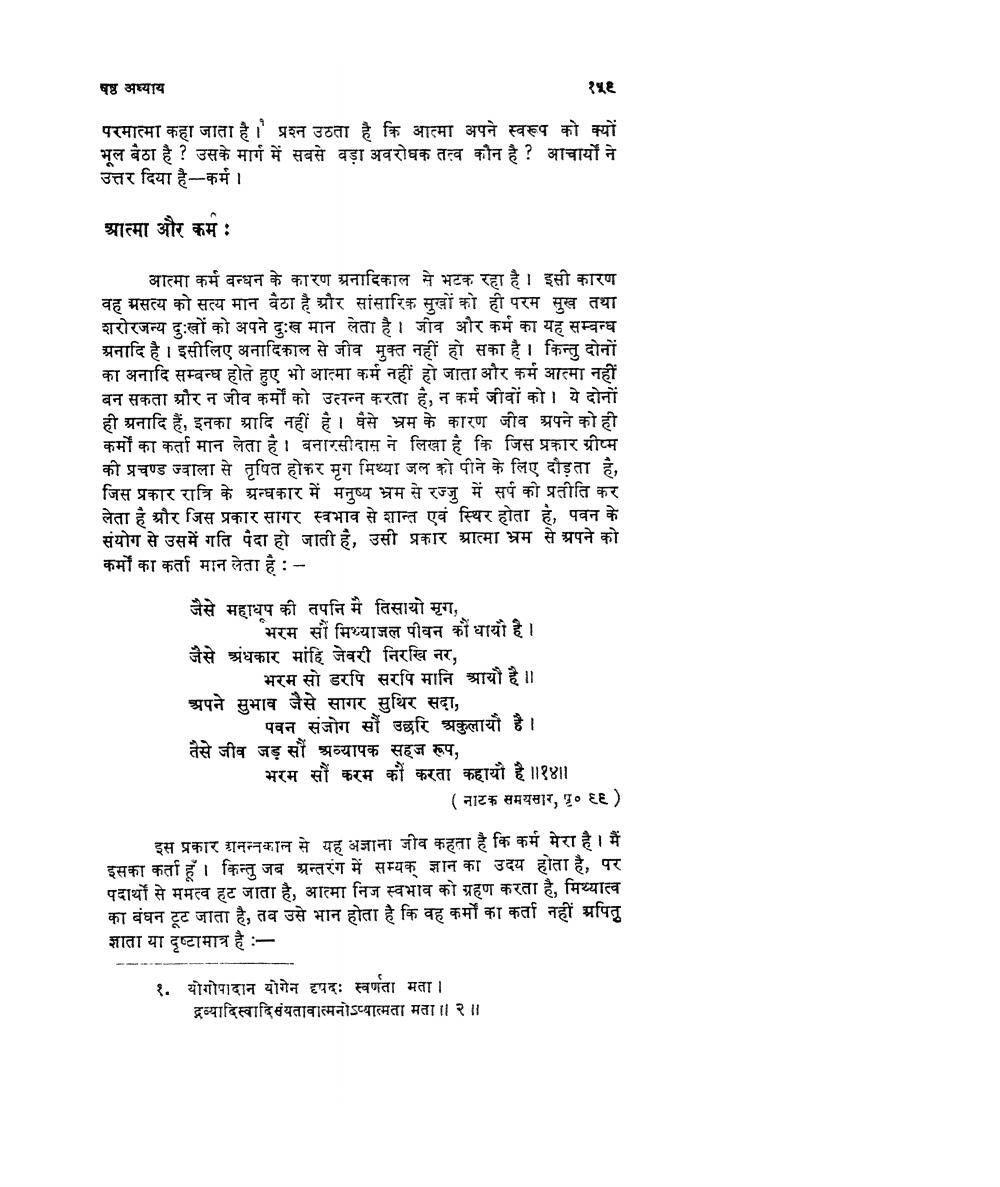________________
षष्ठ अध्याय
१५१
परमात्मा कहा जाता है। प्रश्न उठता है कि आत्मा अपने स्वरूप को क्यों भूल बैठा है ? उसके मार्ग में सबसे बड़ा अवरोधक तत्व कौन है ? आचार्यों ने उत्तर दिया है - कर्म ।
आत्मा और कर्म :
आत्मा कर्म बन्धन के कारण अनादिकाल से भटक रहा है। इसी कारण वह असत्य को सत्य मान बैठा है और सांसारिक सुखों को ही परम सुख तथा शरीरजन्य दुःखों को अपने दुःख मान लेता है। जीव और कर्म का यह सम्वन्ध अनादि है। इसीलिए अनादिकाल से जीव मुक्त नहीं हो सका है। किन्तु दोनों का अनादि सम्बन्ध होते हुए भी आत्मा कर्म नहीं हो जाता और कर्म आत्मा नहीं बन सकता और न जीव कर्मों को उत्सन्न करता है, न कर्म जीवों को। ये दोनों ही अनादि हैं, इनका मादि नहीं है। वैसे भ्रम के कारण जीव अपने को ही कर्मों का कर्ता मान लेता है। बनारसीदास ने लिखा है कि जिस प्रकार ग्रीष्म की प्रचण्ड ज्वाला से तृषित होकर मृग मिथ्या जल को पीने के लिए दौड़ता है, जिस प्रकार रात्रि के अन्धकार में मनुष्य भ्रम से रज्जु में सर्प को प्रतीति कर लेता है और जिस प्रकार सागर स्वभाव से शान्त एवं स्थिर होता है, पवन के संयोग से उसमें गति पैदा हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा भ्रम से अपने को कर्मों का कर्ता मान लेता है :
जैसे महाधूप की सपनि मे तिसावी मृग,
"भरम सी मिध्याजल पीवन की थायी है। जैसे अंधकार मांहि जेवरी निरखि नर,
भरम सो डरपि सरपि मानि आयो है ॥
अपने सुभाव जैसे सागर सुथिर सदा,
पवन संजोग सौ उहरि अकुलायौ है। तैसे जीव जड़ सौं अव्यापक सहज रूप,
भरम सौं करम कौं करता कहायौ है || १४ || ( नाटक समयसार, पृ० ६६ )
इस प्रकार ग्रनन्तकाल से यह अज्ञाना जीव कहता है कि कर्म मेरा है। मैं इसका कर्ता हूँ । किन्तु जब अन्तरंग में सम्यक् ज्ञान का उदय होता है, पर पदार्थों से ममत्व हट जाता है, आत्मा निज स्वभाव को ग्रहण करता है, मिथ्यात्व का बंधन टूट जाता है, तब उसे भान होता है कि वह कर्मों का कर्ता नहीं अपितु शाता या दृष्टामात्र है :
१. योगोपादान योगेन हृपदः स्वर्णता मता । द्रव्यादिस्वादिसंयतावात्मनोऽप्यात्मता मता ॥ २ ॥