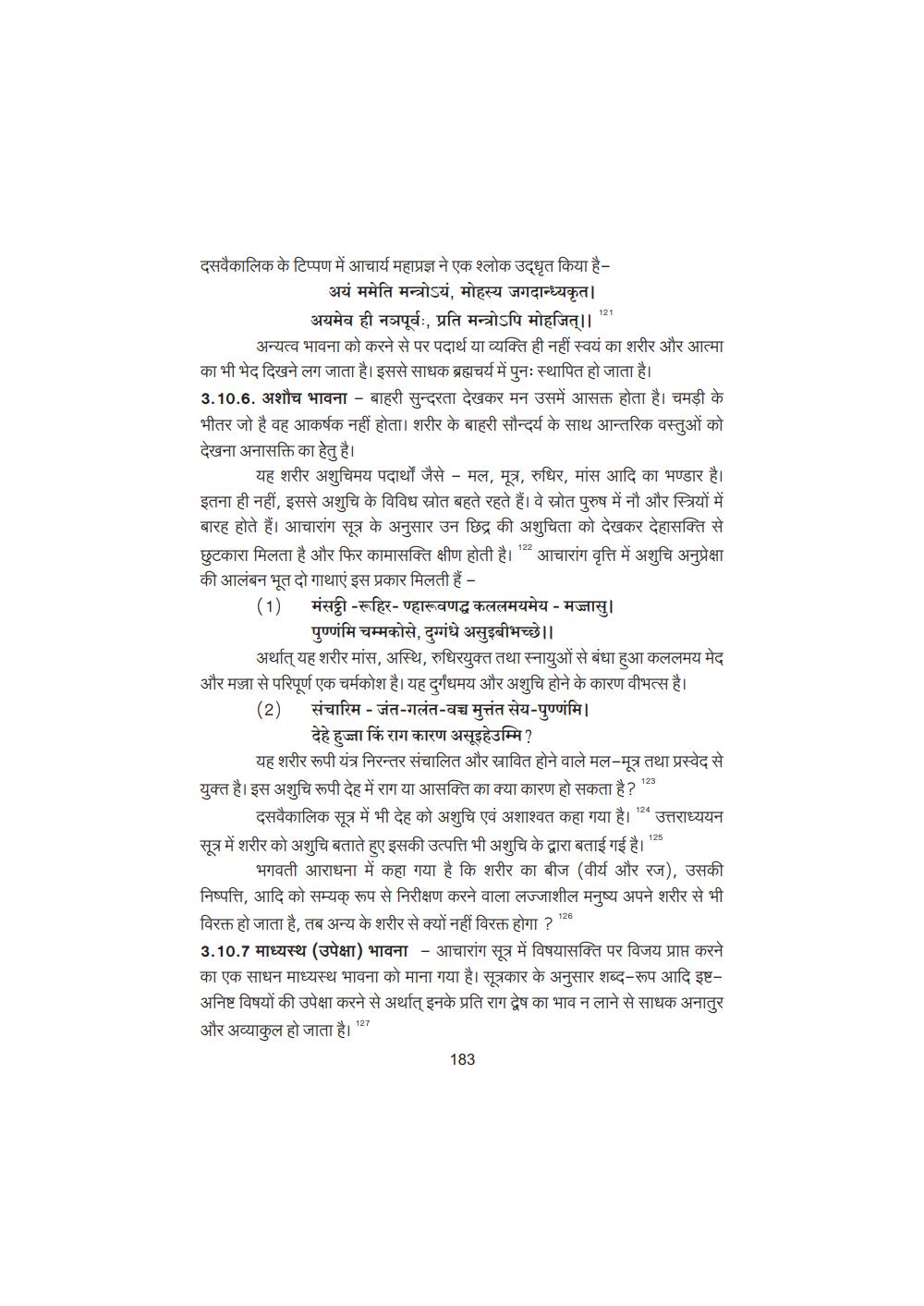________________
दसवैकालिक के टिप्पण में आचार्य महाप्रज्ञ ने एक श्लोक उद्धृत किया है
अयं ममेति मन्त्रोऽयं, मोहस्य जगदान्ध्यकृत । अयमेव ही नञपूर्वः, प्रति मन्त्रोऽपि मोहजित् ।।
121
अन्यत्व भावना को करने से पर पदार्थ या व्यक्ति ही नहीं स्वयं का शरीर और आत्मा का भी भेद दिखने लग जाता है। इससे साधक ब्रह्मचर्य में पुनः स्थापित हो जाता है। 3.10.6. अशौच भावना - बाहरी सुन्दरता देखकर मन उसमें आसक्त होता है। चमड़ी के भीतर जो है वह आकर्षक नहीं होता। शरीर के बाहरी सौन्दर्य के साथ आन्तरिक वस्तुओं को देखना अनासक्ति का हेतु है।
यह शरीर अशुचिमय पदार्थों जैसे मल, मूत्र, रुधिर, मांस आदि का भण्डार है। इतना ही नहीं, इससे अशुचि के विविध स्रोत बहते रहते हैं। वे स्रोत पुरुष में नौ और स्त्रियों में बारह होते हैं। आचारांग सूत्र के अनुसार उन छिद्र की अशुचिता को देखकर देहासक्ति से छुटकारा मिलता है और फिर कामासक्ति क्षीण होती है। आचारांग वृत्ति में अशुचि अनुप्रेक्षा की आलंबन भूत दो गाथाएं इस प्रकार मिलती हैं -
(1)
मंसट्ठी - रूहिर- हारूवणद्ध कललमयमेय मज्जासु । पुण्णमिचम्मकोसे, दुग्गंधे असुहबीभच्छे।।
अर्थात् यह शरीर मांस, अस्थि, रुधिरयुक्त तथा स्नायुओं से बंधा हुआ कललमय मेद और मजा से परिपूर्ण एक चर्मकोश है। यह दुर्गंधमय और अशुचि होने के कारण वीभत्स है। संचारिम- जंत-गलंत - वच्च मुत्तंत सेय- पुण्णंमि । देहे हुज्जा किं राग कारण असुइहेउम्मि ?
(2)
123
124
125
यह शरीर रूपी यंत्र निरन्तर संचालित और स्रावित होने वाले मल-मूत्र तथा प्रस्वेद से युक्त है। इस अशुचि रूपी देह में राग या आसक्ति का क्या कारण हो सकता है ? दसवैकालिक सूत्र में भी देह को अशुचि एवं अशाश्वत कहा गया है। सूत्र में शरीर को अशुचि बताते हुए इसकी उत्पत्ति भी अशुचि के द्वारा बताई गई है। भगवती आराधना में कहा गया है कि शरीर का बीज (वीर्य और रज), उसकी निष्पत्ति, आदि को सम्यक् रूप से निरीक्षण करने वाला लज्जाशील मनुष्य अपने शरीर से भी विरक्त हो जाता है, तब अन्य के शरीर से क्यों नहीं विरक्त होगा ?
उत्तराध्ययन
3.10.7 माध्यस्थ (उपेक्षा) भावना आचारांग सूत्र में विषयासक्ति पर विजय प्राप्त करने का एक साधन माध्यस्थ भावना को माना गया है। सूत्रकार के अनुसार शब्द-रूप आदि इष्टअनिष्ट विषयों की उपेक्षा करने से अर्थात् इनके प्रति राग द्वेष का भाव न लाने से साधक अनातुर और अव्याकुल हो जाता है।
127
183