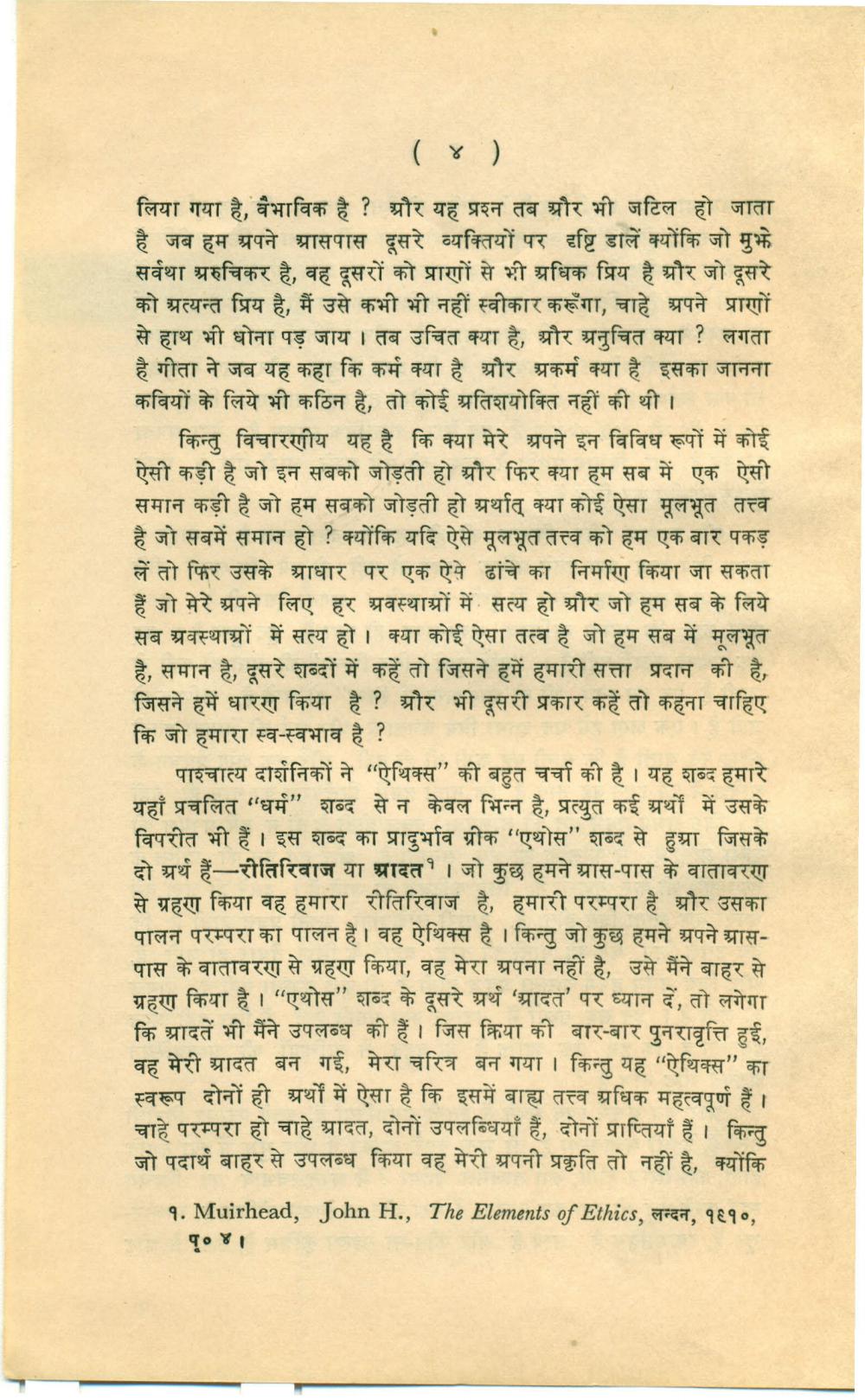________________
( ४ )
लिया गया है, वैभाविक है ? और यह प्रश्न तब और भी जटिल हो जाता है जब हम अपने आसपास दूसरे व्यक्तियों पर दृष्टि डालें क्योंकि जो मुझे सर्वथा अरुचिकर है, वह दूसरों को प्रारणों से भी अधिक प्रिय है और जो दूसरे को अत्यन्त प्रिय है, मैं उसे कभी भी नहीं स्वीकार करूँगा, चाहे अपने प्राणों से हाथ भी धोना पड़ जाय । तब उचित क्या है, और अनुचित क्या ? लगता है गीता ने जब यह कहा कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसका जानना कवियों के लिये भी कठिन है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं की थी ।
किन्तु विचारणीय यह है कि क्या मेरे अपने इन विविध रूपों में कोई ऐसी कड़ी है जो इन सबको जोड़ती हो और फिर क्या हम सब में एक ऐसी समान कड़ी है जो हम सबको जोड़ती हो अर्थात् क्या कोई ऐसा मूलभूत तत्त्व है जो सबमें समान हो ? क्योंकि यदि ऐसे मूलभूत तत्त्व को हम एक बार पकड़ लें तो फिर उसके आधार पर एक ऐसे ढांचे का निर्माण किया जा सकता हैं जो मेरे अपने लिए हर अवस्थाओं में सत्य हो और जो हम सब के लिये सब अवस्थाओं में सत्य हो । क्या कोई ऐसा तत्व है जो हम सब में मूलभूत है, समान है, दूसरे शब्दों में कहें तो जिसने हमें हमारी सत्ता प्रदान की है, जिसने हमें धारण किया है ? और भी दूसरी प्रकार कहें तो कि जो हमारा स्व-स्वभाव है ?
कहना चाहिए
पाश्चात्य दार्शनिकों ने "ऐथिक्स" की बहुत चर्चा की है । यह शब्द हमारे यहाँ प्रचलित "धर्म" शब्द से न केवल भिन्न है, प्रत्युत कई अर्थों में उसके विपरीत भी हैं । इस शब्द का प्रादुर्भाव ग्रीक "एथोस" शब्द से हुआ जिसके दो अर्थ हैं - रीतिरिवाज या श्रादत' । जो कुछ हमने ग्रास-पास के वातावरण से ग्रहण किया वह हमारा रीतिरिवाज है, हमारी परम्परा है और उसका पालन परम्परा का पालन है । वह ऐथिक्स है । किन्तु जो कुछ हमने अपने आसपास के वातावरण से ग्रहण किया, वह मेरा अपना नहीं है, उसे मैंने बाहर से ग्रहण किया है । " एथोस" शब्द के दूसरे अर्थ 'आदत' पर ध्यान दें, तो लगेगा कि श्रादतें भी मैंने उपलब्ध की हैं। जिस क्रिया की बार-बार पुनरावृत्ति हुई, वह मेरी आदत बन गई, मेरा चरित्र बन गया । किन्तु यह “ऐथिक्स" का स्वरूप दोनों ही अर्थों में ऐसा है कि इसमें बाह्य तत्त्व अधिक महत्वपूर्ण हैं । चाहे परम्परा हो चाहे श्रादत, दोनों उपलब्धियाँ हैं, दोनों प्राप्तियाँ हैं । किन्तु जो पदार्थ बाहर से उपलब्ध किया वह मेरी अपनी प्रकृति तो नहीं है, क्योंकि
१. Muirhead, John H., The Elements of Ethics, लन्दन, १६१०, पृ० ४ ।