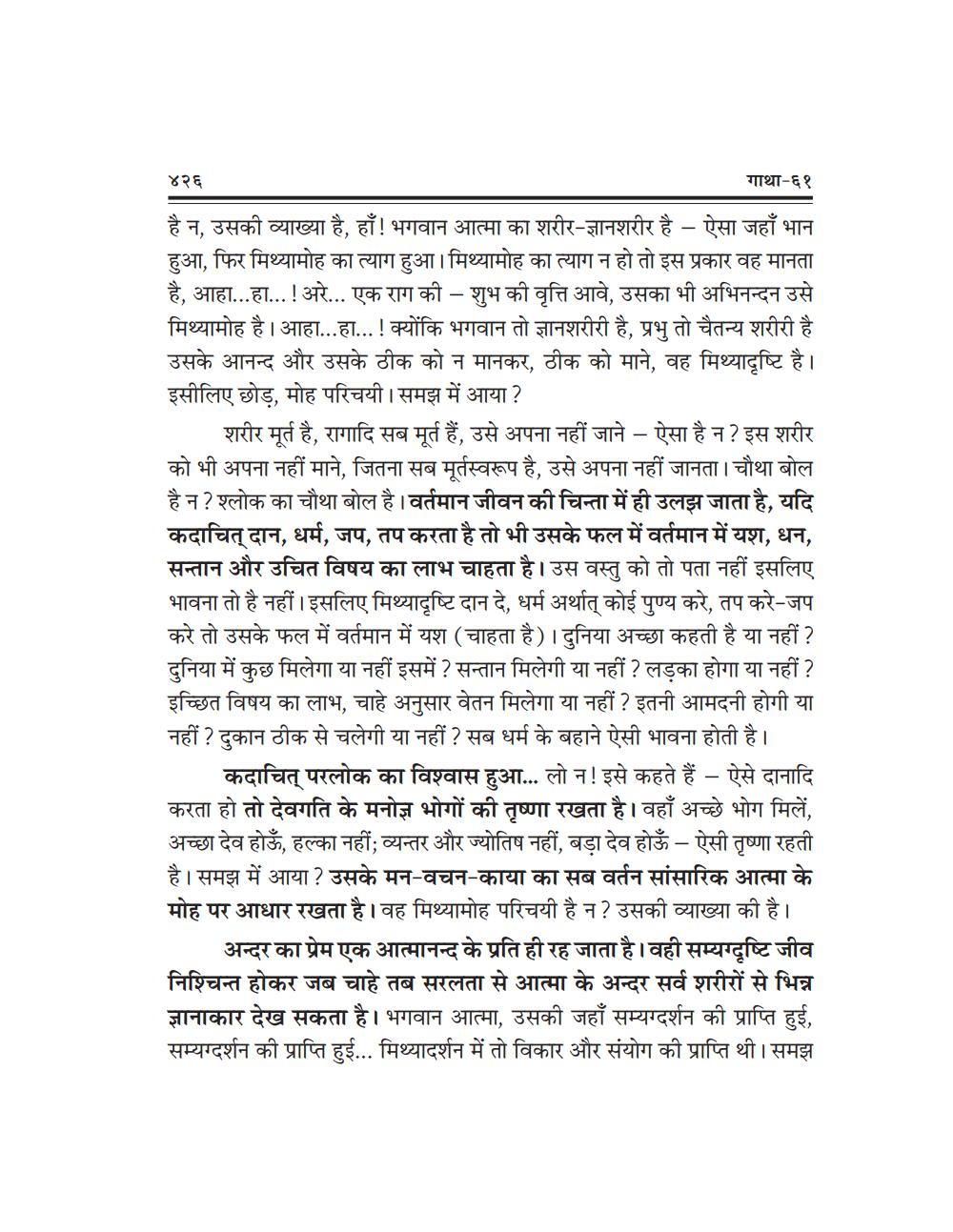________________
गाथा - ६१
४२६
हैन, उसकी व्याख्या है, हाँ ! भगवान आत्मा का शरीर - ज्ञानशरीर है ऐसा जहाँ भान हुआ, फिर मिथ्यामोह का त्याग हुआ । मिथ्यामोह का त्याग न हो तो इस प्रकार वह मानता है, आहा...हा... ! अरे... एक राग की - शुभ की वृत्ति आवे, उसका भी अभिनन्दन उसे मिथ्यामोह है । आहा...हा... ! क्योंकि भगवान तो ज्ञानशरीरी है, प्रभु तो चैतन्य शरीरी है उसके आनन्द और उसके ठीक को न मानकर, ठीक को माने, वह मिथ्यादृष्टि है । इसीलिए छोड़, मोह परिचयी । समझ में आया ?
शरीर मूर्त है, रागादि सब मूर्त हैं, उसे अपना नहीं जाने - ऐसा है न ? इस शरीर को भी अपना नहीं माने, जितना सब मूर्तस्वरूप है, उसे अपना नहीं जानता। चौथा बोल है न ? श्लोक का चौथा बोल है। वर्तमान जीवन की चिन्ता में ही उलझ जाता है, यदि कदाचित् दान, धर्म, जप, तप करता है तो भी उसके फल में वर्तमान में यश, धन, सन्तान और उचित विषय का लाभ चाहता है । उस वस्तु को तो पता नहीं इसलिए भावना तो है नहीं। इसलिए मिथ्यादृष्टि दान दे, धर्म अर्थात् कोई पुण्य करे, तप करे-जप करे तो उसके फल में वर्तमान में यश ( चाहता है)। दुनिया अच्छा कहती है या नहीं ? दुनिया में कुछ मिलेगा या नहीं इसमें ? सन्तान मिलेगी या नहीं ? लड़का होगा या नहीं ? इच्छित विषय का लाभ, चाहे अनुसार वेतन मिलेगा या नहीं ? इतनी आमदनी होगी या नहीं ? दुकान ठीक से चलेगी या नहीं? सब धर्म के बहाने ऐसी भावना होती है।
कदाचित् परलोक का विश्वास हुआ... लो न ! इसे कहते हैं - ऐसे दानादि करता हो तो देवगति के मनोज्ञ भोगों की तृष्णा रखता है । वहाँ अच्छे भोग मिलें, अच्छा देव होऊँ, हल्का नहीं; व्यन्तर और ज्योतिष नहीं, बड़ा देव होऊँ - ऐसी तृष्णा रहती है। समझ में आया? उसके मन-वचन-काया का सब वर्तन सांसारिक आत्मा के मोह पर आधार रखता है । वह मिथ्यामोह परिचयी है न ? उसकी व्याख्या की है।
अन्दर का प्रेम एक आत्मानन्द के प्रति ही रह जाता है। वही सम्यग्दृष्टि जीव निश्चिन्त होकर जब चाहे तब सरलता से आत्मा के अन्दर सर्व शरीरों से भिन्न ज्ञानाकार देख सकता है। भगवान आत्मा, उसकी जहाँ सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हुई, सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हुई... मिथ्यादर्शन में तो विकार और संयोग की प्राप्ति थी । समझ