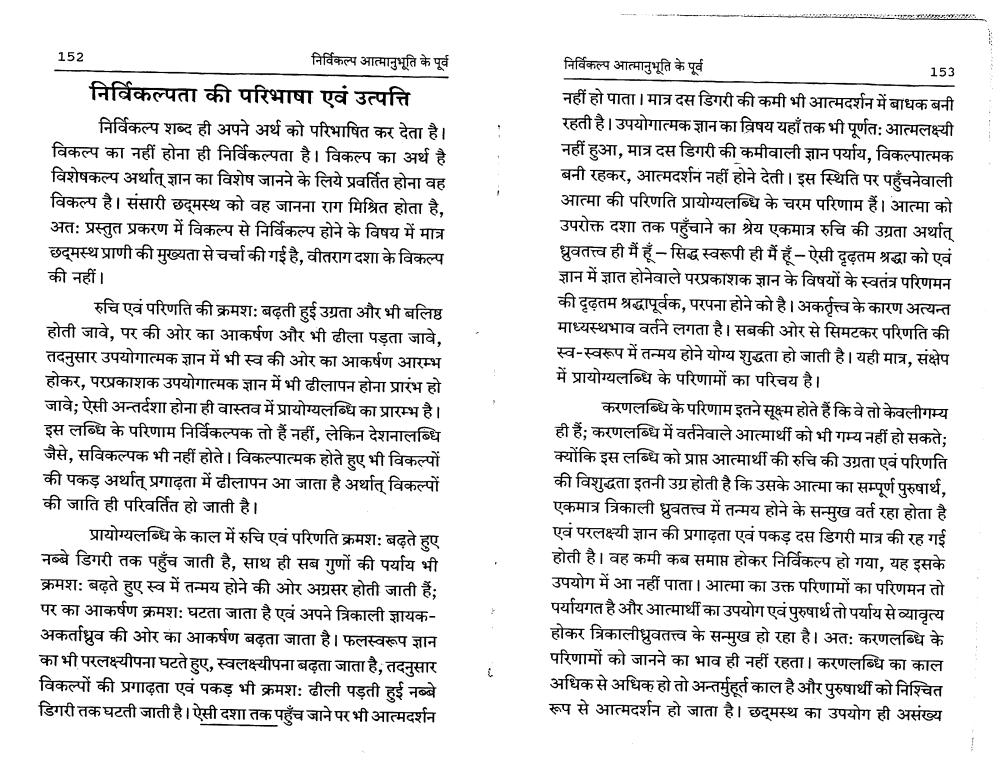________________
152
निर्विकल्प आत्मानुभूति के पूर्व निर्विकल्पता की परिभाषा एवं उत्पत्ति
निर्विकल्प शब्द ही अपने अर्थ को परिभाषित कर देता है। विकल्प का नहीं होना ही निर्विकल्पता है। विकल्प का अर्थ है विशेषकल्प अर्थात् ज्ञान का विशेष जानने के लिये प्रवर्तित होना वह विकल्प है। संसारी छद्मस्थ को वह जानना राग मिश्रित होता है, अत: प्रस्तुत प्रकरण में विकल्प से निर्विकल्प होने के विषय में मात्र छद्मस्थ प्राणी की मुख्यता से चर्चा की गई है, वीतराग दशा के विकल्प की नहीं।
रुचि एवं परिणति की क्रमश: बढ़ती हुई उग्रता और भी बलिष्ठ होती जावे, पर की ओर का आकर्षण और भी ढीला पड़ता जावे, तदनुसार उपयोगात्मक ज्ञान में भी स्व की ओर का आकर्षण आरम्भ होकर, परप्रकाशक उपयोगात्मक ज्ञान में भी ढीलापन होना प्रारंभ हो जावे; ऐसी अन्तर्दशा होना ही वास्तव में प्रायोग्यलब्धि का प्रारम्भ है। इस लब्धि के परिणाम निर्विकल्पक तो हैं नहीं, लेकिन देशनालब्धि जैसे, सविकल्पक भी नहीं होते। विकल्पात्मक होते हुए भी विकल्पों की पकड़ अर्थात् प्रगाढ़ता में ढीलापन आ जाता है अर्थात् विकल्पों की जाति ही परिवर्तित हो जाती है।
प्रायोग्यलब्धि के काल में रुचि एवं परिणति क्रमश: बढ़ते हुए नब्बे डिगरी तक पहुँच जाती है, साथ ही सब गुणों की पर्याय भी क्रमश: बढ़ते हुए स्व में तन्मय होने की ओर अग्रसर होती जाती हैं; पर का आकर्षण क्रमश: घटता जाता है एवं अपने त्रिकाली ज्ञायकअकर्ताध्रुव की ओर का आकर्षण बढ़ता जाता है। फलस्वरूप ज्ञान का भी परलक्ष्यीपना घटते हुए, स्वलक्ष्यीपना बढ़ता जाता है, तदनुसार विकल्पों की प्रगाढ़ता एवं पकड़ भी क्रमशः ढीली पड़ती हुई नब्बे डिगरी तक घटती जाती है। ऐसी दशा तक पहुँच जाने पर भी आत्मदर्शन
निर्विकल्प आत्मानुभूति के पूर्व
153 नहीं हो पाता । मात्र दस डिगरी की कमी भी आत्मदर्शन में बाधक बनी रहती है। उपयोगात्मक ज्ञान का विषय यहाँ तक भी पूर्णत: आत्मलक्ष्यी नहीं हुआ, मात्र दस डिगरी की कमीवाली ज्ञान पर्याय, विकल्पात्मक बनी रहकर, आत्मदर्शन नहीं होने देती। इस स्थिति पर पहुँचनेवाली आत्मा की परिणति प्रायोग्यलब्धि के चरम परिणाम हैं। आत्मा को उपरोक्त दशा तक पहुँचाने का श्रेय एकमात्र रुचि की उग्रता अर्थात् ध्रुवतत्त्व ही मैं हूँ-सिद्ध स्वरूपी ही मैं हूँ-ऐसी दृढ़तम श्रद्धा को एवं ज्ञान में ज्ञात होनेवाले परप्रकाशक ज्ञान के विषयों के स्वतंत्र परिणमन की दृढ़तम श्रद्धापूर्वक, परपना होने को है। अकर्तृत्त्व के कारण अत्यन्त माध्यस्थभाव वर्तने लगता है। सबकी ओर से सिमटकर परिणति की स्व-स्वरूप में तन्मय होने योग्य शुद्धता हो जाती है। यही मात्र, संक्षेप में प्रायोग्यलब्धि के परिणामों का परिचय है।
करणलब्धि के परिणाम इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे तो केवलीगम्य ही हैं; करणलब्धि में वर्तनेवाले आत्मार्थी को भी गम्य नहीं हो सकते; क्योंकि इस लब्धि को प्राप्त आत्मार्थी की रुचि की उग्रता एवं परिणति की विशुद्धता इतनी उग्र होती है कि उसके आत्मा का सम्पूर्ण पुरुषार्थ, एकमात्र त्रिकाली ध्रुवतत्त्व में तन्मय होने के सन्मुख वर्त रहा होता है एवं परलक्ष्यी ज्ञान की प्रगाढ़ता एवं पकड़ दस डिगरी मात्र की रह गई होती है। वह कमी कब समाप्त होकर निर्विकल्प हो गया, यह इसके उपयोग में आ नहीं पाता। आत्मा का उक्त परिणामों का परिणमन तो पर्यायगत है और आत्मार्थी का उपयोग एवं पुरुषार्थ तो पर्याय से व्यावृत्य होकर त्रिकालीध्रुवतत्त्व के सन्मुख हो रहा है। अत: करणलब्धि के परिणामों को जानने का भाव ही नहीं रहता। करणलब्धि का काल अधिक से अधिक हो तो अन्तर्मुहूर्त काल है और पुरुषार्थी को निश्चित रूप से आत्मदर्शन हो जाता है। छद्मस्थ का उपयोग ही असंख्य