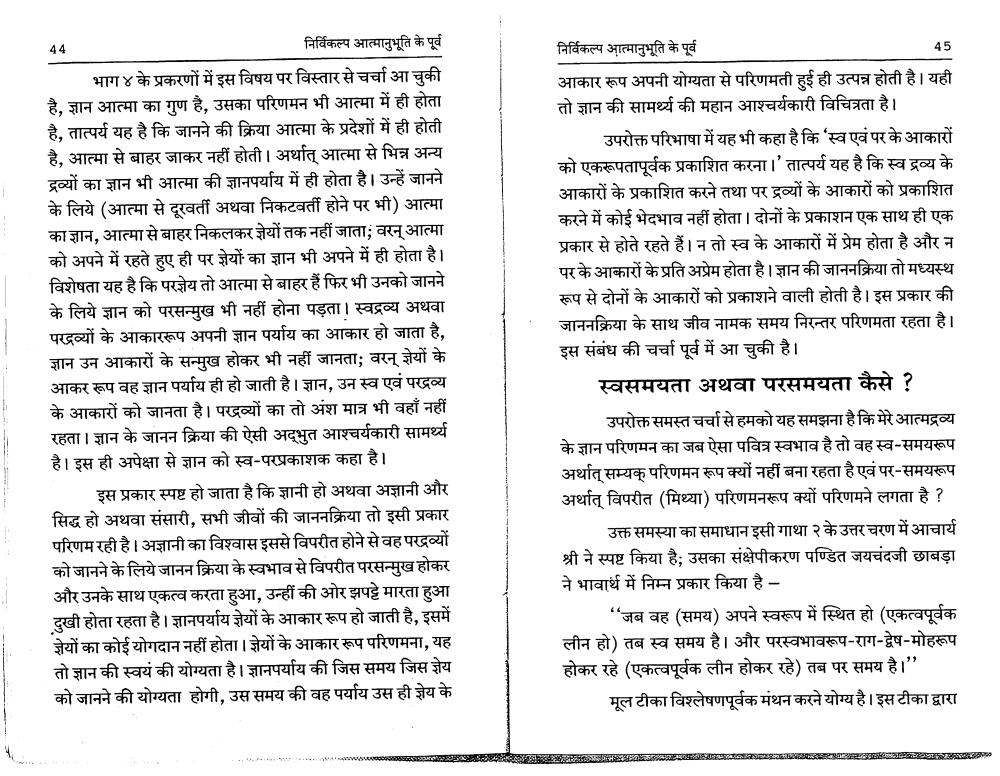________________
निर्विकल्प आत्मानुभूति के पूर्व भाग ४ के प्रकरणों में इस विषय पर विस्तार से चर्चा आ चुकी है, ज्ञान आत्मा का गुण है, उसका परिणमन भी आत्मा में ही होता है, तात्पर्य यह है कि जानने की क्रिया आत्मा के प्रदेशों में ही होती है, आत्मा से बाहर जाकर नहीं होती। अर्थात् आत्मा से भिन्न अन्य द्रव्यों का ज्ञान भी आत्मा की ज्ञानपर्याय में ही होता है। उन्हें जानने के लिये (आत्मा से दूरवर्ती अथवा निकटवर्ती होने पर भी) आत्मा का ज्ञान, आत्मा से बाहर निकलकर ज्ञेयों तक नहीं जाता; वरन् आत्मा को अपने में रहते हुए ही पर ज्ञेयों का ज्ञान भी अपने में ही होता है। विशेषता यह है कि परज्ञेय तो आत्मा से बाहर हैं फिर भी उनको जानने के लिये ज्ञान को परसन्मुख भी नहीं होना पड़ता। स्वद्रव्य अथवा परद्रव्यों के आकाररूप अपनी ज्ञान पर्याय का आकार हो जाता है, ज्ञान उन आकारों के सन्मुख होकर भी नहीं जानता; वरन् ज्ञेयों के आकर रूप वह ज्ञान पर्याय ही हो जाती है। ज्ञान, उन स्व एवं परद्रव्य के आकारों को जानता है। परद्रव्यों का तो अंश मात्र भी वहाँ नहीं रहता। ज्ञान के जानन क्रिया की ऐसी अद्भुत आश्चर्यकारी सामर्थ्य है। इस ही अपेक्षा से ज्ञान को स्व-परप्रकाशक कहा है।
इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी और सिद्ध हो अथवा संसारी, सभी जीवों की जाननक्रिया तो इसी प्रकार परिणम रही है। अज्ञानी का विश्वास इससे विपरीत होने से वह परद्रव्यों को जानने के लिये जानन क्रिया के स्वभाव से विपरीत परसन्मुख होकर
और उनके साथ एकत्व करता हुआ, उन्हीं की ओर झपट्टे मारता हुआ दुखी होता रहता है। ज्ञानपर्याय ज्ञेयों के आकार रूप हो जाती है, इसमें ज्ञेयों का कोई योगदान नहीं होता। ज्ञेयों के आकार रूप परिणमना, यह तो ज्ञान की स्वयं की योग्यता है। ज्ञानपर्याय की जिस समय जिस ज्ञेय को जानने की योग्यता होगी, उस समय की वह पर्याय उस ही ज्ञेय के
निर्विकल्प आत्मानुभूति के पूर्व
45 आकार रूप अपनी योग्यता से परिणमती हुई ही उत्पन्न होती है। यही तो ज्ञान की सामर्थ्य की महान आश्चर्यकारी विचित्रता है।
उपरोक्त परिभाषा में यह भी कहा है कि 'स्व एवं पर के आकारों को एकरूपतापूर्वक प्रकाशित करना।' तात्पर्य यह है कि स्व द्रव्य के आकारों के प्रकाशित करने तथा पर द्रव्यों के आकारों को प्रकाशित करने में कोई भेदभाव नहीं होता। दोनों के प्रकाशन एक साथ ही एक प्रकार से होते रहते हैं। न तो स्व के आकारों में प्रेम होता है और न पर के आकारों के प्रति अप्रेम होता है। ज्ञान की जाननक्रिया तो मध्यस्थ रूप से दोनों के आकारों को प्रकाशने वाली होती है। इस प्रकार की जाननक्रिया के साथ जीव नामक समय निरन्तर परिणमता रहता है। इस संबंध की चर्चा पूर्व में आ चुकी है।
स्वसमयता अथवा परसमयता कैसे ?
उपरोक्त समस्त चर्चा से हमको यह समझना है कि मेरे आत्मद्रव्य के ज्ञान परिणमन का जब ऐसा पवित्र स्वभाव है तो वह स्व-समयरूप अर्थात् सम्यक् परिणमन रूप क्यों नहीं बना रहता है एवं पर-समयरूप अर्थात् विपरीत (मिथ्या) परिणमनरूप क्यों परिणमने लगता है ?
उक्त समस्या का समाधान इसी गाथा २ के उत्तर चरण में आचार्य श्री ने स्पष्ट किया है; उसका संक्षेपीकरण पण्डित जयचंदजी छाबड़ा ने भावार्थ में निम्न प्रकार किया है -
"जब वह (समय) अपने स्वरूप में स्थित हो (एकत्वपूर्वक लीन हो) तब स्व समय है। और परस्वभावरूप-राग-द्वेष-मोहरूप होकर रहे (एकत्वपूर्वक लीन होकर रहे) तब पर समय है।"
मूल टीका विश्लेषणपूर्वक मंथन करने योग्य है। इस टीका द्वारा