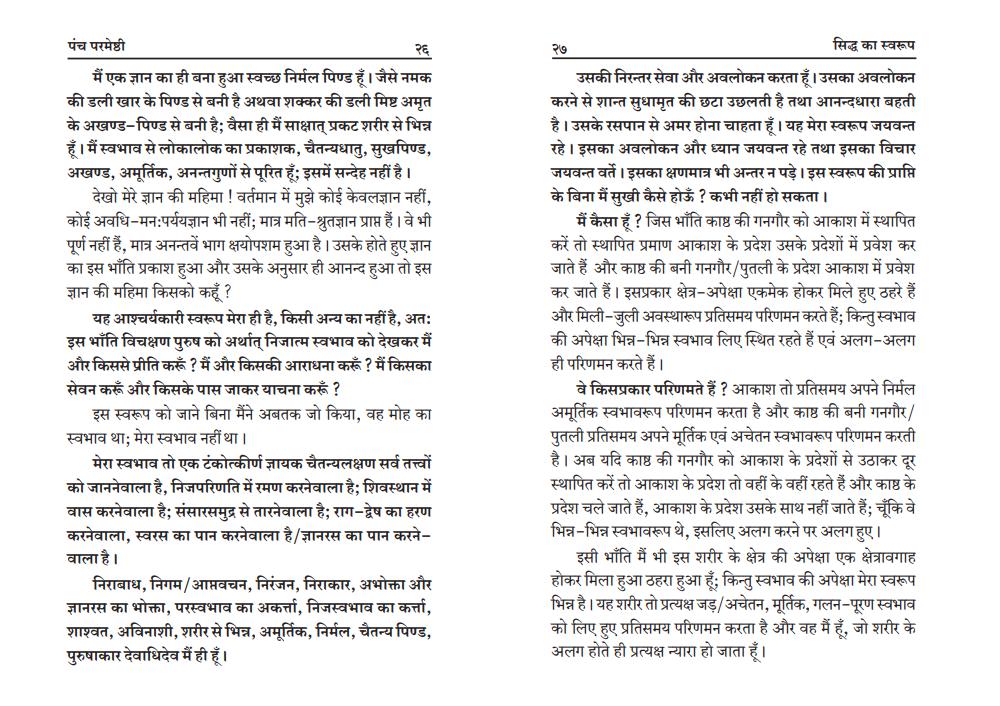________________
७
पंच परमेष्ठी ____मैं एक ज्ञान का ही बना हुआ स्वच्छ निर्मल पिण्ड हूँ। जैसे नमक की डली खार के पिण्ड से बनी है अथवा शक्कर की डली मिष्ट अमृत के अखण्ड-पिण्ड से बनी है; वैसा ही मैं साक्षात् प्रकट शरीर से भिन्न हूँ। मैं स्वभाव से लोकालोक का प्रकाशक, चैतन्यधातु, सुखपिण्ड, अखण्ड, अमूर्तिक, अनन्तगुणों से पूरित हूँ; इसमें सन्देह नहीं है।
देखो मेरे ज्ञान की महिमा ! वर्तमान में मुझे कोई केवलज्ञान नहीं, कोई अवधि-मन:पर्ययज्ञान भी नहीं; मात्र मति-श्रुतज्ञान प्राप्त हैं । वे भी पूर्ण नहीं हैं, मात्र अनन्तवें भाग क्षयोपशम हुआ है। उसके होते हुए ज्ञान का इस भाँति प्रकाश हुआ और उसके अनुसार ही आनन्द हुआ तो इस ज्ञान की महिमा किसको कहूँ? ___यह आश्चर्यकारी स्वरूप मेरा ही है, किसी अन्य का नहीं है, अत: इस भाँति विचक्षण पुरुष को अर्थात् निजात्म स्वभाव को देखकर मैं
और किससे प्रीति करूँ? मैं और किसकी आराधना करूँ? मैं किसका सेवन करूँ और किसके पास जाकर याचना करूँ?
इस स्वरूप को जाने बिना मैंने अबतक जो किया, वह मोह का स्वभाव था; मेरा स्वभाव नहीं था।
मेरा स्वभाव तो एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक चैतन्यलक्षण सर्व तत्त्वों को जाननेवाला है, निजपरिणति में रमण करनेवाला है; शिवस्थान में वास करनेवाला है; संसारसमुद्र से तारनेवाला है; राग-द्वेष का हरण करनेवाला, स्वरस का पान करनेवाला है/ज्ञानरस का पान करनेवाला है।
निराबाध, निगम/आप्तवचन, निरंजन, निराकार, अभोक्ता और ज्ञानरस का भोक्ता, परस्वभाव का अकर्ता, निजस्वभाव का कर्ता, शाश्वत, अविनाशी, शरीर से भिन्न, अमूर्तिक, निर्मल, चैतन्य पिण्ड, पुरुषाकार देवाधिदेव मैं ही हूँ।
सिद्ध का स्वरूप उसकी निरन्तर सेवा और अवलोकन करता हूँ। उसका अवलोकन करने से शान्त सुधामृत की छटा उछलती है तथा आनन्दधारा बहती है। उसके रसपान से अमर होना चाहता हूँ । यह मेरा स्वरूप जयवन्त रहे । इसका अवलोकन और ध्यान जयवन्त रहे तथा इसका विचार जयवन्त वर्ते । इसका क्षणमात्र भी अन्तर न पड़े। इस स्वरूप की प्राप्ति के बिना मैं सुखी कैसे होऊँ ? कभी नहीं हो सकता। ___ मैं कैसा हूँ ? जिस भाँति काष्ठ की गनगौर को आकाश में स्थापित करें तो स्थापित प्रमाण आकाश के प्रदेश उसके प्रदेशों में प्रवेश कर जाते हैं और काष्ठ की बनी गनगौर/पुतली के प्रदेश आकाश में प्रवेश कर जाते हैं। इसप्रकार क्षेत्र-अपेक्षा एकमेक होकर मिले हुए ठहरे हैं
और मिली-जुली अवस्थारूप प्रतिसमय परिणमन करते हैं; किन्तु स्वभाव की अपेक्षा भिन्न-भिन्न स्वभाव लिए स्थित रहते हैं एवं अलग-अलग ही परिणमन करते हैं।
वे किसप्रकार परिणमते हैं ? आकाश तो प्रतिसमय अपने निर्मल अमूर्तिक स्वभावरूप परिणमन करता है और काष्ठ की बनी गनगौर/ पुतली प्रतिसमय अपने मूर्तिक एवं अचेतन स्वभावरूप परिणमन करती है। अब यदि काष्ठ की गनगौर को आकाश के प्रदेशों से उठाकर दूर स्थापित करें तो आकाश के प्रदेश तो वहीं के वहीं रहते हैं और काष्ठ के प्रदेश चले जाते हैं, आकाश के प्रदेश उसके साथ नहीं जाते हैं; चूँकि वे भिन्न-भिन्न स्वभावरूप थे, इसलिए अलग करने पर अलग हुए।
इसी भाँति मैं भी इस शरीर के क्षेत्र की अपेक्षा एक क्षेत्रावगाह होकर मिला हुआ ठहरा हुआ हूँ; किन्तु स्वभाव की अपेक्षा मेरा स्वरूप भिन्न है। यह शरीर तो प्रत्यक्ष जड़/अचेतन, मूर्तिक, गलन-पूरण स्वभाव को लिए हुए प्रतिसमय परिणमन करता है और वह मैं हूँ, जो शरीर के अलग होते ही प्रत्यक्ष न्यारा हो जाता हूँ।