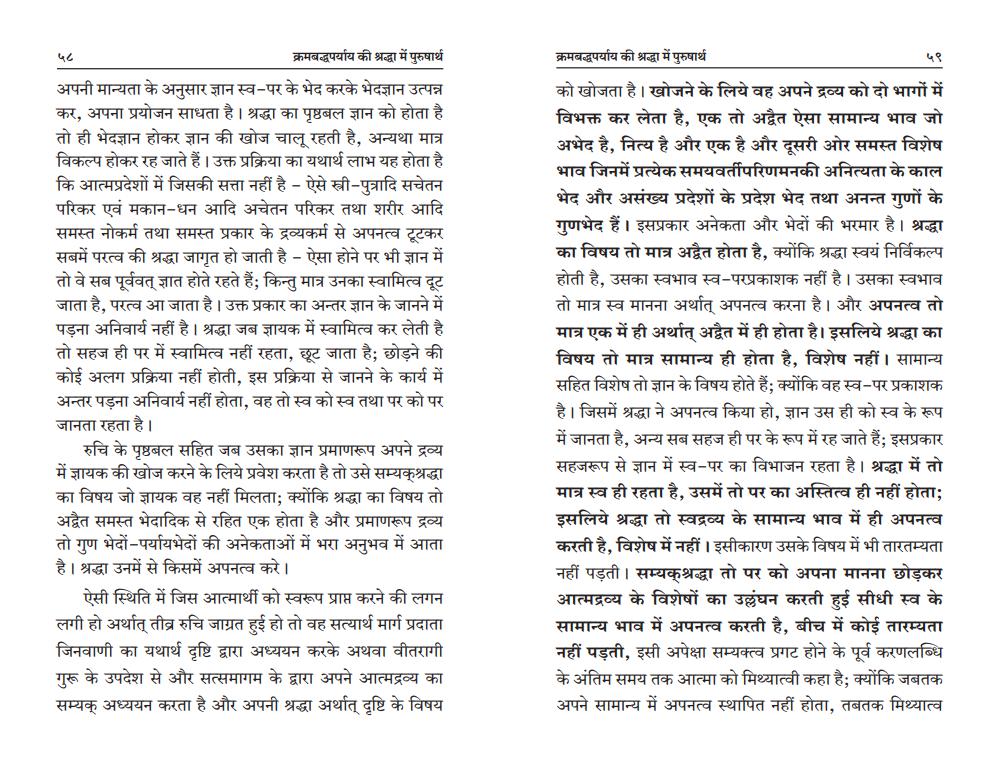________________
५८
क्रमबद्धपर्याय की श्रद्धा में पुरुषार्थ
अपनी मान्यता के अनुसार ज्ञान स्व-पर के भेद करके भेदज्ञान उत्पन्न कर, अपना प्रयोजन साधता है। श्रद्धा का पृष्ठबल ज्ञान को होता है। तो ही भेदज्ञान होकर ज्ञान की खोज चालू रहती है, अन्यथा मात्र विकल्प होकर रह जाते हैं। उक्त प्रक्रिया का यथार्थ लाभ यह होता है कि आत्मप्रदेशों में जिसकी सत्ता नहीं है - ऐसे स्त्री- पुत्रादि सचेतन परिकर एवं मकान-धन आदि अचेतन परिकर तथा शरीर आदि समस्त नोकर्म तथा समस्त प्रकार के द्रव्यकर्म से अपनत्व टूटकर सबमें परत्व की श्रद्धा जागृत हो जाती है - ऐसा होने पर भी ज्ञान में तो वे सब पूर्ववत् ज्ञात होते रहते हैं; किन्तु मात्र उनका स्वामित्व दूट जाता है, परत्व आ जाता है। उक्त प्रकार का अन्तर ज्ञान के जानने में पड़ना अनिवार्य नहीं है। श्रद्धा जब ज्ञायक में स्वामित्व कर लेती है तो सहज ही पर में स्वामित्व नहीं रहता, छूट जाता है; छोड़ने की कोई अलग प्रक्रिया नहीं होती, इस प्रक्रिया से जानने के कार्य में अन्तर पड़ना अनिवार्य नहीं होता, वह तो स्व को स्व तथा पर को पर जानता रहता है।
रुचि के पृष्ठबल सहित जब उसका ज्ञान प्रमाणरूप अपने द्रव्य में ज्ञायक की खोज करने के लिये प्रवेश करता है तो उसे सम्यक् श्रद्धा का विषय जो ज्ञायक वह नहीं मिलता; क्योंकि श्रद्धा का विषय तो अद्वैत समस्त भेदादिक से रहित एक होता है और प्रमाणरूप द्रव्य तो गुणभेदों-पर्यायभेदों की अनेकताओं में भरा अनुभव में आता है। श्रद्धा उनमें से किसमें अपनत्व करे।
ऐसी स्थिति में जिस आत्मार्थी को स्वरूप प्राप्त करने की लगन लगी हो अर्थात् तीव्र रुचि जाग्रत हुई हो तो वह सत्यार्थ मार्ग प्रदाता जिनवाणी का यथार्थ दृष्टि द्वारा अध्ययन करके अथवा वीतरागी गुरू के उपदेश से और सत्समागम के द्वारा अपने आत्मद्रव्य का सम्यक् अध्ययन करता है और अपनी श्रद्धा अर्थात् दृष्टि के विषय
क्रमबद्धपर्याय की श्रद्धा में पुरुषार्थ
५९
को खोजता है । खोजने के लिये वह अपने द्रव्य को दो भागों में विभक्त कर लेता है, एक तो अद्वैत ऐसा सामान्य भाव जो अभेद है, नित्य है और एक है और दूसरी ओर समस्त विशेष भाव जिनमें प्रत्येक समयवर्तीपरिणमनकी अनित्यता के काल भेद और असंख्य प्रदेशों के प्रदेश भेद तथा अनन्त गुणों के गुणभेद हैं। इसप्रकार अनेकता और भेदों की भरमार है। श्रद्धा का विषय तो मात्र अद्वैत होता है, क्योंकि श्रद्धा स्वयं निर्विकल्प होती है, उसका स्वभाव स्व-परप्रकाशक नहीं है। उसका स्वभाव तो मात्र स्व मानना अर्थात् अपनत्व करना है । और अपनत्व तो मात्र एक में ही अर्थात् अद्वैत में ही होता है। इसलिये श्रद्धा का विषय तो मात्र सामान्य ही होता है, विशेष नहीं । सामान्य सहित विशेष तो ज्ञान के विषय होते हैं; क्योंकि वह स्व पर प्रकाशक है। जिसमें श्रद्धा ने अपनत्व किया हो, ज्ञान उस ही को स्व के रूप में जानता है. अन्य सब सहज ही पर के रूप में रह जाते हैं; इसप्रकार सहजरूप से ज्ञान में स्व-पर का विभाजन रहता है। श्रद्धा में तो मात्र स्व ही रहता है, उसमें तो पर का अस्तित्व ही नहीं होता; इसलिये श्रद्धा तो स्वद्रव्य के सामान्य भाव में ही अपनत्व करती है, विशेष में नहीं। इसीकारण उसके विषय में भी तारतम्यता नहीं पड़ती। सम्यक् श्रद्धा तो पर को अपना मानना छोड़कर आत्मद्रव्य के विशेषों का उल्लंघन करती हुई सीधी स्व के सामान्य भाव में अपनत्व करती है, बीच में कोई तारम्यता नहीं पड़ती, इसी अपेक्षा सम्यक्त्व प्रगट होने के पूर्व करणलब्धि के अंतिम समय तक आत्मा को मिथ्यात्वी कहा है; क्योंकि जबतक अपने सामान्य में अपनत्व स्थापित नहीं होता, तबतक मिथ्यात्व