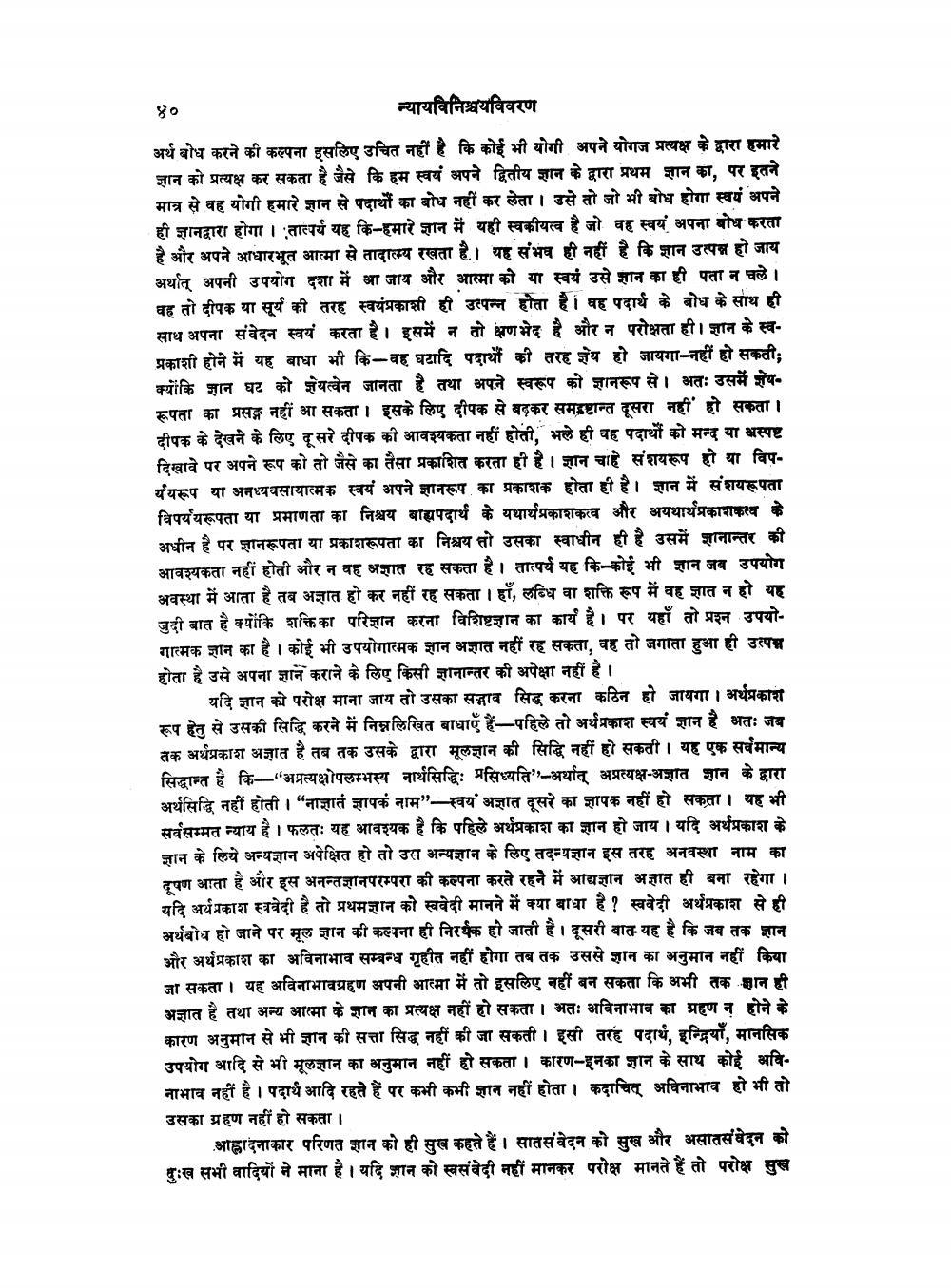________________
न्यायविनिश्चयविवरण
अर्थ बोध करने की कल्पना इसलिए उचित नहीं है कि कोई भी योगी अपने योगज प्रत्यक्ष के द्वारा हमारे ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकता है जैसे कि हम स्वयं अपने द्वितीय ज्ञान के द्वारा प्रथम ज्ञान का, पर इतने मात्र से वह योगी हमारे ज्ञान से पदार्थों का बोध नहीं कर लेता। उसे तो जो भी बोध होगा स्वयं अपने ही ज्ञानद्वारा होगा। तात्पर्य यह कि-हमारे ज्ञान में यही स्वकीयत्व है जो वह स्वयं अपना बोध करता है और अपने आधारभूत आत्मा से तादात्म्य रखता है। यह संभव ही नहीं है कि ज्ञान उत्पन्न हो जाय अर्थात् अपनी उपयोग दशा में आ जाय और आत्मा को या स्वयं उसे ज्ञान का ही पता न चले। वह तो दीपक या सूर्य की तरह स्वयंप्रकाशी ही उत्पन्न होता है। वह पदार्थ के बोध के साथ ही साथ अपना संवेदन स्वयं करता है। इसमें न तो क्षणभेद है और न परोक्षता ही। ज्ञान के स्वप्रकाशी होने में यह बाधा भी कि-वह घटादि पदार्थों की तरह ज्ञेय हो जायगा-नहीं हो सकती%B क्योंकि ज्ञान घट को ज्ञेयत्वेन जानता है तथा अपने स्वरूप को ज्ञानरूप से। अतः उसमें ज्ञेय. रूपता का प्रसङ्ग नहीं आ सकता। इसके लिए दीपक से बढ़कर समदृष्टान्त दूसरा नहीं हो सकता। दीपक के देखने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती, भले ही वह पदार्थों को मन्द या अस्पष्ट दिखावे पर अपने रूप को तो जैसे का तैसा प्रकाशित करता ही है। ज्ञान चाहे संशयरूप हो या विपर्य यरूप या अनध्यवसायात्मक स्वयं अपने ज्ञानरूप का प्रकाशक होता ही है। ज्ञान में संशयरूपता विपर्ययरूपता या प्रमाणता का निश्चय बाह्यपदार्थ के यथार्थप्रकाशकत्व और अयथार्थप्रकाशकत्व के अधीन है पर ज्ञानरूपता या प्रकाशरूपता का निश्चय तो उसका स्वाधीन ही है उसमें ज्ञानान्तर की आवश्यकता नहीं होती और न वह अज्ञात रह सकता है। तात्पर्य यह कि कोई भी ज्ञान जब उपयोग अवस्था में आता है तब अज्ञात हो कर नहीं रह सकता। हाँ, लब्धि वा शक्ति रूप में वह ज्ञात न हो यह जुदी बात है क्योंकि शक्ति का परिज्ञान करना विशिष्टज्ञान का कार्य है। पर यहाँ तो प्रश्न उपयोगात्मक ज्ञान का है। कोई भी उपयोगात्मक ज्ञान अज्ञात नहीं रह सकता, वह तो जगाता हुआ ही उत्पा होता है उसे अपना ज्ञान कराने के लिए किसी ज्ञानान्तर की अपेक्षा नहीं है।
यदि ज्ञान को परोक्ष माना जाय तो उसका सद्भाव सिद्ध करना कठिन हो जायगा । अर्थप्रकाश रूप हेतु से उसकी सिद्धि करने में निम्नलिखित बाधाएँ हैं–पहिले तो अर्थप्रकाश स्वयं ज्ञान है अतः जब तक अर्थप्रकाश अज्ञात है तब तक उसके द्वारा मूलज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती। यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि-"अप्रत्यक्षोपलम्भस्य नार्थसिद्धिः प्रसिध्यति'' अर्थात् अप्रत्यक्ष-अज्ञात ज्ञान के द्वारा अर्थसिद्धि नहीं होती । “नाज्ञातं ज्ञापकं नाम"-स्वयं अज्ञात दूसरे का ज्ञापक नहीं हो सकता। यह भी सर्वसम्मत न्याय है । फलतः यह आवश्यक है कि पहिले अर्थप्रकाश का ज्ञान हो जाय । यदि अर्थप्रकाश के ज्ञान के लिये अन्यज्ञान अपेक्षित हो तो उरा अन्यज्ञान के लिए तदन्यज्ञान इस तरह अनवस्था नाम का दृषण आता है और इस अनन्तज्ञानपरम्परा की कल्पना करते रहने में आद्यज्ञान अज्ञात ही बना रहेगा। यदि अर्थप्रकाश स्ववेदी है तो प्रथमज्ञान को स्ववेदी मानने में क्या बाधा है? स्ववेदी अर्थप्रकाश से ही अर्थबोध हो जाने पर मूल ज्ञान की कल्पना ही निरर्थक हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जब तक ज्ञान और अर्थप्रकाश का अविनाभाव सम्बन्ध गृहीत नहीं होगा तब तक उससे ज्ञान का अनुमान नहीं किया जा सकता। यह अविनाभावग्रहण अपनी आत्मा में तो इसलिए नहीं बन सकता कि अभी तक ज्ञान ही अज्ञात है तथा अन्य आत्मा के ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। अतः अविनाभाव का ग्रहण न होने के कारण अनुमान से भी ज्ञान की सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती। इसी तरह पदार्थ, इन्द्रियाँ, मानसिक उपयोग आदि से भी मूलज्ञान का अनुमान नहीं हो सकता । कारण-इनका ज्ञान के साथ कोई अविनाभाव नहीं है । पदार्थ आदि रहते हैं पर कभी कभी ज्ञान नहीं होता। कदाचित् अविनाभाव हो भी तो उसका ग्रहण नहीं हो सकता।
आह्लादनाकार परिणत ज्ञान को ही सुख कहते हैं। सातसंवेदन को सुख और असातसंवेदन को दुःख सभी वादियों ने माना है। यदि ज्ञान को स्वसंवेदी नहीं मानकर परोक्ष मानते हैं तो परोक्ष सुख