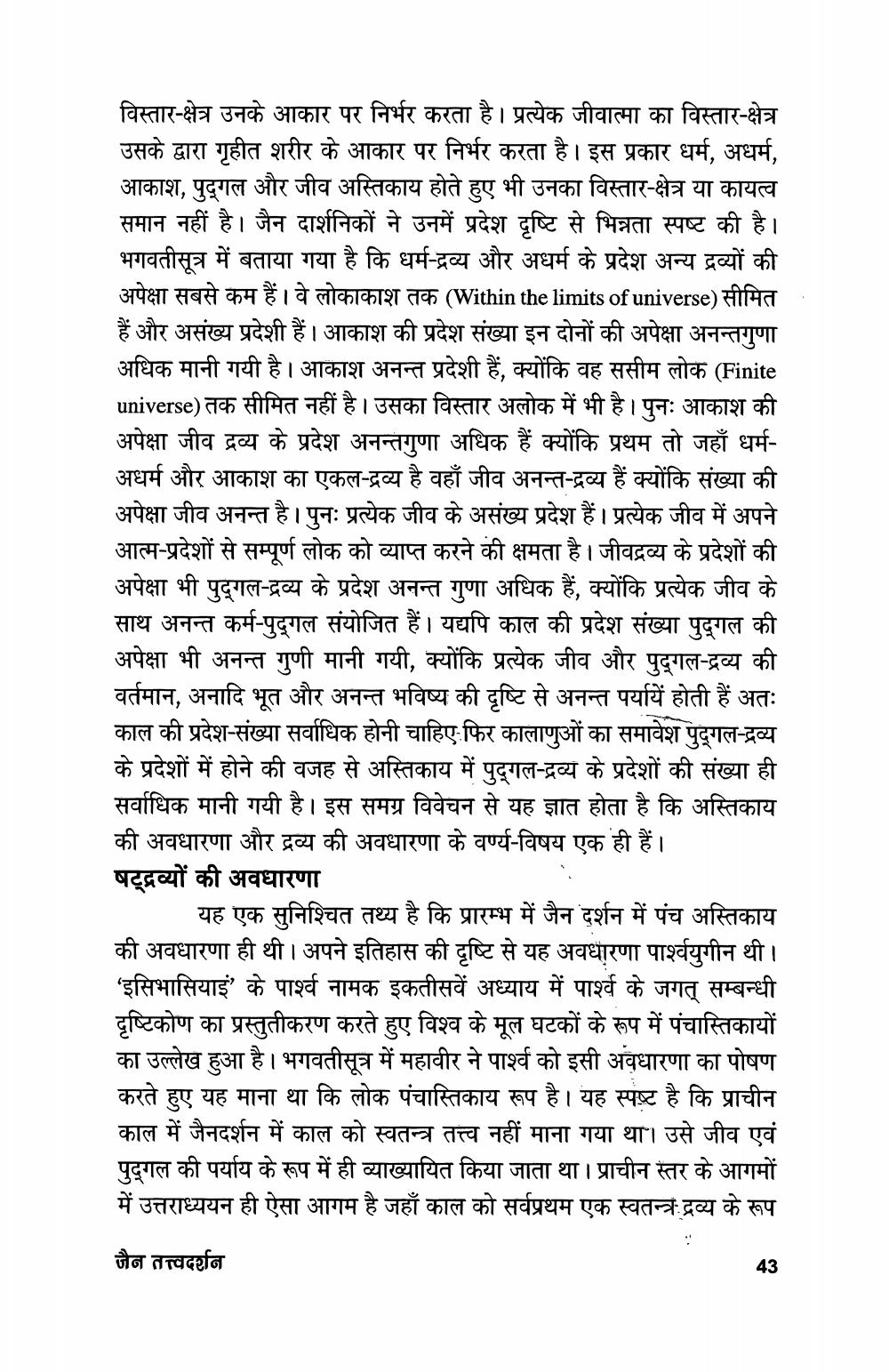________________
1
विस्तार क्षेत्र उनके आकार पर निर्भर करता है । प्रत्येक जीवात्मा का विस्तार - क्षेत्र उसके द्वारा गृहीत शरीर के आकार पर निर्भर करता है । इस प्रकार धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव अस्तिकाय होते हुए भी उनका विस्तार - क्षेत्र या काव समान नहीं है। जैन दार्शनिकों ने उनमें प्रदेश दृष्टि से भिन्नता स्पष्ट की है भगवतीसूत्र में बताया गया है कि धर्म-द्रव्य और अधर्म के प्रदेश अन्य द्रव्यों की अपेक्षा सबसे कम हैं। वे लोकाकाश तक (Within the limits of universe) सीमित हैं और असंख्य प्रदेशी हैं । आकाश की प्रदेश संख्या इन दोनों की अपेक्षा अनन्तगुणा अधिक मानी गयी है। आकाश अनन्त प्रदेशी हैं, क्योंकि वह ससीम लोक (Finite universe) तक सीमित नहीं है । उसका विस्तार अलोक में भी है । पुनः आकाश की अपेक्षा जीव द्रव्य के प्रदेश अनन्तगुणा अधिक हैं क्योंकि प्रथम तो जहाँ धर्मअधर्म और आकाश का एकल- द्रव्य है वहाँ जीव अनन्त - द्रव्य हैं क्योंकि संख्या की अपेक्षा जीव अनन्त है। पुनः प्रत्येक जीव के असंख्य प्रदेश हैं । प्रत्येक जीव में अपने आत्म-प्रदेशों से सम्पूर्ण लोक को व्याप्त करने की क्षमता है । जीवद्रव्य के प्रदेशों की अपेक्षा भी पुद्गल - द्रव्य के प्रदेश अनन्त गुणा अधिक हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव के साथ अनन्त कर्म-पुद्गल संयोजित हैं । यद्यपि काल की प्रदेश संख्या पुद्गल की अपेक्षा भी अनन्त गुणी मानी गयी, क्योंकि प्रत्येक जीव और पुद्गल - द्रव्य की वर्तमान, अनादि भूत और अनन्त भविष्य की दृष्टि से अनन्त पर्यायें होती हैं अतः काल की प्रदेश-संख्या सर्वाधिक होनी चाहिए- फिर कालाणुओं का समावेश पुद्गल-द्रव्य के प्रदेशों में होने की वजह से अस्तिकाय में पुद्गल - द्रव्य के प्रदेशों की संख्या ही सर्वाधिक मानी गयी है । इस समग्र विवेचन से यह ज्ञात होता है कि अस्तिकाय की अवधारणा और द्रव्य की अवधारणा के वर्ण्य विषय एक ही हैं । षट्द्रव्यों की अवधारणा
यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि प्रारम्भ में जैन दर्शन में पंच अस्तिकाय की अवधारणा ही थी। अपने इतिहास की दृष्टि से यह अवधारणा पार्श्वयुगीन थी । 'इसिभासियाई' के पार्श्व नामक इकतीसवें अध्याय में पार्श्व के जगत् सम्बन्धी दृष्टिकोण का प्रस्तुतीकरण करते हुए विश्व के मूल घटकों के रूप में पंचास्तिकायों का उल्लेख हुआ है। भगवतीसूत्र में महावीर ने पार्श्व को इसी अवधारणा का पोषण करते हुए यह माना था कि लोक पंचास्तिकाय रूप है । यह स्पष्ट है कि प्राचीन काल में जैनदर्शन में काल को स्वतन्त्र तत्त्व नहीं माना गया था । उसे जीव एवं पुद्गल की पर्याय के रूप में ही व्याख्यायित किया जाता था । प्राचीन स्तर के आगमों में उत्तराध्ययन ही ऐसा आगम है जहाँ काल को सर्वप्रथम एक स्वतन्त्र द्रव्य के रूप जैन तत्त्वदर्शन
"
43