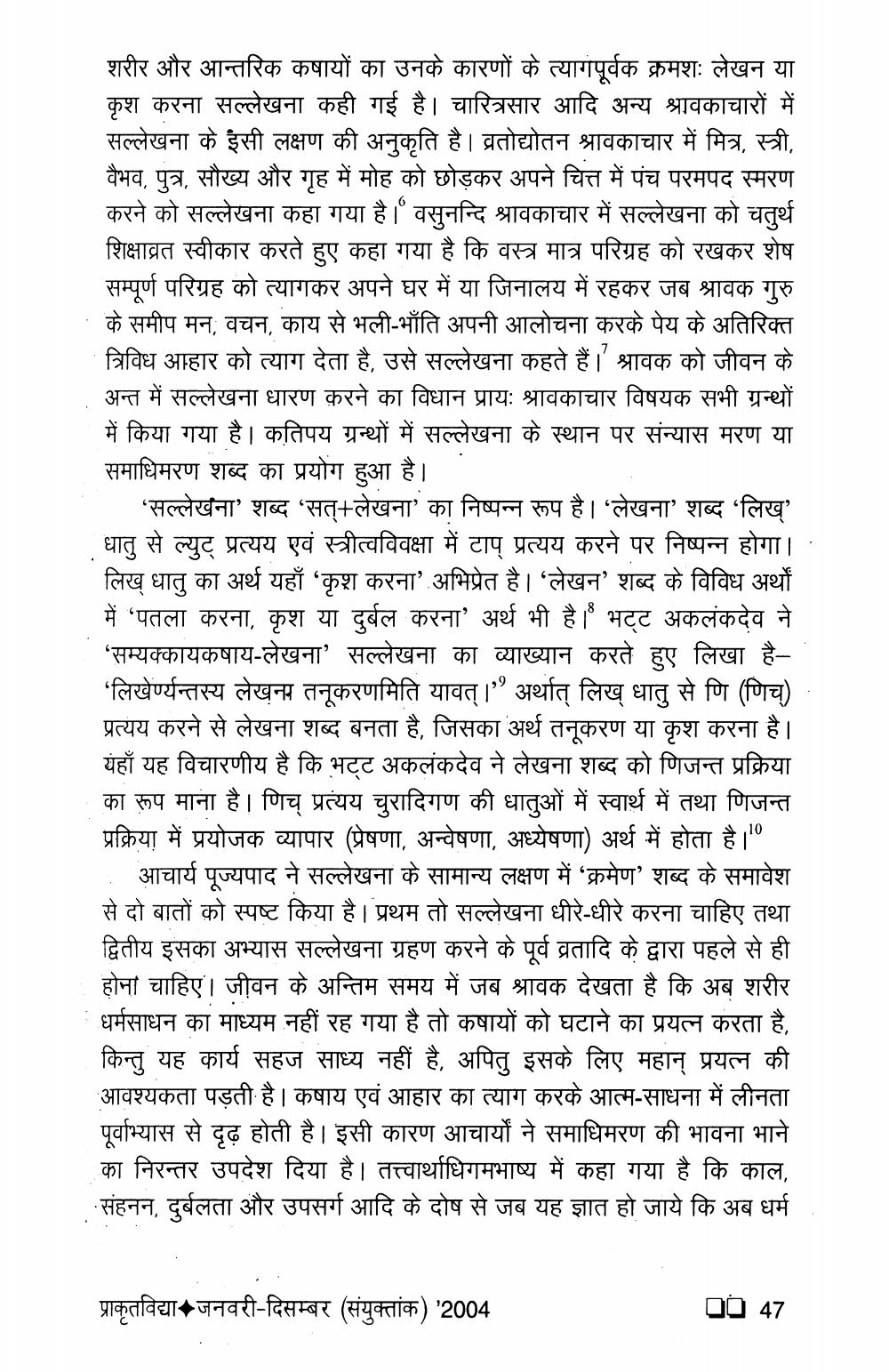________________ शरीर और आन्तरिक कषायों का उनके कारणों के त्यागपूर्वक क्रमशः लेखन या कृश करना सल्लेखना कही गई है। चारित्रसार आदि अन्य श्रावकाचारों में सल्लेखना के इसी लक्षण की अनुकृति है। व्रतोद्योतन श्रावकाचार में मित्र, स्त्री, वैभव, पुत्र, सौख्य और गृह में मोह को छोड़कर अपने चित्त में पंच परमपद स्मरण करने को सल्लेखना कहा गया है। वसुनन्दि श्रावकाचार में सल्लेखना को चतुर्थ शिक्षाव्रत स्वीकार करते हुए कहा गया है कि वस्त्र मात्र परिग्रह को रखकर शेष सम्पूर्ण परिग्रह को त्यागकर अपने घर में या जिनालय में रहकर जब श्रावक गुरु के समीप मन, वचन, काय से भली-भाँति अपनी आलोचना करके पेय के अतिरिक्त त्रिविध आहार को त्याग देता है, उसे सल्लेखना कहते हैं। श्रावक को जीवन के अन्त में सल्लेखना धारण करने का विधान प्रायः श्रावकाचार विषयक सभी ग्रन्थों में किया गया है। कतिपय ग्रन्थों में सल्लेखना के स्थान पर संन्यास मरण या समाधिमरण शब्द का प्रयोग हुआ है। _ 'सल्लेखना' शब्द 'सत्+लेखना' का निष्पन्न रूप है। 'लेखना' शब्द 'लिख' धातु से ल्युट् प्रत्यय एवं स्त्रीत्वविवक्षा में टाप् प्रत्यय करने पर निष्पन्न होगा। . लिख धातु का अर्थ यहाँ 'कृश करना' अभिप्रेत है। 'लेखन' शब्द के विविध अर्थों में 'पतला करना, कृश या दुर्बल करना' अर्थ भी है। भट्ट अकलंकदेव ने 'सम्यक्कायकषाय-लेखना' सल्लेखना का व्याख्यान करते हुए लिखा है'लिखेर्ण्यन्तस्य लेखना तनूकरणमिति यावत् / " अर्थात् लिख धातु से णि (णिच) प्रत्यय करने से लेखना शब्द बनता है, जिसका अर्थ तनूकरण या कृश करना है। यहाँ यह विचारणीय है कि भट्ट अकलंकदेव ने लेखना शब्द को णिजन्त प्रक्रिया का रूप माना है। णिच् प्रत्यय चुरादिगण की धातुओं में स्वार्थ में तथा णिजन्त प्रक्रिया में प्रयोजक व्यापार (प्रेषणा, अन्वेषणा, अध्येषणा) अर्थ में होता है। आचार्य पूज्यपाद ने सल्लेखना के सामान्य लक्षण में 'क्रमेण' शब्द के समावेश से दो बातों को स्पष्ट किया है। प्रथम तो सल्लेखना धीरे-धीरे करना चाहिए तथा द्वितीय इसका अभ्यास सल्लेखना ग्रहण करने के पूर्व व्रतादि के द्वारा पहले से ही होना चाहिए। जीवन के अन्तिम समय में जब श्रावक देखता है कि अब शरीर धर्मसाधन का माध्यम नहीं रह गया है तो कषायों को घटाने का प्रयत्न करता है, किन्तु यह कार्य सहज साध्य नहीं है, अपितु इसके लिए महान् प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। कषाय एवं आहार का त्याग करके आत्म-साधना में लीनता पूर्वाभ्यास से दृढ़ होती है। इसी कारण आचार्यों ने समाधिमरण की भावना भाने का निरन्तर उपदेश दिया है। तत्त्वार्थाधिगमभाष्य में कहा गया है कि काल, संहनन, दुर्बलता और उपसर्ग आदि के दोष से जब यह ज्ञात हो जाये कि अब धर्म प्राकृतविद्या-जनवरी-दिसम्बर (संयुक्तांक) '2004 00 47