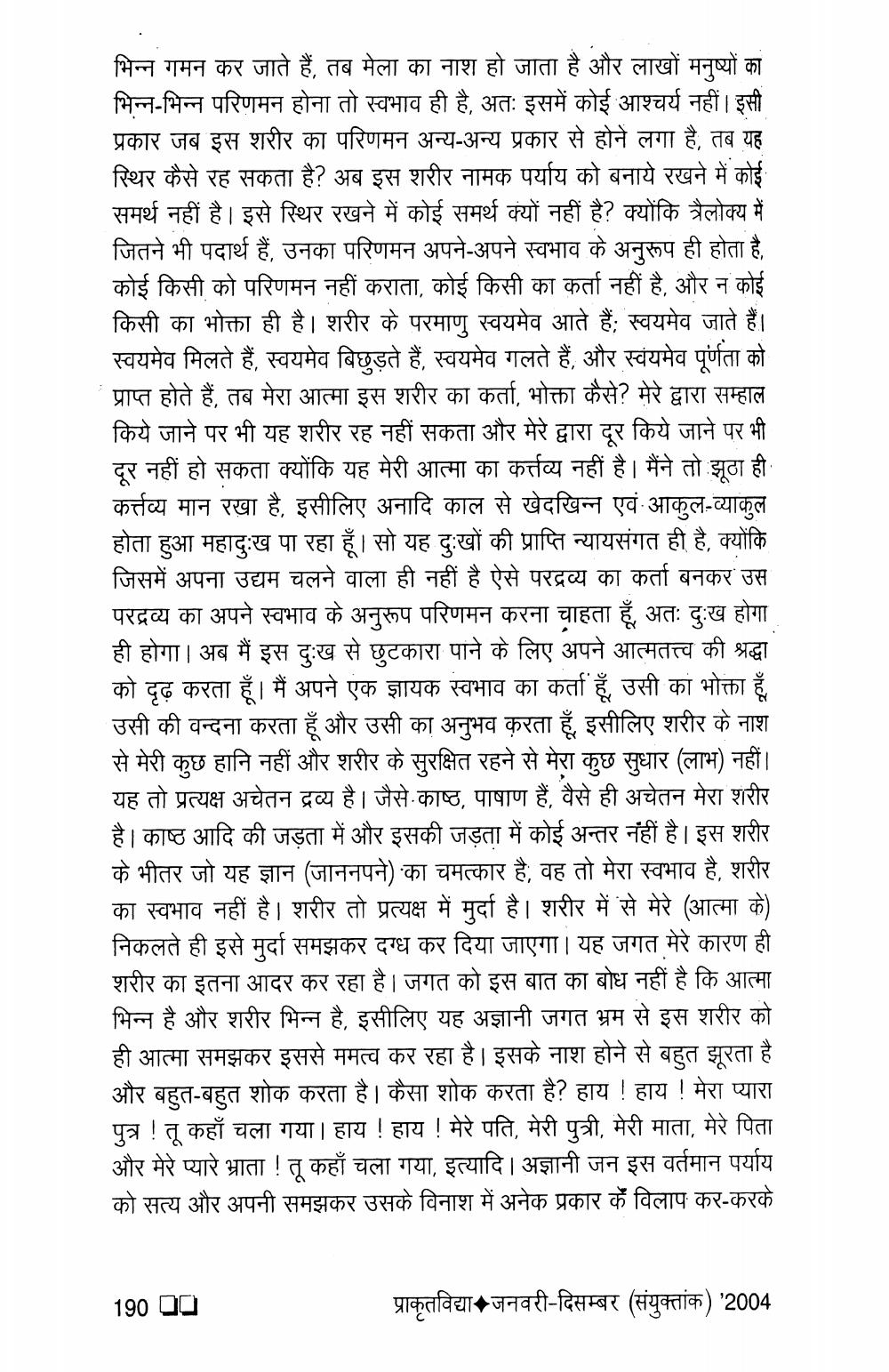________________ भिन्न गमन कर जाते हैं, तब मेला का नाश हो जाता है और लाखों मनुष्यों का भिन्न-भिन्न परिणमन होना तो स्वभाव ही है, अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इसी प्रकार जब इस शरीर का परिणमन अन्य-अन्य प्रकार से होने लगा है, तब यह स्थिर कैसे रह सकता है? अब इस शरीर नामक पर्याय को बनाये रखने में कोई समर्थ नहीं है। इसे स्थिर रखने में कोई समर्थ क्यों नहीं है? क्योंकि त्रैलोक्य में जितने भी पदार्थ हैं, उनका परिणमन अपने-अपने स्वभाव के अनुरूप ही होता है, कोई किसी को परिणमन नहीं कराता, कोई किसी का कर्ता नहीं है, और न कोई किसी का भोक्ता ही है। शरीर के परमाणु स्वयमेव आते हैं; स्वयमेव जाते हैं। स्वयमेव मिलते हैं, स्वयमेव बिछुड़ते हैं, स्वयमेव गलते हैं, और स्वयमेव पूर्णता को प्राप्त होते हैं, तब मेरा आत्मा इस शरीर का कर्ता, भोक्ता कैसे? मेरे द्वारा सम्हाल किये जाने पर भी यह शरीर रह नहीं सकता और मेरे द्वारा दूर किये जाने पर भी दूर नहीं हो सकता क्योंकि यह मेरी आत्मा का कर्त्तव्य नहीं है। मैंने तो झूठा ही कर्त्तव्य मान रखा है, इसीलिए अनादि काल से खेदखिन्न एवं आकुल-व्याकुल होता हुआ महादुःख पा रहा हूँ। सो यह दुःखों की प्राप्ति न्यायसंगत ही है, क्योंकि जिसमें अपना उद्यम चलने वाला ही नहीं है ऐसे परद्रव्य का कर्ता बनकर उस परद्रव्य का अपने स्वभाव के अनुरूप परिणमन करना चाहता हूँ, अतः दुःख होगा ही होगा। अब मैं इस दुःख से छुटकारा पाने के लिए अपने आत्मतत्त्व की श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ। मैं अपने एक ज्ञायक स्वभाव का कर्ता हूँ, उसी का भोक्ता हूँ, उसी की वन्दना करता हूँ और उसी का अनुभव करता हूँ, इसीलिए शरीर के नाश से मेरी कुछ हानि नहीं और शरीर के सुरक्षित रहने से मेरा कुछ सुधार (लाभ) नहीं। यह तो प्रत्यक्ष अचेतन द्रव्य है। जैसे काष्ठ, पाषाण हैं, वैसे ही अचेतन मेरा शरीर है। काष्ठ आदि की जड़ता में और इसकी जड़ता में कोई अन्तर नहीं है। इस शरीर के भीतर जो यह ज्ञान (जाननपने) का चमत्कार है, वह तो मेरा स्वभाव है, शरीर का स्वभाव नहीं है। शरीर तो प्रत्यक्ष में मुर्दा है। शरीर में से मेरे (आत्मा के) निकलते ही इसे मुर्दा समझकर दग्ध कर दिया जाएगा। यह जगत मेरे कारण ही शरीर का इतना आदर कर रहा है। जगत को इस बात का बोध नहीं है कि आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, इसीलिए यह अज्ञानी जगत भ्रम से इस शरीर को ही आत्मा समझकर इससे ममत्व कर रहा है। इसके नाश होने से बहुत झूरता है और बहुत-बहुत शोक करता है। कैसा शोक करता है? हाय ! हाय ! मेरा प्यारा पुत्र ! तू कहाँ चला गया। हाय ! हाय ! मेरे पति, मेरी पुत्री, मेरी माता, मेरे पिता और मेरे प्यारे भ्राता ! तू कहाँ चला गया, इत्यादि / अज्ञानी जन इस वर्तमान पर्याय को सत्य और अपनी समझकर उसके विनाश में अनेक प्रकार के विलाप कर-करके 190 00 प्राकृतविद्या-जनवरी-दिसम्बर (संयुक्तांक) '2004