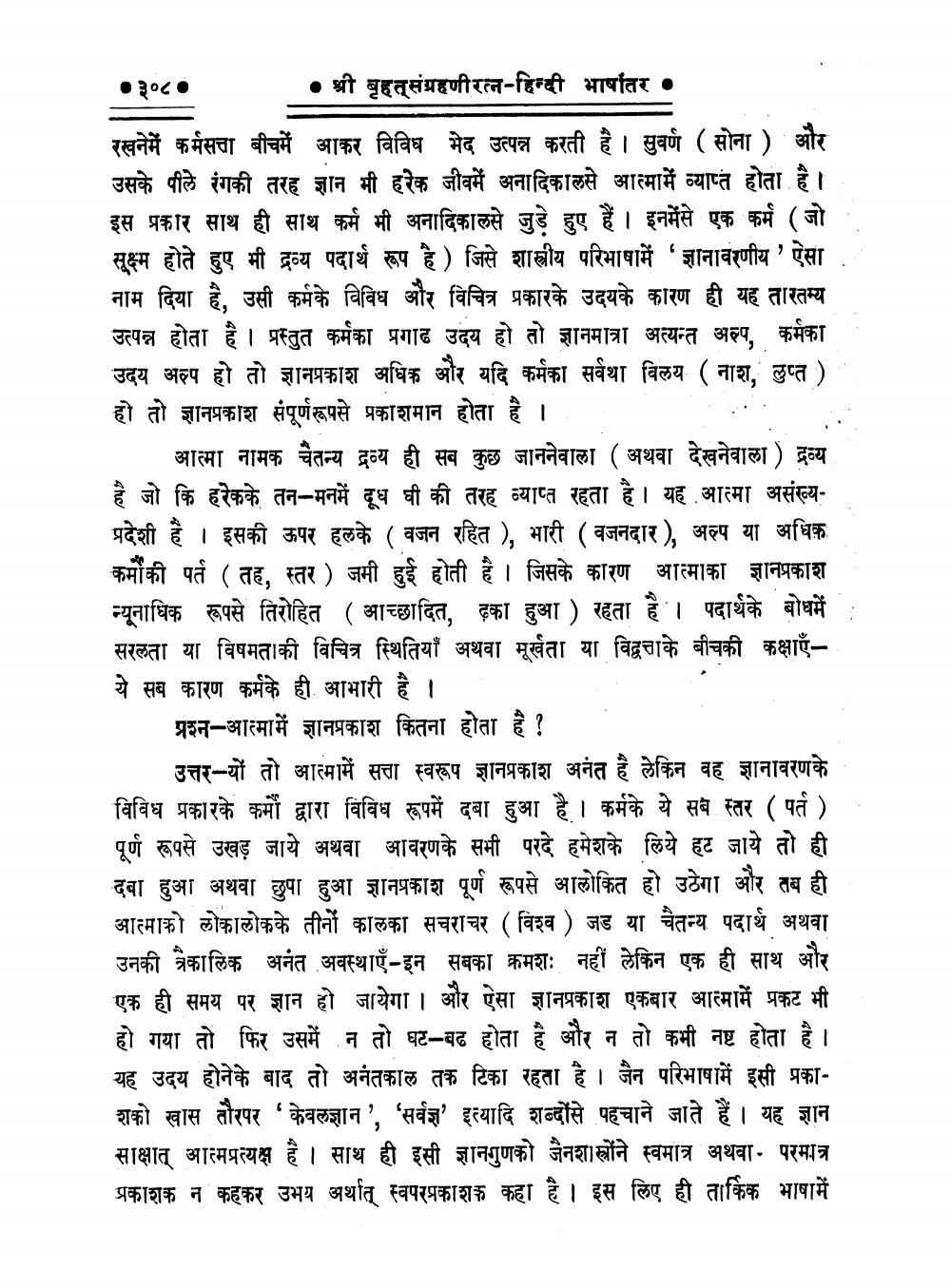________________ * श्री बृहत्संग्रहणीरत्न-हिन्दी भाषांतर * रखनेमें कर्मसत्ता बीचमें आकर विविध भेद उत्पन्न करती है। सुवर्ण (सोना) और उसके पीले रंगकी तरह ज्ञान भी हरेक जीवमें अनादिकालसे आत्मामें व्याप्त होता है। इस प्रकार साथ ही साथ कर्म भी अनादिकालसे जुड़े हुए हैं। इनमेंसे एक कर्म (जो सूक्ष्म होते हुए भी द्रव्य पदार्थ रूप है ) जिसे शास्त्रीय परिभाषामें 'ज्ञानावरणीय ' ऐसा नाम दिया है, उसी कर्मके विविध और विचित्र प्रकारके उदयके कारण ही यह तारतम्य उत्पन्न होता है / प्रस्तुत कर्मका प्रगाढ उदय हो तो ज्ञानमात्रा अत्यन्त अल्प, कर्मका उदय अल्प हो तो ज्ञानप्रकाश अधिक और यदि कर्मका सर्वथा विलय ( नाश, लुप्त ) हो तो ज्ञानप्रकाश संपूर्णरूपसे प्रकाशमान होता है / ____ आत्मा नामक चैतन्य द्रव्य ही सब कुछ जाननेवाला ( अथवा देखनेवाला) द्रव्य है जो कि हरेकके तन-मनमें दूध घी की तरह व्याप्त रहता है। यह आत्मा असंख्यप्रदेशी है / इसकी ऊपर हलके ( वजन रहित ), भारी ( वजनदार), अल्प या अधिक कोकी पर्त ( तह, स्तर ) जमी हुई होती है। जिसके कारण आत्माका ज्ञानप्रकाश न्यूनाधिक रूपसे तिरोहित ( आच्छादित, ढका हुआ ) रहता है / पदार्थके बोधमें सरलता या विषमताकी विचित्र स्थितियाँ अथवा मूर्खता या विद्वत्ताके बीचकी कक्षाएँये सब कारण कर्मके ही आभारी है / प्रश्न-आत्मामें ज्ञानप्रकाश कितना होता है ? उत्तर-यों तो आत्मामें सत्ता स्वरूप ज्ञानप्रकाश अनंत है लेकिन वह ज्ञानावरणके विविध प्रकारके कर्मों द्वारा विविध रूपमें दबा हुआ है। कर्मके ये सब स्तर ( पर्त ) पूर्ण रूपसे उखड़ जाये अथवा आवरणके सभी परदे हमेशके लिये हट जाये तो ही दवा हुआ अथवा छुपा हुआ ज्ञानप्रकाश पूर्ण रूपसे आलोकित हो उठेगा और तब ही आत्माको लोकालोकके तीनों कालका सचराचर ( विश्व ) जड या चैतन्य पदार्थ अथवा उनकी कालिक अनंत अवस्थाएँ-इन सबका क्रमशः नहीं लेकिन एक ही साथ और एक ही समय पर ज्ञान हो जायेगा। और ऐसा ज्ञानप्रकाश एकबार आत्मामें प्रकट भी हो गया तो फिर उसमें न तो घट-बढ होता है और न तो कभी नष्ट होता है। यह उदय होनेके बाद तो अनंतकाल तक टिका रहता है / जैन परिभाषामें इसी प्रकाशको खास तौरपर 'केवलज्ञान', 'सर्वज्ञ' इत्यादि शब्दोंसे पहचाने जाते हैं। यह ज्ञान साक्षात् आत्मप्रत्यक्ष है / साथ ही इसी ज्ञानगुणको जैनशास्त्रोंने स्वमात्र अथवा. परमात्र प्रकाशक न कहकर उभय अर्थात् स्वपरप्रकाशक कहा है। इस लिए ही तार्किक भाषामें