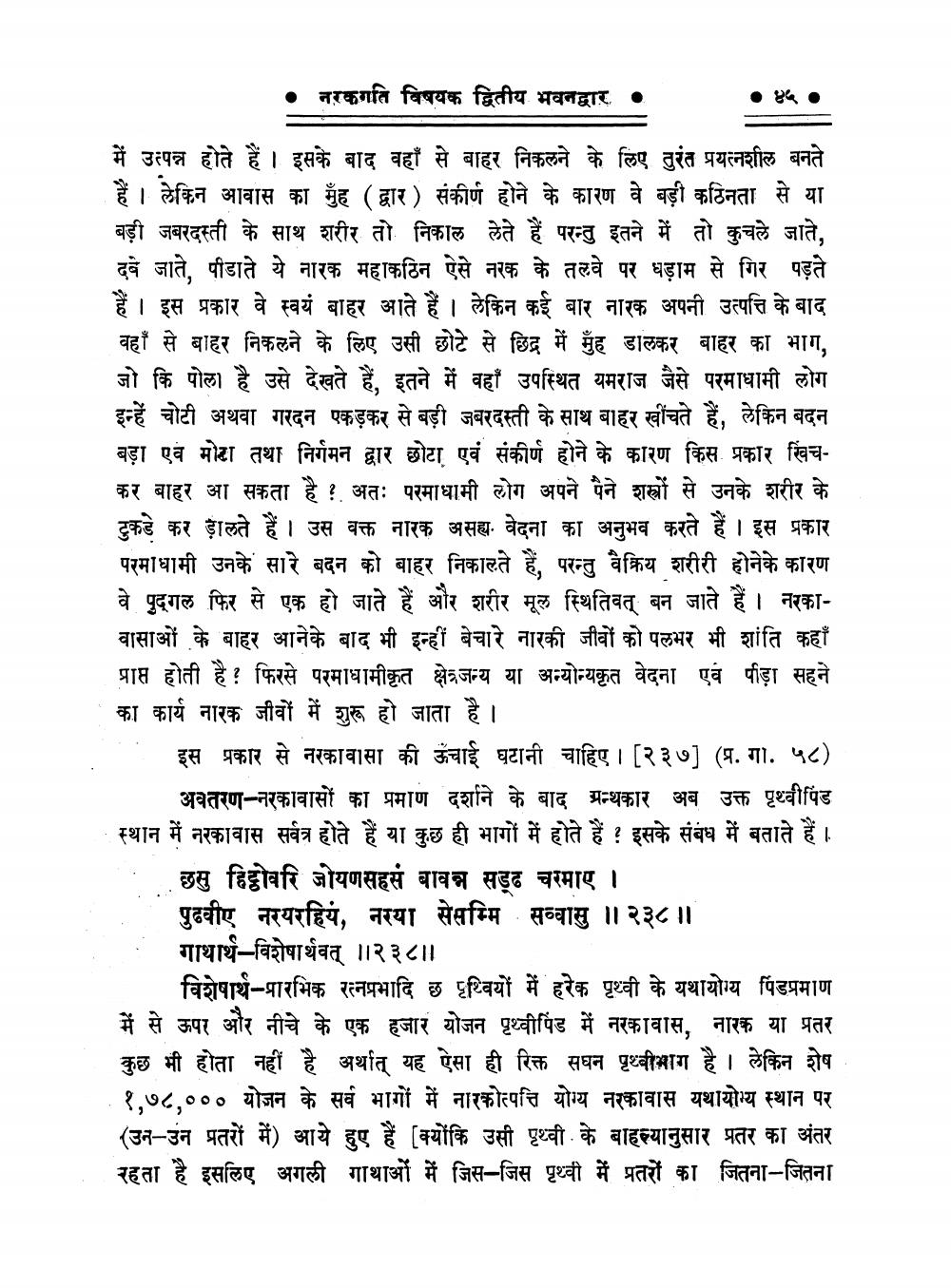________________ * नरकगति विषयक द्वितीय भवनद्वार, . में उत्पन्न होते हैं। इसके बाद वहाँ से बाहर निकलने के लिए तुरंत प्रयत्नशील बनते हैं / लेकिन आवास का मुँह (द्वार ) संकीर्ण होने के कारण वे बड़ी कठिनता से या बड़ी जबरदस्ती के साथ शरीर तो निकाल लेते हैं परन्तु इतने में तो कुचले जाते, दवे जाते, पीडाते ये नारक महाकठिन ऐसे नरक के तलवे पर धड़ाम से गिर पड़ते हैं। इस प्रकार वे स्वयं बाहर आते हैं / लेकिन कई बार नारक अपनी उत्पत्ति के बाद वहाँ से बाहर निकलने के लिए उसी छोटे से छिद्र में मुँह डालकर बाहर का भाग, जो कि पोला है उसे देखते हैं, इतने में वहाँ उपस्थित यमराज जैसे परमाधामी लोग इन्हें चोटी अथवा गरदन एकड़कर से बड़ी जबरदस्ती के साथ बाहर खींचते हैं, लेकिन बदन बड़ा एव मोटा तथा निर्गमन द्वार छोटा एवं संकीर्ण होने के कारण किस प्रकार खिंचकर बाहर आ सकता है ! अतः परमाधामी लोग अपने पैने शस्त्रों से उनके शरीर के टुकड़े कर डालते हैं। उस वक्त नारक असह्य. वेदना का अनुभव करते हैं / इस प्रकार परमाधामी उनके सारे बदन को बाहर निकालते हैं, परन्तु वैक्रिय शरीरी होनेके कारण वे पुद्गल फिर से एक हो जाते हैं और शरीर मूल स्थितिवत् बन जाते हैं। नरकावासाओं के बाहर आनेके बाद भी इन्हीं बेचारे नारकी जीवों को पलभर भी शांति कहाँ प्राप्त होती है ! फिरसे परमाधामीकृत क्षेत्रजन्य या अन्योन्यकृत वेदना एवं पीड़ा सहने का कार्य नारक जीवों में शुरू हो जाता है / इस प्रकार से नरकावासा की ऊंचाई घटानी चाहिए / [237] (प्र. गा. 58) अवतरण-नरकावासों का प्रमाण दर्शाने के बाद ग्रन्थकार अब उक्त पृथ्वीपिंड - स्थान में नरकावास सर्वत्र होते हैं या कुछ ही भागों में होते हैं ? इसके संबंध में बताते हैं / छसु हिट्ठोवरि जोयणसहसं बावन्न सड्ढ चरमाए / पुढवीए नरयरहियं, नरया सेसम्मि सव्वासु // 238 // गाथार्थ-विशेषार्थवत् // 238 // विशेषार्थ-प्रारभिक रत्नप्रभादि छ पृथ्वियों में हरेक पृथ्वी के यथायोग्य पिंडप्रमाण में से ऊपर और नीचे के एक हजार योजन पृथ्वीपिंड में नरकावास, नारक या प्रतर कुछ भी होता नहीं है अर्थात् यह ऐसा ही रिक्त सघन पृथ्वीमाग है / लेकिन शेष 1,78,000 योजन के सर्व भागों में नारकोत्पत्ति योग्य नरकावास यथायोग्य स्थान पर (उन-उन प्रतरों में) आये हुए हैं क्योंकि उसी पृथ्वी के बाहल्यानुसार प्रतर का अंतर रहता है इसलिए अगली गाथाओं में जिस-जिस पृथ्वी में प्रतरों का जितना-जितना