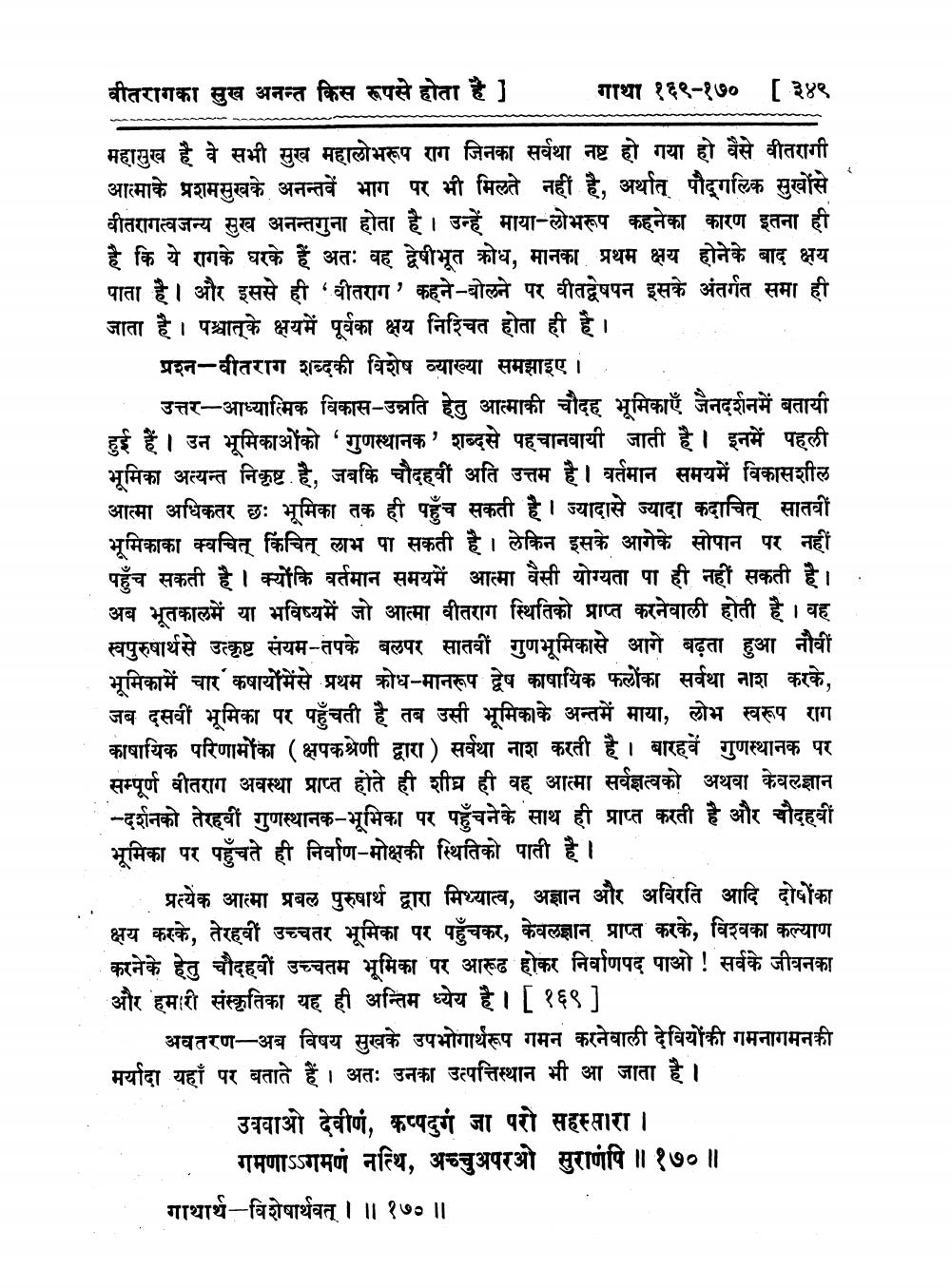________________ वीतरागका सुख अनन्त किस रूपसे होता है ] गाथा 169-170 [349 महासुख है वे सभी सुख महालोभरूप राग जिनका सर्वथा नष्ट हो गया हो वैसे वीतरागी आत्माके प्रशमसुखके अनन्तवें भाग पर भी मिलते नहीं है, अर्थात् पौद्गलिक सुखोंसे वीतरागत्वजन्य सुख अनन्तगुना होता है। उन्हें माया-लोभरूप कहनेका कारण इतना ही है कि ये रागके घरके हैं अतः वह द्वेषीभूत क्रोध, मानका प्रथम क्षय होनेके बाद क्षय पाता है। और इससे ही 'वीतराग' कहने-बोलने पर वीतद्वेषपन इसके अंतर्गत समा ही जाता है। पश्चात्के क्षयमें पूर्वका क्षय निश्चित होता ही है। प्रश्न-वीतराग शब्दकी विशेष व्याख्या समझाइए। उत्तर-आध्यात्मिक विकास-उन्नति हेतु आत्माकी चौदह भूमिकाएँ जैनदर्शनमें बतायी हुई हैं। उन भूमिकाओंको ‘गुणस्थानक' शब्दसे पहचानवायी जाती है। इनमें पहली भूमिका अत्यन्त निकृष्ट है, जबकि चौदहवीं अति उत्तम है। वर्तमान समयमें विकासशील आत्मा अधिकतर छः भूमिका तक ही पहुँच सकती है। ज्यादासे ज्यादा कदाचित् सातवीं भूमिकाका क्वचित् किंचित् लाभ पा सकती है। लेकिन इसके आगेके सोपान पर नहीं पहुँच सकती है। क्योंकि वर्तमान समयमें आत्मा वैसी योग्यता पा ही नहीं सकती है। अब भूतकालमें या भविष्यमें जो आत्मा वीतराग स्थितिको प्राप्त करनेवाली होती है। वह स्वपुरुषार्थसे उत्कृष्ट संयम-तपके बलपर सातवीं गुणभूमिकासे आगे बढ़ता हुआ नौवीं भूमिकामें चार कषायोंमेंसे प्रथम क्रोध-मानरूप द्वेष काषायिक फलोंका सर्वथा नाश करके, जब दसवीं भूमिका पर पहुँचती है तब उसी भूमिकाके अन्तमें माया, लोभ स्वरूप राग काषायिक परिणामोंका (क्षपकश्रेणी द्वारा ) सर्वथा नाश करती है। बारहवें गुणस्थानक पर सम्पूर्ण वीतराग अवस्था प्राप्त होते ही शीघ्र ही वह आत्मा सर्वज्ञत्वको अथवा केवलज्ञान -दर्शनको तेरहवीं गुणस्थानक-भूमिका पर पहुँचनेके साथ ही प्राप्त करती है और चौदहवीं भूमिका पर पहुंचते ही निर्वाण-मोक्षकी स्थितिको पाती है। . प्रत्येक आत्मा प्रबल पुरुषार्थ द्वारा मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति आदि दोषोंका क्षय करके, तेरहवीं उच्चतर भूमिका पर पहुंचकर, केवलज्ञान प्राप्त करके, विश्वका कल्याण करनेके हेतु चौदहवों उच्चतम भूमिका पर आरूढ होकर निर्वाणपद पाओ! सर्वके जीवनका और हमारी संस्कृतिका यह ही अन्तिम ध्येय है। [ 169] अवतरण-अब विषय सुखके उपभोगार्थरूप गमन करनेवाली देवियोंकी गमनागमनकी मर्यादा यहाँ पर बताते हैं। अतः उनका उत्पत्तिस्थान भी आ जाता है। उववाओ देवीणं, कप्पदुगं जा परो सहस्तारा / गमणाऽऽगमणं नस्थि, अच्चुअपरओ सुराणपि // 170 // गाथार्थ-विशेषार्थवत् / / / 170 / /