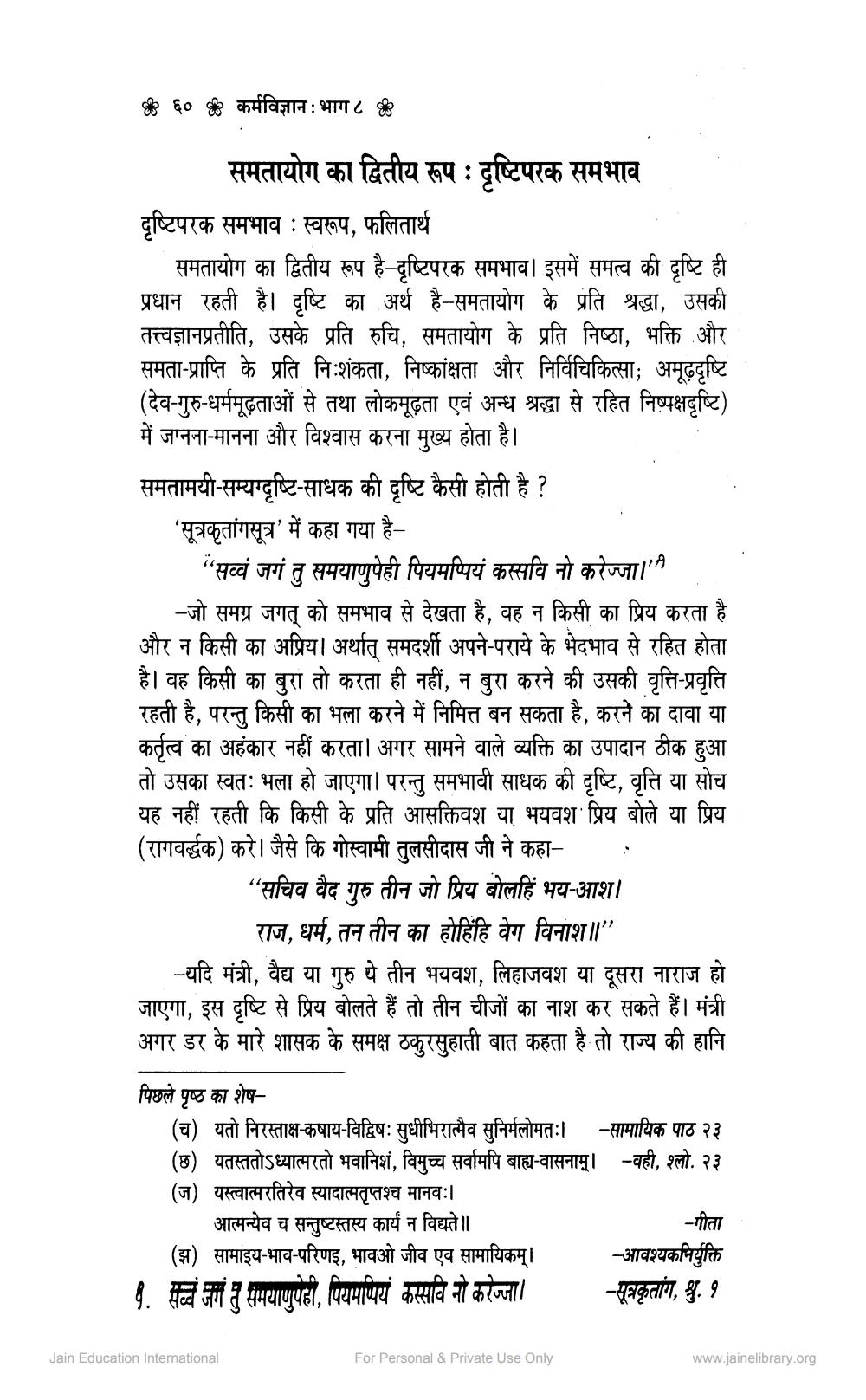________________
६० कर्मविज्ञान : भाग ८
समतायोग का द्वितीय रूप : दृष्टिपरक समभाव
दृष्टिपरक समभाव : स्वरूप,
फलितार्थ
समतायोग का द्वितीय रूप है - दृष्टिपरक समभाव। इसमें समत्व की दृष्टि ही प्रधान रहती है । दृष्टि का अर्थ है - समतायोग के प्रति श्रद्धा, उसकी तत्त्वज्ञानप्रतीति, उसके प्रति रुचि, समतायोग के प्रति निष्ठा, भक्ति और समता-प्राप्ति के प्रति निःशंकता, निष्कांक्षता और निर्विचिकित्सा; अमूढदृष्टि (देव-गुरु- धर्ममूढ़ताओं से तथा लोकमूढ़ता एवं अन्ध श्रद्धा से रहित निष्पक्षदृष्टि ) में जानना-मानना और विश्वास करना मुख्य होता है।
समतामयी-सम्यग्दृष्टि-साधक की दृष्टि कैसी होती है ?
'सूत्रकृतांगसूत्र' में कहा गया है
“सव्वं जगं तु समयाणुपेही पियमप्पियं कस्सवि नो करेज्जा ।”
- जो समग्र जगत् को समभाव से देखता है, वह न किसी का प्रिय करता है। और न किसी का अप्रिय। अर्थात् समदर्शी अपने-पराये के भेदभाव से रहित होता है। वह किसी का बुरा तो करता ही नहीं, न बुरा करने की उसकी वृत्ति-प्रवृत्ति रहती है, परन्तु किसी का भला करने में निमित्त बन सकता है, करने का दावा या कर्तृत्व का अहंकार नहीं करता। अगर सामने वाले व्यक्ति का उपादान ठीक हुआ तो उसका स्वतः भला हो जाएगा। परन्तु समभावी साधक की दृष्टि, वृत्ति या सोच यह नहीं रहती कि किसी के प्रति आसक्तिवश या भयवश प्रिय बोले या प्रिय ( रागवर्द्धक) करे। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा
“सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहिं भय-आश । राज, धर्म, तन तीन का होहिंहि वेग विनाश ॥”
-यदि मंत्री, वैद्य या गुरु ये तीन भयवश, लिहाजवंश या दूसरा नाराज हो जाएगा, इस दृष्टि से प्रिय बोलते हैं तो तीन चीजों का नाश कर सकते हैं। मंत्री अगर डर के मारे शासक के समक्ष ठकुरसुहाती बात कहता है तो राज्य की हानि
पिछले पृष्ठ का शेष
(च) यतो निरस्ताक्ष-कषाय-विद्विषः सुधीभिरात्मैव सुनिर्मलोमतः । (छ) यतस्ततोऽध्यात्मरतो भवानिशं विमुच्च सर्वामपि बाह्य - वासनाम्। (ज) यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ।
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥
(झ) सामाइय-भाव - परिणइ, भावओ जीव एव सामायिकम् ।
१. सव्वं जां तु समयाणुपेही, पियमप्पियं कस्सवि नो करेज्जा ।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
- सामायिक पाठ २३ - वही, श्लो. २३
- गीता
- आवश्यक नियुक्ति
- सूत्रकृतांग, श्रु. १
www.jainelibrary.org