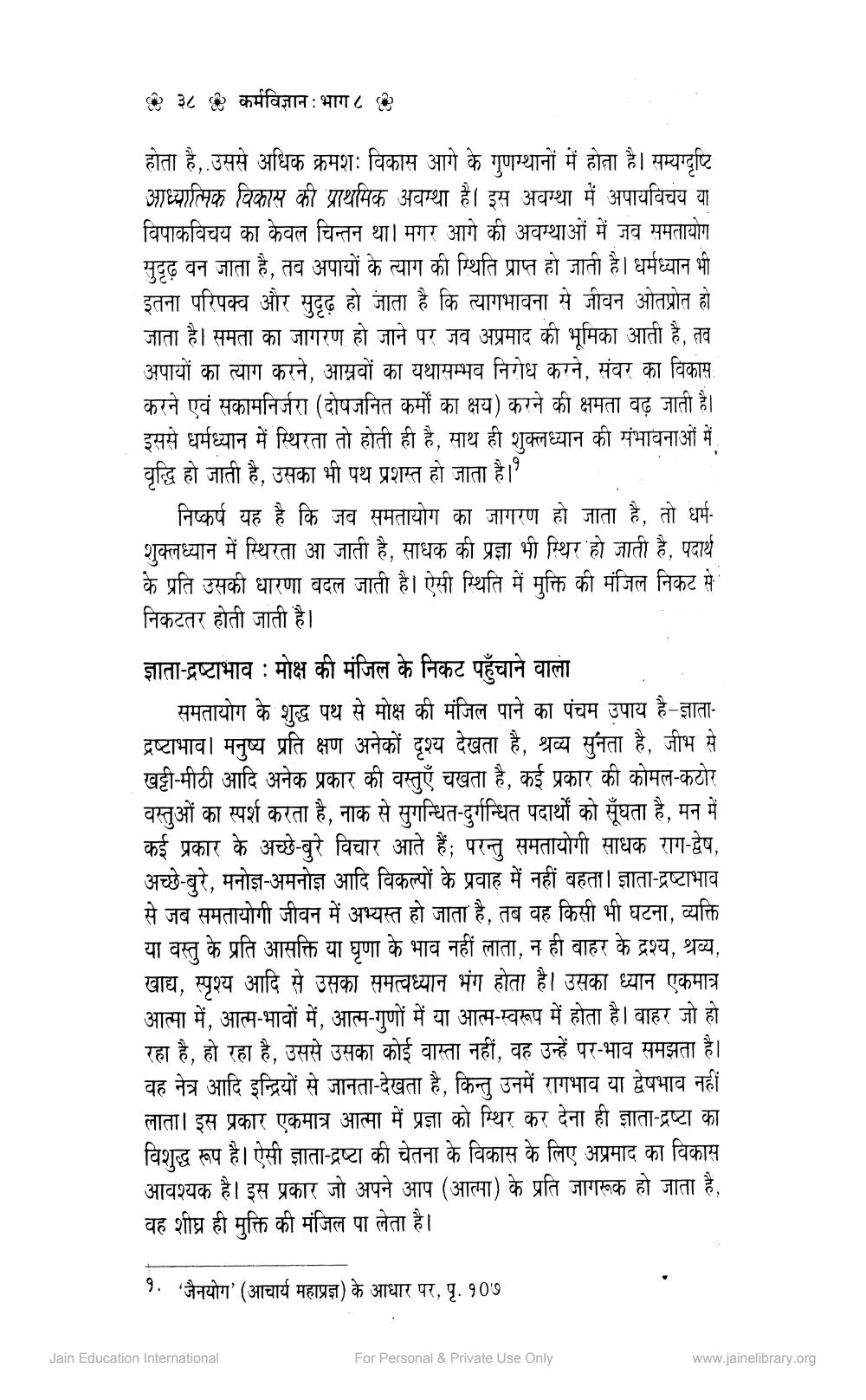________________
६ ३८ ४ कर्मविज्ञान : भाग ८३
होता है, उससे अधिक क्रमशः विकास आगे के गुणस्थानों में होता है । सम्यग्दृष्टि आध्यात्मिक विकास की प्राथमिक अवस्था है। इस अवस्था में अपायविचय या विपाकविचय का केवल चिन्तन था। मगर आगे की अवस्थाओं में जब समतायोग सुदृढ़ वन जाता है, तब अपायों के त्याग की स्थिति प्राप्त हो जाती है। धर्मध्यान भी इतना परिपक्व और सुदृढ़ हो जाता है कि त्यागभावना से जीवन ओतप्रोत हो जाता है। समता का जागरण हो जाने पर जव अप्रमाद की भूमिका आती है, तव अपायों का त्याग करने, आम्रवों का यथासम्भव निरोध करने, संवर का विकास करने एवं सकामनिर्जरा (दोषजनित कर्मों का क्षय) करने की क्षमता बढ़ जाती है। इससे धर्मध्यान में स्थिरता तो होती ही है, साथ ही शुक्लध्यान की संभावनाओं में वृद्धि हो जाती है, उसका भी पथ प्रशस्त हो जाता है । '
निष्कर्ष यह है कि जब समतायोग का जागरण हो जाता है, तो धर्मशुक्लध्यान में स्थिरता आ जाती है, साधक की प्रज्ञा भी स्थिर हो जाती है, पदार्थ के प्रति उसकी धारणा बदल जाती है। ऐसी स्थिति में मुक्ति की मंजिल निकट से निकटतर होती जाती है।
ज्ञाता-द्रष्टाभाव : मोक्ष की मंजिल के निकट पहुँचाने वाला
समतायोग के शुद्ध पथ से मोक्ष की मंजिल पाने का पंचम उपाय है - ज्ञाताद्रष्टाभाव। मनुष्य प्रति क्षण अनेकों दृश्य देखता है, श्रव्य सुनता है, जीभ से खट्टी-मीठी आदि अनेक प्रकार की वस्तुएँ चखता है, कई प्रकार की कोमल - कठोर वस्तुओं का स्पर्श करता है, नाक से सुगन्धित-दुर्गन्धित पदार्थों को सूँघता है, मन में कई प्रकार के अच्छे-बुरे विचार आते हैं; परन्तु समतायोगी साधक राग-द्वेष, अच्छे-बुरे, मनोज्ञ-अमनोज्ञ आदि विकल्पों के प्रवाह में नहीं बहता। ज्ञाता-द्रष्टाभाव से जब समतायोगी जीवन में अभ्यस्त हो जाता है, तब वह किसी भी घटना, व्यक्ति या वस्तु के प्रति आसक्ति या घृणा के भाव नहीं लाता, न ही बाहर के द्रश्य, श्रव्य, खाद्य, स्पृश्य आदि से उसका समत्वध्यान भंग होता है । उसका ध्यान एकमात्र आत्मा में, आत्म-भावों में, आत्म-गुणों में या आत्म-स्वरूप में होता है। बाहर जो हो रहा है, हो रहा है, उससे उसका कोई वास्ता नहीं, वह उन्हें पर भाव समझता है। वह नेत्र आदि इन्द्रियों से जानता - देखता है, किन्तु उनमें रागभाव या द्वेषभाव नहीं लाता। इस प्रकार एकमात्र आत्मा में प्रज्ञा को स्थिर कर देना ही ज्ञाता - द्रष्टा का विशुद्ध रूप है। ऐसी ज्ञाता-द्रष्टा की चेतना के विकास के लिए अप्रमाद का विकास आवश्यक है। इस प्रकार जो अपने आप (आत्मा) के प्रति जागरूक हो जाता हैं, वह शीघ्र ही मुक्ति की मंजिल पा लेता है।
१. 'जैनयोग' ( आचार्य महाप्रज्ञ ) के आधार पर, पृ. १०७
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org