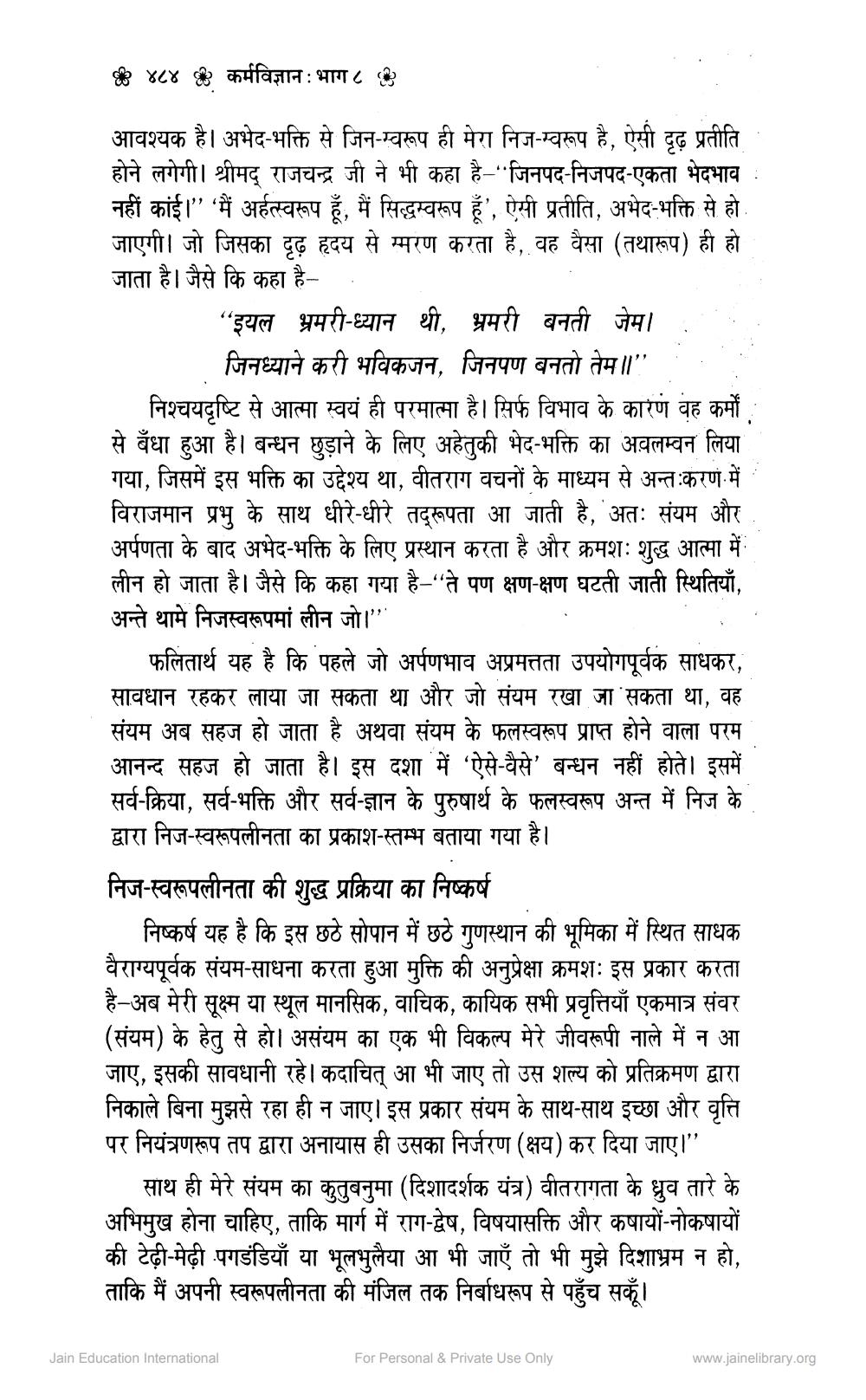________________
४८४ ४ कर्मविज्ञान : भाग ८४
आवश्यक है। अभेद-भक्ति से जिन - स्वरूप ही मेरा निज-स्वरूप है, ऐसी दृढ़ प्रतीति होने लगेगी। श्रीमद् राजचन्द्र जी ने भी कहा है- "जिनपद - निजपद - एकता भेदभाव नहीं कांई । ” 'मैं अर्हत्स्वरूप हूँ, मैं सिद्धस्वरूप हूँ, ऐसी प्रतीति, अभेद-भक्ति से हो जाएगी। जो जिसका दृढ़ हृदय से स्मरण करता है, वह वैसा ( तथारूप ) ही हो जाता है। जैसे कि कहा है
“इयल भ्रमरी - ध्यान थी, भ्रमरी बनती जेम । जिनध्याने करी भविकजन, जिनपण बनतो तेम ॥"
निश्चयदृष्टि से आत्मा स्वयं ही परमात्मा है। सिर्फ विभाव के कारण वह कर्मों से बँधा हुआ है। बन्धन छुड़ाने के लिए अहेतुकी भेद-भक्ति का अवलम्वन लिया गया, जिसमें इस भक्ति का उद्देश्य था, वीतराग वचनों के माध्यम से अन्तःकरण में विराजमान प्रभु के साथ धीरे-धीरे तद्रूपता आ जाती है, अतः संयम और अर्पणता के बाद अभेद-भक्ति के लिए प्रस्थान करता है और क्रमशः शुद्ध आत्मा में लीन हो जाता है। जैसे कि कहा गया है- "ते पण क्षण-क्षण घटती जाती स्थितियाँ, अन्ते थामे निजस्वरूपमां लीन जो ।""
फलितार्थ यह है कि पहले जो अर्पणभाव अप्रमत्तता उपयोगपूर्वक साधकर, सावधान रहकर लाया जा सकता था और जो संयम रखा जा सकता था, वह संयम अब सहज हो जाता है अथवा संयम के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला परम आनन्द सहज हो जाता है । इस दशा में 'ऐसे-वैसे' बन्धन नहीं होते। इसमें सर्व-क्रिया, सर्व-भक्ति और सर्व-ज्ञान के पुरुषार्थ के फलस्वरूप अन्त में निज द्वारा निज-स्वरूपलीनता का प्रकाश स्तम्भ बताया गया है।
निज-स्वरूपलीनता की शुद्ध प्रक्रिया का निष्कर्ष
निष्कर्ष यह है कि इस छठे सोपान में छठे गुणस्थान की भूमिका में स्थित साधक वैराग्यपूर्वक संयम-साधना करता हुआ मुक्ति की अनुप्रेक्षा क्रमशः इस प्रकार करता है- अब मेरी सूक्ष्म या स्थूल मानसिक, वाचिक, कायिक सभी प्रवृत्तियाँ एकमात्र संवर (संयम) के हेतु से हो । असंयम का एक भी विकल्प मेरे जीवरूपी नाले में न आ जाए, इसकी सावधानी रहे। कदाचित् आ भी जाए तो उस शल्य को प्रतिक्रमण द्वारा निकाले बिना मुझसे रहा ही न जाए। इस प्रकार संयम के साथ-साथ इच्छा और वृत्ति पर नियंत्रणरूप तप द्वारा अनायास ही उसका निर्जरण (क्षय) कर दिया जाए ।"
साथ ही मेरे संयम का कुतुबनुमा ( दिशादर्शक यंत्र ) वीतरागता के ध्रुव तारे के अभिमुख होना चाहिए, ताकि मार्ग में राग-द्वेष, विषयासक्ति और कषायों - नोकषायों की टेढ़ी-मेढ़ी पगडंडियाँ या भूलभुलैया आ भी जाएँ तो भी मुझे दिशाभ्रम न हो, ताकि मैं अपनी स्वरूपलीनता की मंजिल तक निर्बाधरूप से पहुँच सकूँ।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org